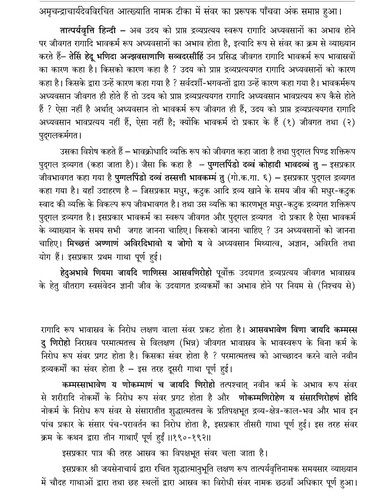I and Jineshji had a good elaborated discussion on it. Now he wish to take time to think on it. In the mean time, with his consent posting my views on the topic.
इस विषय पर कुछ शंकाए और उनके समाधान निम्न प्रकार हो सकते है।
शंका 1
जयसेन आचार्य की टीका अनुसार भावकर्म के दो भेद है। क्या अमृतचन्द्र आचार्य की टीका में उनके कथनो से ही उसके दो भेद सिद्ध कर सकते हैं?
उत्तर:
गाथा 328-331 की टीका में अमृतचन्द्रदेव ने भावकर्म लिखा है।
टीका: “जीव ही मिथ्यात्वादि भावकर्म का कर्ता है; क्योंकि यदि वह (भावकर्म) अचेतन प्रकृति का कार्य हो तो उसे (भावकर्म को) अचेतनत्व का प्रसंग आ जायेगा। जीव अपने ही मिथ्यात्वादि भावकर्म का कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुद्गलद्रव्य के मिथ्यात्वादि भावकर्म को करे तो पुद्गलद्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जायेगा। 329- 331”
यह गाथा ‘जीव के भावकर्म का कर्ता कौन?’ इस संदर्भ में है। फिरभी उसमें आचार्यदेव ने यह भी सिद्ध किया कि जीव भावकर्म का कर्ता तो है किंतु केवल अपने भावकर्म का। जो पुद्गल के मिथ्यात्व आदि भावकर्म है उसका कर्ता जीव नहीं। इससे सिद्ध होता है कि पुद्गल के भावकर्म है जो अमृतचन्द्रदेव को स्वीकार है। दोनों प्रकार के भावकर्मो का स्वीकार है इसलिए तो कहना पड़ा कि जीव पुद्गल के भावकर्म का कर्ता नहीं। केवल अपने भावकर्म का कर्ता है।
शंका 2
गाथा ८७ में दिए मिथ्यात्व आदि अजीव द्रव्यास्रव का अर्थ नए आनेवाले कर्म है या कर्मोदयरुप आस्रव?
उत्तर:
भाषा टीकाकार ने गाथा 87 से पहेले ही प्रश्न में पूछा है कि मिथ्यात्व आदि भाव क्या हैं? प्रश्न भाव पर ही है।
अब टीका के वाक्यों को देखते है। (कृपया समयसार मूल शास्त्र गाथा ८७ की टीका खोलकर आगे का उत्तर पढ़े।)
टीका: “मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव” - देखिए यहां भाव लिखा है।
टीका: “जो भाव हैं वे प्रत्येक मयूर और दर्पण” - अब मयूर और दर्पण से स्पष्ट है कि नये बंध रहे या सत्ता में पड़े द्रव्यकर्म की बात नहीं किन्तु उदयगत कर्म और जीव के भाव के निमित नैमित्तिक की बात है। यह मयूर और दर्पण का द्रष्टांत नये आनेवाले कर्म के साथ घटित नहीं होता।
टिका: “इसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्यस्वभाव से अजीव के द्वारा भाये जाते हैं वे अजीव ही हैं”- देखिये फिर यहाँ इत्यादि भाव लिखा है।
अब भावार्थ में तो तीन बार उदय और भाव की यह बात स्पष्ट ही लिखी गई है कि
भावार्थ :-
- पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मरूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीव है और कर्म के निमित्त से जीव विभावरूप परिणमित होता है, वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं इसलिये जीव हैं।
देखिये यहां स्पष्ट ही हो रहा है कि मयूर और दर्पण से कर्मउदय और जीव के विकार का निमित नैमित्तिक बताया जा रहा है। अब यदि यहाँ नए बंध रहे कर्म अर्थ करेंगे तो पंडित जयचंद जी के भावार्थ से विरोध व्यक्त होगा।
-
यहाँ यह समझना चाहिये कि मिथ्यात्वादि कर्म की प्रकृतियाँ पुद्गलद्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोगस्वरूप है। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेदज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है।
-
जब उनका भेदज्ञान होता है अर्थात् जीवभाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ८७॥
मुमुक्षु का प्रयोजन सम्यकत्व प्राप्ति है तो पुद्गल भावकर्म के स्वीकार के बिना उससे भेदज्ञान कैसे करेंगे? क्योंकि 87 के भावार्थ के यहां प्रस्तुत तीसरे पॉइंट अनुसार जीवभाव और अजीवभाव में भेदज्ञान से मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है। और फिर टीकाकार आचार्य ने बार बार भाव शब्द लिखा होने के बाद भी खेद है कि किसी कारणवश ऐसी मान्यता बन जाती है कि गाथा में नये कर्मो आस्रव ही भासता है। मिथ्यात्व आदि शब्द से कर्मोदय और कर्मोदय को भावकर्म रूप अस्वीकार वर्तता है। जबकी गाथा 328-331 की टीका में तो अमृतचन्द्रदेव ने भावकर्म लिखा भी है।
शंका 3
उदयागत कर्म को आस्रव कहते है उसका गाथा १६४-१६५ से अतिरिक्त आधार।
उत्तर:
प्रथम तो जब गाथा 164 में कर्मोदय को आस्रव कहा है तो कर्मोदय को आस्रव कहने का निषेध नहीं हो सकता है। फिर भी उसे आस्रव कहने के अन्य आधार भी यहाँ दिए जा रहे है।
कोई समझे कि उदय को आस्रव बस एक गाथा 164-165 में ही कहा है जो की स्थूल कथन है। किंतु ऐसा नहीं। गाथा 169 के उत्थानीका में ही द्रव्यास्रव शब्द है। और 170 में उन 4 प्रकार के द्रव्यास्रव को बंध के हेतु लिखे है। यहाँ से स्पष्ट है कि 169-170 में उदय की बात है।
इतना ही नहीं भावपाहुड गाथा 114 में जयचंदजी तत्त्व की भावना का चिन्तन कराते हुए आस्रव तत्व का चिंतन कर्मोदय से करा रहे है, नवीन कर्म आगमन से नहिं।
भावपाहुड गाथा 114: “तीसरा `आस्रवतत्त्व’ है वह जीव-पुद्गल के संयोग जनित भाव हैं, इनमें अनादि कर्मसम्बन्ध से जीव के भाव (भाव आस्रव) तो राग-द्वेष-मोह हैं और अजीव पुद्गल के भावकर्म के उदयरूप मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग द्रव्यास्रव हैं । इनकी भावना करना कि ये (असद्भूत व्यवहारनय अपेक्षा) मुझे होते हैं (अशुद्ध निश्चयनय से) राग-द्वेष-मोह भाव मेरे हैं, इनसे कर्मो का बंध होता है, उससे संसार होता है, इसलिए इनका कर्ता न होना (स्व में अपने ज्ञाता रहना।)”
और अध्यात्म अभ्यास शुरू करने हेतु जो सबसे पहले पढ़ी जाती है ऐसी जैन सिद्धान्त प्रवेशिका में भी आस्रव को 4 प्रकार के बताते हुए कर्मोदय को आस्रव लिखा है।
अमृतचंद्रदेव और जयसेनाचार्य दोनों की टीका में आस्रव और प्रत्यय पर्यायवाची की तरह प्रयोग हुआ है। हिंदी अनुवादक ने भी संस्कृत में दिए कर्मोदय-प्रत्यय शब्द का हिंदी में आस्रव अनुवाद एक नही कई बार किया हैं। भावार्थ में तो जयचंदजी ने कर्मोदय-प्रत्यय को अधिकतर द्रव्यास्रव ही लिखा है।
इसतरह पूर्व के अनेक पंडितों ने कर्मोदय को आस्रव स्वीकारा है।
शंका 4
कर्मो के परिणाम जैसे की उदय बंध सता आदि उनको हम जानते नहीं तो उससे भेद्ज्ञान नहीं हो सकता।
उत्तर:
समयसार गाथा 75.
जो कर्म का परिणाम अरु नोकर्म का परिणाम है
सो नहीं करे जो मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी है।
गाथा 75 पढ़ते हुए विचार जरूर करना चाहिए कि यहां “मात्र जाने” ऐसा कह के कर्मों के परिणाम को ज्ञानी जानता है ऐसा क्यों लिखा।
टीका में लिखा है कि “निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदिरूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम…” - क्या इन अंतरंग मोह राग द्वेष आदि "जीव के है और पुद्गल के कहे है?” या वास्तविक पुद्गल है?
यदि वह मोह राग द्वेष आदि को “जीव के है किंतु पुद्गल के परिणाम कहे है” - ऐसा मानते है तो, टीका में तो स्पष्ट लिखा है कि “पुद्गल परिणाम और आत्मा को घट और कुम्भार की भांति व्याप्यव्यापकभाव के अभाव के कारण कर्ताकर्मपने की असिद्धि है।” यदि उसे जीव के है और पुद्गल के कहे है, तो फिर जीव के साथ व्याप्यव्यापकभाव का अभाव नही। क्योंकि यदि वे जीव के मोह आदि है तो जीव उनमें व्यापक है ही। इसतरह टीका के व्याप्यव्यापकभाव के अभाव की बात से यह बात का विरोध आ रहा है।
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि यहाँ लिखे मोह राग द्वेष आदि अंतरंग परिणाम वे वास्तविक पुद्गल है। जीव के भाव को पुद्गल कहने रूप पुद्गल नही। जीव का उसमें व्याप्यव्यापकभाव का अभाव भी है। और जीव उनका ज्ञाता है।
हाँ जीव, ‘कर्म के मोह आदि उदय को जानता है’ - यह आचार्य की बात स्वीकारते हुए यह जिज्ञासा हो सकती है कि कैसे जानता है? अब उसका उत्तर गाथा 132 से 136 की टीका में पुद्गल के मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग के उदय का ज्ञान में कैसा स्वाद आता है वह दिया है। उस नैमित्तिक स्वाद से निमित का ज्ञान होता है और उससे भेदज्ञान संभव और आवश्यक है।
इस टीका में दी हुई एक लाइन जरूर लक्ष में लेना कि “यह पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि के उदय हेतुभुत होने पर जो कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि भाव…”
इससे 2 बात सामने आती है।
पहेले तो यह मिथ्यात्व आदि पौद्गलिक है। जीव के नहीं।
इस लाइन से एक और मुख्य बात पर लक्ष दिलाना चाहती हूं की कर्म के (मोहनियकर्म के) उदयरूप आस्रव को मिथ्यात्वादि लिखा जाता है और नए कर्म के आगमन/बंध को ज्ञानावरणादि लिखने की पद्धति है।
गाथा 164-165 में भी उसी तरह दिया है। इसलिए पौद्गलिक *मिथ्यात्वादि आस्रव शब्द से कर्मोदय समझना चाहिए। नवीन कर्म आस्रवण नहीं।
यह बात यदि ध्यान में रहेगी तो जब कभी जिन जिन गाथाओं में मिथ्यात्वादि लिखा होगा तो “वह जीव के ही हो सकते है” - ऐसा अर्थ शीघ्रता से न करने में सावचेती रहेगी क्योंकि वह मिथ्यात्व आदि कर्मोदय भी हो सकते हैं।
और यदि उन गाथाओं में पुद्गल के मिथ्यात्व की बात ज्ञान में बैठ गई तो उनके लिए आस्रव शब्द है, वह आस्रव शब्द कर्मउदय के लिए कैसे? यह उलझन नहीं रहेगी। क्योंकि सामान्यतः पुद्गल के मिथ्यात्वादि शब्द उदय के लिए है नए कर्म आस्रवण/ बंध के लिए नहीं।
समयसार में आस्रव अधिकार में जीव एवं पुद्गल के मिथ्यात्वादि आस्रव की ही चर्चा अधिक एवं प्रधान है ज्ञानावरणादि आस्रव की कम है।
समयसार के पूर्वरंग में गाथा ३६ में “मोह कुछ मेरा नहीं” कहते हुए आचार्य टीका की प्रथम लाईन में ही लिखते है की “निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रगट होकर भावकरुप होनेवाला पुद्गलद्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता।“ – अब यहाँ भावक कहकर स्पष्ट कर्मोदय की बात है। क्योंकि जीव का मोह तो भाव्य कहलाता है। और टीका की अंतिम लाईन है की “इसप्रकार भावकभाव जो मोह का उदय उससे भेद्ज्ञान हुआ।“ इसतरह पुद्गल मोह भी सिद्ध हुआ और उससे भेद्ज्ञान भी।
पुद्गल मोह को पुद्गल मानकर उससे से भेद्ज्ञान करना शास्त्रयुक्त है। उसे न स्वीकारते हुए “जीव के मोह को पुद्गल कहा है” – इस सुने हुए कथन की सिद्धि के लिए गाथाओ का अनर्थ करते हुए गाथा ६९ में द्रव्य-पर्याय में संयोगसिद्ध सम्बद्ध, गाथा १८१ में द्रव्य-पर्याय में प्रदेश भिन्न आदि असिद्धान्तिक बातों की सिद्धि क्यों? फिर उसके लिए ज्ञान और द्रष्टि के विषय में विरोध खड़ा होने से और फिर उसके भी विविध तर्क ढूंढते है।
संयोगसिद्ध सम्बन्ध द्रव्य पर्याय में नहीं होते, दों भिन्न द्रव्यों में होते है इस संबंधित कुछ आधार यहाँ प्रस्तुत करती हूँ।
टीका ६९-७० में दिया है की “जबतक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आस्रवों में” - यहाँ सोचना है की संयोगसिद्ध सम्बन्ध किनमें होता हैं?
जैनकोष से संयोग संबध के आधार लिए जा रहे हैं।
- धर्म-धर्मी में संयोग संबंध का निरास:
अब यदि भेद पक्ष का स्वीकार करने वाले वैशेषिक या बौद्ध दंडी-दंडीवत् गुण के संयोग से द्रव्य को ‘गुणवान्’ कहते हैं तो उनके पक्ष में अनेकों दूषण आते हैं– द्रव्यत्व या उष्णत्व आदि सामान्य धर्मों के योग से द्रव्य व अग्नि द्रव्यत्ववान् या उष्णत्ववान् बन सकते हैं पर द्रव्य या उष्ण नहीं। (राजवार्तिक/5/2/4/43/32 ); ( राजवार्तिक/1/1/12/6/4 )।
इस आधार से यह सिद्ध होता है की
• एक द्रव्य के धर्म धर्मी में संयोग सम्बन्ध मानना बौद्ध और वैशेषिक मान्यता है जैन नहीं।
• यदि कोई तर्क करे की यह बात स्वाभाविक धर्म/पर्याय के लिए हैं जब की गाथा ६९-७० में वैभाविक पर्याय की बात है। तो प्रथम तो आधार में ऐसा लिखा नहीं गया की यह तर्क मात्र स्वाभाविक के लिए है विभाविक के लिए नहीं।
• और दूसरी बात, यदि स्वाभाविक पर्याय से तादात्म्यपना स्वीकार किया जा रहा हैं तो यह सिद्ध हुआ की “द्रव्य-पर्याय” में संयोग सम्बन्ध नहीं है।
अब केवल वैभाविक पर्याय से ही द्रव्य का संयोग सम्बन्ध सिद्ध या असिद्ध करना है।
आगे दिए जा रहे टीका के कथन अनुसार स्वाभाविक पर्याय का अपनेपन से स्वीकार होना चाहिए। टीकांश: ‘आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होने से उनके भेद को (पृथकत्व को) न देखता हुआ, निःशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है।’
अब यह देखते हैं की क्या विभाविक पर्याय का द्रव्य से संयोगसंबंध है? तो संयोगसंबंध की सारी व्याख्या यह कहती हे की भिन्न पदार्थ में ही सयोग हो सकता हे।
शास्त्र आधार:-
• दूसरी बात यह भी है कि संयोग संबंध तो दो स्वतंत्र सत्ताधारी पदार्थों में होता है, जैसे कि देवदत्त व फरसे का संबंध। परंतु यहाँ तो द्रव्य व गुण भिन्न सत्ताधारी पदार्थ ही प्रसिद्ध नहीं है, जिनका कि संयोग होना संभव हो सके। ( सर्वार्थसिद्धि/5/2/266/10 ) ( राजवार्तिक/1/1/5/7/5/8 ); ( राजवार्तिक/1/9/11/46/19 ); ( राजवार्तिक/5/2/10/439/20 ); ( राजवार्तिक/5/2/3/436/31 ); ( कषायपाहुड़ 1/1-20/322/353/6 )।
• सर्वार्थसिद्धि/6/9/326/7 संयुजाते इति संयोगो मिश्रीकृतम् । =संयोग का अर्थ मिश्रित करना अर्थात् मिलाना है। ( राजवार्तिक/6/9/2/516/1 )
• धवला 15/24/2 को संजोगो। पुधप्पसिद्धाण मेलणं संजोगो। =पृथक् सिद्ध पदार्थों के मेल को संयोग कहते हैं।
• मू.आ./48 की वसुनंदि कृत टीका - अनात्मीयस्यात्मभाव: संयोग:। =अनात्मीय पदार्थों में आत्मभाव होना संयोग है।
द्रव्य - वैभाविक पर्याय में संयोग संबंध का आधार नहीं मिल रहा। इसलिए बिना आधार यह बात रखना दोष है। यह वैशेषिक मान्यता हैं जिसका अपने आचार्यों ने निषेध किया हैं। और हम उनकी परंपरा के होकर जिनका अपने आचार्यों ने निषेध किया उसे जैनमत के रूप में प्रस्तुत करें? ऐसा दोष कभी न हो हमसे।
जब शास्त्र कहतें हैं की दो पृथक पदार्थों में संयोग होता है, और पुद्गलगत क्रोधादि पृथक पदार्थ होते हैं। तो इस गाथा में क्रोधादि का आत्मा के साथ संयोग सम्बन्ध दिखाया है उसे पुद्गल स्वीकारने में क्या दोष आ रहा हैं?
उसे पुद्गलरुप अस्वीकार करते हुए, जीव के मानकर, सिद्धान्त से विरोध खड़ा होता है। और फिर व्यवहार नय से नहीं निश्चय से जीव के क्रोधादि को पुद्गल के खाते में डालते हुए उसे पर्याय रूप लेकर द्रव्य से पर्याय का संयोग सम्बन्ध सिद्ध का शास्त्र आधार होना आवश्यक है। जो मिल नही रहा।
जीव क्रोधादि का पृथकवाला संयोग नहीं किन्तु निमिताधीन होने से जीव क्रोधादि का जीवद्रव्य के स्वयं के साथ भी संयोग है - ऐसा तर्क शास्त्र में लिखा मिलता नहीं? पुद्गल कर्म का तो जीवक्रोधादि से संयोग है और जीव को भी अपने ही भावों से संयोग कहेंगे तो संयोग शब्द का अर्थ ही क्या रहेगा?
जिनेशजी इसपर अधिक चिंतन और अन्य विद्वानों से चर्चा-विचारणा चाहते है इसलिए अब उनकी सहमती से यह मेरे विचार फॉरम पर रख रही हूँ।
जिनेशजी का सुझाव था की मैं एक लेख लिखकर विद्वानों को भेजू। वैसे यह लिखा जा रहा उत्तर स्वयं एक लेखरुप ही है तो लेख की आवश्यकता तो अभी नहीं भासती। और समाज में मेरी ऐसी कोई भूमिका नही है की अन्य विद्वान मुझे सुनने को समय निकाले। हाँ यदि, आप में से कोई २०-२५-३० जिज्ञासु-विद्वान-अभ्यासी को एकत्रित कर पाए तो ५- दिवसीय सम्मेलन की व्यवस्था में मदद कर सकती हूँ।
आचार्यदेव द्वारा रचित समयसार के सम्यक् अर्थ द्वारा सत्यता से सम्यक्त्व तक सभी जीव पहोचें ऐसी भावना के साथ विराम लेती हूँ। आभार।