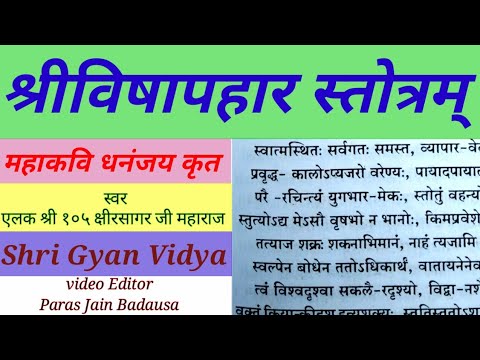महाकवि धनञ्जयप्रणीतम्
विषापहारस्तोत्रम्
(उपजाति छन्द)
आप ही शरण
स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः।
प्रवृद्धकालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराणः॥१॥
अन्वयार्थ - (स्वात्मस्थित: अपि सर्वगतः) आत्मस्वरूप में स्थित होकर भी सर्वव्यापक, (समस्तव्यापारवेदी अपि) सब व्यापारों के जानकार होकर भी (विनिवृत्तसङ्गः) परिग्रह से रहित, (प्रवृद्धकालः अपि अजर:) दीर्घ आयु वाले होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं ऐसे (वरेण्यः) श्रेष्ठ (पुराण: पुरुषः) प्राचीन पुरुष-भगवान् वृषभनाथ [न:] हम सबको (अपायात्) विनाश से (पायात्) बचावें-रक्षित करें।
टीका - पुराणः पुरुषः श्रीमदादिब्रह्मा। अपायात् कष्टात् अव्यात्। पुरिशेतेऽसौ पुरुषः। कीदृशः पुरुषः? स्वात्मस्थितोऽपि सर्वगतः। यः स्वात्मस्थितः स सर्वगतः कथमिति शब्दतो विरोध प्रदर्श्य अर्थतो विरोधमपहरति। स्वात्मनि अनन्तानन्तज्ञानादिलक्षणे स्वरूपे स्थितः। सर्वप्रतिगतः ज्ञानेन लोकालोकव्यापकत्वात् अस्य सर्वगतत्वं न विरुध्यते। पुनर्विनिवृत्तसङ्गोऽपि समस्त-व्यापारवेदी। यो विनिवृत्तसङ्गः स समस्तव्यापारवेदीति कथमिति शब्दतो विरोधमुपदार्थतो विरोधमपाकरोति। विशेषण निवृत्तः परित्यक्तः सङ्गो बहिरन्तरुपलेपो येन सः। समस्ताः सर्वे ये व्यापारा जीवपुद्गलादि- द्रव्यव्याप्रियमाणाऽनन्तगुणपर्याय-लक्षणार्थ क्रियादयस्तेषां वेत्ता। अथवा सम्यक्प्रकारेणास्ता निराकृता ये व्यापारा असिमषिकृषिवाणिज्यलक्षणास्तान् वेत्तीति। पुनः प्रवृद्ध-कालोऽप्यजरः । इति शब्दतो विरोधमुपदार्थतो विरोधं परिहरति । प्रकर्षेण वृद्धः। एधितः कालः समयो यस्य सः। अनाद्यनन्तत्वात् । न विद्यते जरा यस्य सोऽजरः । जरेत्युपलक्षणं । जराजन्ममृत्युध्वन्सीत्यर्थः पुनर्वरेण्यः । वरः श्रेष्ठ इत्यर्थः। वो युष्मान् पायादिति कर्मपदमध्याहार्यम्।
भावार्थ- श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। इस अलंकार में सुनते समय विरोध मालूम होता है पर बाद में अर्थ का विचार करने से उसका परिहार हो जाता है। देखिये-जो अपने स्वरूप में स्थित होगा वह सर्वव्यापक कैसे होगा? यह विरोध है, पर उसका परिहार यह है कि पुराण पुरुष आत्म प्रदेशों की अपेक्षा अपने स्वरूप में ही स्थित हैं पर उनका ज्ञान सब जगह के पदार्थों को जानता है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत हैं। जो सम्पूर्ण व्यापारों का जानने वाला है वह परिग्रह रहित कैसे हो सकता है? यह विरोध है। उसका परिहार यह है कि आप सर्व पदार्थों के स्वाभाविक अथवा वैभाविक परिवर्तनों को जानते हुये भी कर्मों के सम्बन्ध से रहित हैं। इसी तरह दीर्घायु से सहित होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं यह विरोध है। उसका परिहार इस तरह है कि महापुरुषों के शरीर में वृद्धावस्था का विकार नहीं होता अथवा शुद्ध आत्मस्वरूप की अपेक्षा वे कभी भी जीर्ण नहीं होते। इस तरह श्लोक में विघ्न-बाधाओं से अपनी रक्षा करने के लिए पुराण-पुरुष से प्रार्थना की गई है।
अचिन्त्य योगी
परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्यः।
स्तुत्योऽद्य मेऽसौ वृषभो न भानो: किमप्रवेशे विशति प्रदीप:॥२॥
अन्वयार्थ- (परैः) दूसरों के द्वारा (अचिन्त्यम्) चिन्तन करने के अयोग्य (युगभारम्) कर्मयुग के भार को (एकः) अकेले ही (वहन्) धारण किये हुए तथा (योगिभि: अपि) मुनियों के द्वारा भी (स्तोतुम् अशक्यः) जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती है ऐसे (असौ वृषभ:) वे भगवान् वृषभनाथ! (अद्य) आज (मे स्तुत्य:) मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं अर्थात् आज मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। सो ठीक है (भानो:) सूर्य का (अप्रवेशे) प्रवेश नहीं होने पर (किम्) क्या (प्रदीपः) दीपक (न विशति) प्रवेश नहीं करता? अर्थात् करता है।
टीका- अद्य मे ममऽसौ वृषभः श्रीमदादिब्रह्मा स्तुत्यस्तवनीयः । कृत्यानि कर्तरि षष्ठी चेति मे इत्यत्र षष्ठी। असौ कः? यः श्रीमदादिब्रह्मा योगिभिरपि ब्रह्मर्द्धिसम्पन्नैरपि स्तोतुमशक्यः। कीदृशोऽसौ? एकोऽसहायः सन् परैरन्यपुरुषैरचिन्त्यं मनसाप्यस्मरणीयं कृतयुगारम्भे कल्पवृक्षाद्यभावेन जीवनोपायाभावे जिजीविषया संक्लिश्यमानप्राणिप्राणधारणोपायप्रदर्शनस्वरूपं युगभारं वहन् धरन्। भानोः सूर्यस्याप्रवेशेऽप्रचारे प्रदीपः किं न प्रविशति? अपि तु प्रविशतीत्यर्थः।
भावार्थ- भगवन्! यहाँ जब भोगभूमि के बाद कर्मभूमि का समय प्रारम्भ हुआ था उस समय की सब व्यवस्था आप अकेले ही कर गये थे। इस तरह आप की विलक्षण शक्ति को देखकर योगी भी कह उठे थे कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। पर मैं आज आपकी स्तुति कर रहा हूँ, इसका कारण मेरा अभिमान नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि जिस गुफा में सूर्य का प्रवेश नहीं हो पाता उस गुफा में भी दीपक प्रवेश कर लेता है। यह ठीक है कि दीपक सूर्य की भाँति गुफा के सब पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी योगियों की तरह आपकी पूर्ण स्तुति नहीं कर सकूँगा, फिर भी मुझ में जितनी सामर्थ्य है उससे बाज क्यों आऊँ?
मेरे स्तुत्य
तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्।
स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि॥३॥
अन्वयार्थ - (शक्रः) इन्द्र ने (शकनाभिमानं) स्तुति कर सकने की शक्ति का अभिमान (तत्याज) छोड़ दिया था, किन्तु (अहम्) मैं (स्तवनानुबन्धं) स्तुति के उद्योग को (न त्यजामि) नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं (वातायनेन इव) झरोखे की तरह (स्वल्पेन बोधेन) थोड़े से ज्ञान के द्वारा (ततः) उस झरोखे और ज्ञान से (अधिकार्थम) अधिक अर्थ को (निरूपयामि) निरूपित कर रहा हूँ।
टीका - शक्रो देवेन्द्रः । स्तवनानुबन्धं स्तवनसम्बन्धिनं । शकनाभिमानं त्वा स्तोतुमहं शक्त इत्यभिमानं । तत्याज अजहात् । अहं स्तवनानुबन्धं । शकनाभिमानं । न त्यजामि न जहामि । स्तवनस्य अनुबन्धो यस्मिन् स तं । स्वल्पेन बोधेन। ततः इन्द्रात् स्वल्पज्ञानेनाधिकार्थं प्रभूतार्थं । अहं निरूपयामि बंभणीमि । केनेव? वातायनेनेव । यथा वातायनेन गवाक्षेण अधिकार्थं स्थूलतरं गजाद्यर्थं कश्चित् निरूपयति ।
भावार्थ– जिस तरह छोटे से झरोखे में झाँककर उससे कई गुणी वस्तुओं का वर्णन किया जाता है उसी तरह मैं भी अपने अल्प ज्ञान से जानकर आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ । मुझे अपनी इस अनोखी सूझ पर हर्ष और विश्वास दोनों हैं । इसलिए मैं इन्द्र की तरह अपनी शक्ति को नहीं छिपाता ।
वचन अगोचर
त्वं विश्वदृश्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः ।
वक्तुं कियान्कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततोऽशक्तिकथा तवास्तु॥४॥
अन्वयार्थ– (त्वम्) आप (विश्वदृश्वा 'अपि ') सबको देखने वाले होकर भी (सकलैः) सबके द्वारा (अदृश्यः) नहीं देखे जाते, आप (अशेषम् विद्वान्) सबको जानते हैं पर (निखिलैः अवेद्यः) सबके द्वारा नहीं जाने जाते। आप (कियान् कीदृशः) कितने और कैसे हैं (इति) यह भी (वक्तुम् अशक्यः) कहने को असमर्थ हैं (ततः) उससे ( तव स्तुतिः) आपकी स्तुति (अशक्तिकथा ) मेरी असामर्थ्य की कहानी ही (अस्तु) हो ।
टीका - भो जिन ! ततः कारणात् तव भगवतः स्तुतिस्त्वमेतावान् ईदृश इति प्रमातुं न पार्यसे । यतस्ततः स्तवनकरणे अशक्तिकथा तवास्तु भूयात् । अशक्तिः अशक्या कथा यस्यां सा । हे भगवन्! त्वं विश्वदृश्वा। विश्व पश्यतीति विश्वदृश्वा सकलजीवादिपदार्थ साक्षात् द्रष्टेत्यर्थः। त्वं सकलैरदृश्यः निरूपत्वात् । त्वमशेषं लोकालोकाकाशं विद्वान् जानन्। केवलज्ञानविराज-मानत्वात् निखिलैरवेद्यः, न वेत्तुं शक्यः त्वं कियान् कियत्परिमाणाधिकरणः कीदृशः इति वक्तुं अशक्यः, न शक्यः अशक्यः।
भावार्थ- आप सबको देखते हैं पर आपको देखने की किसी में शक्ति नहीं है। आप सबको जानते हैं पर आपको जानने की किसी में शक्ति नहीं है। आप कैसे और कितने परिमाण वाले हैं यह भी कहने की किसी में शक्ति नहीं है। इस तरह आपकी स्तुति मानो अपनी अशक्ति की चर्चा करना ही है। इससे पहले के श्लोक में कवि ने कहा था कि आपकी स्तुति से इन्द्र ने अभिमान छोड़ दिया था पर मैं नहीं छोडूंगा अर्थात् मुझमें स्तुति करने की शक्ति है पर जब वे स्तुति करना प्रारम्भ करते हैं और प्रारम्भ में ही उन्हें कहना पड़ता है कि सबमें आपको देखने की, जानने की अथवा कहने की शक्ति नहीं है जिसका तात्पर्य अर्थ यह होता है कि मुझमें भी उसकी शक्ति नहीं है, तब उन्हें भी अन्त में स्वीकार करना पड़ता है कि इन्द्र ने जो शक्ति का अभिमान छोड़ा था वह ठीक ही किया था और मेरे द्वारा की गई यह स्तुति भी मेरी अशक्ति की कथा ही हो।
नि:स्वार्थ बालवैद्य
व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै-रुल्लापतां लोकमवापिपस्त्वं।
हिताहितान्वेषणमान्द्यभाज: सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः॥५॥
अन्वयार्थ- (त्वम्) आपने (बालम् इव) बालक की तरह (आत्मदोषैः) अपने द्वारा किये गये अपराधों से (व्यापीडितम्) अत्यन्त पीड़ित (लोकम्) संसारी मनुष्यों को (उल्लाघताम्) नीरोगता (अवापिप:) प्राप्त कराई है। निश्चय से आप (हिताहितान्वेषणमान्यभाजः) भले-बुरे के विचार करने में मुर्खता को प्राप्त हए (सर्वस्य जन्तोः) सब प्राणियों के (बालवैद्यः) बालवैद्य हैं।
टीका- हे ब्रह्मन्! त्वं सर्वस्य जन्तोः सकलभव्यप्राणिगणस्य। बालवैद्योऽसि बालचिकित्सोऽसि। संसारवर्त्तिनां भव्यजीवानां त्वमेव परोपकारी नान्य इति तात्पर्यार्थः। कथंभूतस्य जन्तोः मोक्षो मोक्षकारणं हितं। संसार: संसारकारणं अहितं। तयोरन्वेषणे विचारणे मान्य। मन्दत्वं जडत्वं भजतीति। तस्य कुतो वैद्योऽसि? यतः कारणात् त्वदाश्रितं सर्वं लोकमुल्लाघतां नीरोगतामबाधतां प्रापयसीत्यर्थः । कथंभूतं लोकं? आत्मदोषैः पूर्वजन्मोपार्जितकर्मभिर्व्यापीडितं - बाधितं, कमिवं ? बालमिव। यथा कश्चन बालवैद्यो बालमुल्लाघतां नीरोगतां नयति । कीदृशं बालं ? आत्मदोषै- र्वातादिभिर्व्यापीडितं व्याहतम् ।
भावार्थ - जिस तरह बालकों की चिकित्सा करने वाला वैद्य, अपनी भूल से पैदा किये हुए वात, पित्त, कफ आदि दोषों से पीड़ित बालकों के अच्छे बुरे का ज्ञान करा कर उन्हें नीरोग बना देता है और अपने ‘बाल वैद्य’ इस नाम को सार्थक बना लेता है उसी तरह आप भी हित और अहित के निर्णय करने में असमर्थ बाल अर्थात् अज्ञानी जीवों के हित, अहित का बोध कराकर संसार के दुःखों से छुड़ाकर स्वस्थ बना देते हैं । इस तरह आपका भी ‘बाल वैद्य’ अर्थात् ’ अज्ञानियों के वैद्य’ यह नाम सार्थक सिद्ध होता है।
शीघ्र फल प्रदाता
दाता न हर्ता दिवसं विवस्वानद्यश्व इत्यच्युत ! दर्शिताशः ।
सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय ॥६॥
अन्वयार्थ - ( अच्युत!) अपने उदारता आदि गुणों से कभी च्युत न होने वाले हे अच्युत ! (विवस्वान्) सूर्य (न दाता ‘न’ हर्ता) न देता है न अपहरण करता है सिर्फ ( अद्य श्वः) आजकल (इति) इस तरह (दर्शिताश:) आशा [दूसरे पक्ष में दिशा को] दिखाता हुआ (अशक्तः ‘सन्’) असमर्थ होता हुआ (एवम्) ऐसे ही - बिना लिए दिये ही (सव्याजम् ) कपट सहित (दिवसम् ) दिन को ( गमयति) बिता देता है, किन्तु आप (नताय) नम्र मनुष्य के लिए (क्षणेन) क्षणभर में (अभिमतम्) इच्छित वस्तु (दत्से) दे देते हैं।
टीका - भो अच्युत ! नताय नम्राय । क्षणेन क्षणमात्रेण अभिमतं मनोऽभिलषितं । दत्से यच्छसि । भो त्रिलोकैकनाथ! अभिमुखायाभिमतफलं त्वदन्यः कोऽपि दातुं न प्रभवतीति भावार्थः । न च्युतः सम्यग्दर्शनादिस्वभावो यस्य स तस्यामन्त्रणे भो अच्युत ! विवस्वान् सूर्य इव त्वदन्यो अशक्तोऽसमर्थः पुमान् स दाता न हर्ता दातुमशक्यत्वात् । अद्य श्व इति दर्शिता आशा वाञ्छा येन सः । पक्षे प्रदर्शित दिग्मण्डलो भूत्वा । एवं सव्याजं यथा स्यात्तथा । दिवसं गमयति कालयापनां करोतीत्यर्थः ।
भावार्थ- लोग सूर्योदय होते ही हाथ जोड़ शिर झुकाकर " नमो नारायण” कहते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं और उससे इच्छित वरदान मांगते हैं, पर वह “ आज दूँगा- कल दूँगा” इस तरह आशा दिखाता हुआ दिन बिता देता है, किसी को कुछ लेता देता नहीं है - असमर्थ जो ठहरा। पर आप नम्र मनुष्य को उसकी इच्छित वस्तु क्षणभर में दे देते हैं। इस तरह आप सूर्य से बहुत बढ़कर हैं ।
दर्पणवत् वीतरागता
उपैति भक्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखं ।
सदावदातद्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि॥७॥
अन्वयार्थ - ( त्वयि सुमुखः ) आपके अनुकूल चलने वाला पुरुष (भक्त्या) भक्ति से ( सुखानि) सुखों को (उपैति) प्राप्त होता है (च) जैन विद्यापीठ और (विमुखः) प्रतिकूल चलने वाला पुरुष (स्वभावात्) स्वभाव से ही (दुःखम् 'उपैति ') दुःख पाता है, किन्तु (त्वम्) आप (तयोः) उन दोनों के आगे (आदर्श इव) दर्पण की तरह (सदा) हमेशा (अवदातद्युतिः) उज्ज्वल कान्तियुक्त तथा (एकरूपः) एक सदृश (अवभासि) शोभायमान रहते हैं ।
टीका - भो नाथ! त्वयि परमेश्वरे ! सुमुखः सम्यग्दृष्टिः । भक्त्या कृत्वा। स्वभावात् सहजतया । सुखानि सौधर्मेन्द्रनागेन्द्र - चक्रयादि- जनितनानासातानि । उपैति प्राप्नोतीति भावः । च पुनस्त्वयि विषये विमुखः प्राणी मिथ्यादृष्टिदुःखं नारकतिर्यङ्गिनगोदजनिताऽसातमुपैति । तयोर्भाक्तिका- भाक्तिकयोस्त्वं भगवानेकरूपः । अवभासि शोभसे । क इव । आदर्श इव यथा आदर्शो मुकुरः सुमुख - विमुखयोरङ्गिनोरेकरूपः शोभते । कीदृशस्त्वं ? सदाऽवदाता निर्मला द्युतिर्यस्य सः ।
भावार्थ - जिस प्रकार दर्पण के सामने मुँह करने वाला पुरुष दर्पण में अपना सुन्दर चेहरा देखकर सुखी होता है और पीठ देकर खड़ा हुआ पुरुष अपना चेहरा न देख सकने से दुःखी होता है- उनके सुख दुःख में दर्पण कारण नहीं है। दर्पण तो उन दोनों के लिए हमेशा एकरूप ही है, पर वे दो मनुष्य अपनी अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया से अपने आप सुखी दुःखी होते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य आपके विषय में सुमुख होता है अर्थात् आपको पूज्य दृष्टि से देखता है - आपकी भक्ति करता है वह शुभ कर्मों का बन्ध होने अथवा अशुभ कर्मों की निर्जरा होने से स्वयं सुखी होता है और जो आपके विषय में विमुख रहता है अर्थात् आपको पूज्य नहीं समझता और न आपकी भक्ति ही करता है वह अशुभ कर्मों का बन्ध होने से दुःख पाता है । उनके सुख दुःख में आप कारण नहीं है। आप तो हमेशा दोनों के लिए रागद्वेष रहित और चैतन्य चमत्कार मय एकरूप ही हैं।
सर्वव्यापी
अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर्मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र ।
द्यावापृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि ॥८॥
अन्वयार्थ - ( अब्धेः ) समुद्र की (अगाधता) गहराई [ तत्र अस्ति ] वहाँ है (यतः सः पयोधि:) जहाँ वह समुद्र है । (मेरो:) सुमेरुपर्वत की (तुङ्गा प्रकृतिः) उन्नत प्रकृति - ऊँचाई (तत्र) वहाँ है (यत्र सः) जहाँ वह सुमेरु पर्वत है (च) और ( द्यावापृथिव्योः) आकाश - पृथ्वी की (पृथुता) विशालता भी (तथैव) उसी प्रकार है अर्थात् जहाँ आकाश और पृथ्वी है, वहीं उनकी विशालता है । परन्तु (त्वदीया अगाधता) आपकी गहराई (तुङ्गा प्रकृतिः) उन्नत प्रकृति ( च पृथुता) और हृदय की विशालता ने (भुवनान्तराणि) तीनों लोकों के मध्यभाग को (व्याप) व्याप्त कर लिया है ।
टीका - भो देव ! अब्धेः समुद्रस्यागाधता गम्भीरता यतो यावत्क्षेत्रं स पयोधिः समुद्रोऽस्ति तावत्येवास्ति । च पुनः मेरोर्मंदरस्य तुङ्गा प्रकृतिरुन्नतस्वभावो यत्रेति यावत्क्षेत्रं स मेरुरस्ति तावत्येवास्ति । द्यावापृथिव्योर्गगनावन्योः पृथुता विशालता तथैवेति यत्र तिष्ठतस्तत्रैवेत्यर्थः ।त्वदीया सा गम्भीरा तुङ्गता विशालता च भुवनान्तराणि लोकालोकमशेषं व्यापत् प्राप्नोति स्म । अनेन सर्वज्ञस्य महिमा लोकोत्तरः प्रकटितः ।
भावार्थ– अगाधता शब्द के दो अर्थ हैं - समुद्र वगैरह में पानी की गहराई और मनुष्य हृदय में रहने वाले धैर्य की अधिकता । तुंगा प्रकृति शब्द भी द्व्यर्थक है। पहाड़ वगैरह की ऊँचाई और मन में दीनता का न होना। इसी तरह पृथुता, विशालता के भी दो अर्थ हैं। जमीन आकाश वगैरह के प्रदेशों का फैलाव और मनमें सबको अपनाने के भाव, सबके प्रति प्रेममयी भावना ।
भगवन्! समुद्र की गम्भीरता समुद्र के ही पास है, मेरु पर्वत की ऊँचाई मेरु के ही पास है और आकाश पृथ्वी की विस्तारता भी उन्हीं के पास है परन्तु आपकी अगाधता - धैर्यवृत्ति, ऊँचाई - अदैन्यवृत्ति और पृथुता- उदारवृत्ति सारे संसार में फैली हुई है। इसलिए जो कहा करते हैं कि आपकी गम्भीरता समुद्र के समान है, उन्नत प्रकृति मेरु की तरह है और विशालता आकाश पृथिवी के सदृश है वे भूल करते हैं ।
यथार्थ वस्तु प्रतिपादक
तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च ।
दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर्विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं॥९॥
अन्वयार्थ - (अनवस्था ) भ्रमणशीलता - परिवर्तनशीलता (तव) आपका (परमार्थतत्त्वम्) वास्तविक सिद्धान्त है (च) और (त्वया) आपके द्वारा (पुनरागमः न गीत:) मोक्ष से वापस आने का उपदेश दिया नहीं गया है तथा (त्वम्) आप (दृष्टम्) प्रत्यक्ष इस लोक सम्बन्धी सुख (विहाय ) छोड़कर (अदृष्टम्) परलोक सम्बन्धी सुख को (ऐषी:) चाहते हैं; इस तरह (त्वम्) आप (विरुद्धवृत्तः अपि) विपरीत प्रवृत्ति युक्त होने पर भी (समञ्जसः) उचितता से युक्त हैं ।
टीका— भो नाथ! त्वं विरुद्धवृत्तोऽपि विरुद्धचरणोऽपि समंजसः समीचीनः। लोकचरणाद्विरुद्धं वृत्तमाचरणं यस्य सः। तव मतेऽनवस्था परमार्थतत्त्वं वर्तते । अनवस्था विरुद्धपक्षे भ्रमणं । विरोधपरिहारपक्षे सर्वथा नित्यत्वमेकत्वमित्याद्येकरूपताऽवस्था तदभावोऽनवस्था निश्चितार्थतत्त्वं । त्वया भगवता पुनरागमः पुनरावत्तिः न गीतः न कथितः । भो देव! च पुनः । त्वं दृष्टं दृष्टफलं । विहाय परित्यज्य । अदृष्टमदृष्टफलमैषीर्वाञ्छसि स्म। विरुद्धपक्षे दृष्टं दृष्टफलं । विरोधपरिहारपक्षे इन्द्रियसुखं । अदृष्टं अदृष्टफलं विरुद्धपक्षे। विरोधपरिहार - पक्षेऽतीन्द्रियसुखं । इति यावत्। विरुद्धपक्षे पुनरागमनं पुनरावृत्तिः । विरोधपरिहारपक्षे मुक्तजीवानां पुनरागमनाभावः।
भावार्थ- जब आपका सिद्धान्त है कि सब पदार्थ परिवर्तनशील हैं - सभी में उत्पाद व्यय ध्रौव्य होता है तब सिद्धों में भी परिवर्तन अवश्य होगा, किन्तु आप उनके पुनरागमन को संसार में वापस आने को स्वीकार नहीं करते, यह विरुद्ध बात है । जो मनुष्य प्रत्यक्ष सामने रखी हुई वस्तु को छोड़कर अप्रत्यक्ष-परभव में प्राप्त होने वाली वस्तु के पीछे पड़ता है, लोक में वह अच्छा नहीं कहलाता, परन्तु, आप वर्तमान के सुखों को छोड़कर भविष्य के सुख प्राप्त करने की इच्छा से उद्योग करते हैं यह भी विरुद्ध बात है । पर जब इन दोनों बातों का तत्त्व दृष्टि से विचार करते हैं तब वे दोनों ठीक मालूम होने लगती हैं जिससे आपकी प्रवृत्ति उचित ही रही आती है। यद्यपि पर्यायदृष्टि से सब पदार्थों में परिवर्तन होता है-सिद्धों में भी होता है तथापि द्रव्यदृष्टि से सब पदार्थ अपरिवर्तनरूप भी हैं। संसार में आने का कारण कर्मबन्ध है और वह कर्मबन्ध सिद्ध अवस्था में जड़मूल से नष्ट हो जाता है इसलिए सिद्ध जीव फिर कभी लौटकर संसार में वापिस नहीं आते, यह आपका सिद्धान्त उचित ही है । इसी तरह आपने वर्तमान के क्षणभंगुर - इन्द्रियजनित सुखों से मोह छोड़कर सच्चे आत्म- सुख को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। वह सच्चा सुख तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि यह प्राणी इन्द्रियजनित सुख में लगा रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष के अल्प सुख को छोड़कर वीतरागता प्राप्त करने से परभव में सच्चा सुख प्राप्त होता हो उसे कौन प्राप्त न करना चाहेगा? इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है ।
काम विजयी
स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः ।
अशेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवानजागः ॥१०॥
अन्वयार्थ–(स्मरः) काम (भवता एव) आपके द्वारा ही (सुदग्ध:) अच्छी तरह भस्म किया गया है (यदि नाम शम्भुः) यदि आप कहें कि महादेव ने भी तो भस्म किया था तो वह कहना ठीक नहीं क्योंकि बाद में वह (तस्मिन्) उस काम के विषय में (उद्धूलितात्मा) कलंकित हो गया था और (विष्णु अपि) विष्णु ने भी (वृन्दोपहतः ‘सन्’) वृन्दा–लक्ष्मी नामक स्त्री से प्रेरित हो अथवा वृन्द - स्त्री पुत्रादि समस्त परिग्रह के समूह से पीड़ित हो। (अशेत) शयन किया था । (येन) जिस कारण से (भवान् अजागः) आप जागृत रहे अर्थात् कामनिद्रा में अचेत नहीं हुए। इसलिए (किं गृह्यते) कामदेव के द्वारा आपकी कौन-सी वस्तु ग्रहण की जाती है अर्थात् क्यों भी नहीं?
टीका— भो देव! भवतैव त्वयैव । स्मरः कामः । सुदग्धः सुखेन दग्ध इत्यर्थः। यदि नाम निश्चयेन । तस्मिन्भस्मितात्मनि भस्मरूपे शम्भुरीश्वरः उद्धूलितो लुठितत्वाल्लिप्त आत्मा यस्य सः । ईश्वरेण कामो दग्ध इत्यसत्यमीति सूचितं । विष्णुर्नारायणो वृन्दोपहतोपि सन् अशेत । सागरमध्ये सकलपरिग्रहानूल्लसन्नपि वैचित्येन सुप्तवान् । येन कारणेन भवान् त्वं अजागः। जाग्रदवस्थामिवान्वभूः अत आह । ततः सकाशात्। येन कारणेन कामेन किं वस्तु गृह्यते? ।
भावार्थ– हे भगवन्! जगद्विजयी काम को आपने ही भस्म किया था। लोग जो कहा करते हैं कि महादेव ने भस्म किया था वह ठीक नहीं, क्योंकि बाद में महादेव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह कर लिया था और काम में इतने आसक्त हुए कि अपना आधा शरीर स्त्रीरूप कर लिया था । इसी तरह विष्णु ने भी वृन्दा- लक्ष्मी के वशीभूत हो तरह तरह की कामचेष्टाएँ की थीं, पर आप हमेशा ही आत्मव्रत में लीन रहे तथा काम को इस तरह पछाड़ा कि वह फिर पनप नहीं सका।
स्वतः गुणवान्
स नीरजाः स्यादपरोऽघवान्वा तद्वृोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वं ।
स्वतोऽम्बुराशेर्महिमा न देव! स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥११॥
अन्वयार्थ - (वा) अथवा (स) वह ब्रह्मादि देवों का समूह (नीरजा) पाप रहित (स्यात्) हो और (अपरः) दूसरा देव (अघवान् ‘स्यात्’) पाप सहित हो, इस तरह (तदोषकीर्त्या एव) उनके दोषों के वर्णन करने मात्र से ही (ते) आपकी (गुणित्वम् न) गुण सहितता नहीं है। (देव!) हे देव! (अम्बुराशेः) समुद्र की (महिमा) विशालता (स्वतः ‘स्यात्’) स्वभाव से ही होती है (जलाशयस्य स्तोकापवादने न) तालाब के ‘छोटा है’ ऐसी निन्दा करने से नहीं होती।
टीका— भो देव! स हरिहरादिप्रसिद्धः परो देवः। नीरजाः पापरहितः स्याद्वा अथवा स देव अघवान् पापसहितः स्यात्। तद्द्वोषकीर्त्यैव ते तव भगवतः गुणित्वं न गुणवत्ता न । निर्गत रजो यस्मात्स नीरजाः । अघं पापं विद्यते यस्य सः। तेषां हरिहरादिदेवानां दोषास्तेषां कीर्तिः कथनं तया। गुणाविद्यते यस्य स तस्य भावो गुणित्वं । अम्बुराशेः समुद्रस्य स्वत एवं महिमास्ति। जलाशयस्याख्यात-सरोवरादिस्तोकापवादेन न स्यात् । तुच्छत्व- ख्यापनलक्षणदूषणेन न भवेत् । स्तोकः स्वल्प इति यो हि अपवादस्तेन।
भावार्थ - हे भगवन् ! दूसरे के दोष बतलाकर हम आपका गुणीपना सिद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि आप स्वभाव से ही गुणी हैं। सरोवर को छोटा कह देने मात्र से समुद्र की विशालता सिद्ध नहीं होती किन्तु विशालता उसका स्वभाव है इसलिए वह विशाल - बड़ा कहलाता है।
कार्य-कारणज्ञ
कर्मस्थितिं जन्तुरनेक भूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य ।
त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः॥१२॥
अन्वयार्थ – (जन्तुः) जीव (कर्मस्थितिम् ) कर्मों की स्थिति को (अनेक भूमिम्) अनेक जगह (नयति) ले जाता है (च) और (सा) वह कर्मों की स्थिति (अमुम्) उस जीव को (अनेक भूमिम्) अनेक जगह ले जाती है। इस तरह (जिनेन्द्र!) हे जिनेन्द्रदेव! (त्वम्) आपने (भवाब्धौ) संसाररूप समुद्र में (नौनाविकयो इव) नाव और नाविक की तरह (तयोः) उन दोनों में (हि) निश्चय से ( परस्परस्य) एक-दूसरे का (नेतृभावम्) नेतृत्व (आख्यः) कहा है।
टीका- भो जिनेन्द्र ! जन्तुः प्राणी । कर्मस्थितिमनेकभूमिं नानावस्थां नयति प्रापयति । कर्मणां स्थितिस्तां । च पुनः सा कार्यस्थितिः अमुं जन्तुमनेकभूमिं नयति हि निश्चितं । भवाब्धौ तयोर्जीवकर्मणोः परस्पर- स्यान्योन्यस्य नेतृभावं नेतृत्वं प्रापकत्वं आख्यः कथयसि स्म। कयोरिव? नौनाविकयोरिव । यथा नौनाविकमनेकभूमिं नयति यथा नाविको नावमनेकभूमिं नयति ।
भावार्थ - सिद्धान्त ग्रन्थों में कहा गया है कि यह जीव अपने भले बुरे भावों से जिन कर्मों को बाँधता है वे कर्म तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक फल देकर खिर नहीं जाते। इस बीच में जीव जन्म-मरण कर अनेक स्थानों में पैदा हो जाता है। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है और जीव का जन्म-मरणकर जहाँ तहाँ पैदा होना आयु आदि कर्मों की सहायता के बिना नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही जीवको चारों गतियों में जहाँ तहाँ ले जाते हैं । हे भगवन्! आपने इन दोनों में परस्पर का नेतृत्व उस तरह कहा है जिस तरह कि समुद्र में पड़े हुए जहाज और खेवटिया में हुआ करता है।
अज्ञ चेष्टा
**सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति । **
तैलाय बालाः सिकतासमूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः॥१३॥
अन्वयार्थ- जिस प्रकार (बाला:) बालक (तैलाय) तेल के लिए (सिकता-समूहम्) बालू के समूह को (निपीडयन्ति) पेलते हैं (स्फुटम्) ठीक उसी प्रकार (अत्वदीयाः) आपके प्रतिकूल चलने वाले पुरुष (सुखाय) सुख के लिए (दुःखानि) दुःखों को (गुणाय) गुण के लिए (दोषान्) दोषों को और (धर्माय) धर्म के लिए (पापानि) पापों को (समाचरन्ति) आचरित करते हैं ।
टीका— भो देव! अत्वदीयास्त्वत्तः पराङ्मुखाः पुमांसः । स्फुटं निश्चितं सुखाय सुखार्थं । दुःखानि समाचरन्ति । गुणाय गुणार्थं दोषान् समाचरन्ति। धर्माय धर्मार्थं । पापानि समाचरन्ति । पुनः बालस्तैलाय तैलार्थं । सिकतासमूहं वालुकापुञ्जं । निपीडयन्ति पीलयन्तीत्यर्थः ।
भावार्थ– हे भगवन्! जो आपके शासन में नहीं चलते उन्हें धार्मिक तत्त्वों का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता इसलिए वे अज्ञानियों की तरह उल्टे आचरण करते हैं । वे किसी स्त्री, राज्य या स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सुखी होने की इच्छा से तरह-तरह के कायक्लेश कर दुःख उठाते हैं पर सकाम तपस्या का कोई फल नहीं होता इसलिए वे अन्त में भी दुःखी ही रहते हैं। “हममें शील-शांति आदि गुणों का विकाश हो” ऐसी इच्छा रखते हुए भी रति-लम्पटी, क्रोधी आदि देवों की उपासना करते हैं पर उन देवों की शीलघातक और क्रोधयुक्त क्रियाओं का उनपर बुरा असर पड़ता है जिससे उनमें गुणों का विकाश न होकर दोषों का ही विकाश हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञादि धर्म करने की इच्छा से पशुहिंसा आदि पाप करते हैं जिससे उल्टा पापबन्ध ही होता है । हे प्रभो! यह बिलकुल स्पष्ट है कि उनकी क्रियायें उन बालकों जैसी हैं जो कि तैल पाने की इच्छा से बालु के पुञ्ज को कोल्हू में पेलते हैं।
विष हरता
विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च ।
भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि ॥ १४॥
अन्वयार्थ—(अहो) आश्चर्य है कि लोग (विषापहारम्) विष को दूर करने वाले (मणिम्) मणि को (औषधानि) औषधियों को (मन्त्रम्) मन्त्र को (च) और (रसायनम्) रसायन को (समुद्दिश्य) उद्देश्य कर (भ्राम्यन्ति) यहाँ वहाँ घूमते हैं, किन्तु (त्वम्) आप ही मणि, औषधि, मन्त्र और रसायन हैं (इति) ऐसा ( न स्मरन्ति) ख्याल नहीं करते, क्योंकि (तानि) वे मणि आदि (तव एव) आपके ही (पर्यायनामानि) पर्यायवाची नाम हैं।
टीका— विषान्यपहरतीति विषापहारस्तं । मणिं तथौषधानि तथा मन्त्रं च पुनः। रसायनं सिद्धरसं समुद्दिश्य भ्राम्यन्ति भ्रमणं कुर्वन्ति । अहो इति खेदे । त्वं इति न स्मरन्ति जना इति शेषः । इतीति किं ? एतानि विषापहारमण्यादीनि तवैव भगवतः पर्यायनामानि अपरनामानि इत्यर्थः ।
भावार्थ - हे भगवन्! जो मनुष्य शुद्ध हृदय से आपका स्मरण करते हैं उनके विष वगैरह का विकार अपने आप दूर हो जाता है। कहा जाता है कि एक समय स्तोत्र के रचयिता धनञ्जय कवि के लड़के को साँप ने डँस लिया तब वे अन्य उपचार न कर उसे सीधे जिनमन्दिर में ले गये और वहाँ विषापहार स्तोत्र रचकर भगवान् के सामने पढ़ने लगे। उनकी सच्ची भक्ति के प्रभाव से पुत्र का विष दूर होने लगा और वे “विषापहारं मणिमौषधानि " इस श्लोक को पढ़कर पूरा करते हैं त्यों ही पुत्र उठकर बैठ जाता है - उसका विष विकार बिलकुल दूर हो जाता है। कवि ने स्तोत्र को पूरा किया और इसके पाठ से विष विकार दूर हुआ था इसलिए इसका नाम विषापाहार स्तोत्र प्रचलित किया।
समदृष्टि वीतरागी
चित्ते न किञ्चित्कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वम्।
हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः ॥१५॥
अन्वयार्थ—(देवः) हे देव! (त्वम्) आप (चित्ते) अपने हृदय में (किञ्चित्) कुछ भी ( न कृतवान् असि ) नहीं करते हैं - रखते हैं, , किन्तु (येन) जिसके द्वारा आप (चेतसि) हृदय में (कृतः) धारण किए हैं (तेन) उसके द्वारा (सर्वम्) समस्त (जगत्) संसार (हस्ते कृतम्) हाथ में कर लिया गया है अर्थात् उसने सब कुछ पा लिया है यह (विचित्रम्) आश्चर्य की बात है और आप (चित्तबाह्यः अपि) मन से चिन्तन करने के अयोग्य होते हुए भी (सुखेन जीवति) अनन्त सुख से जीवित हैं, यह आश्चर्य है।
टीका - भो देव! त्वं चित्तेऽन्तःकरणे किञ्चित् कमपि पुमांसं न कृतवान् असि वर्तसे। येन पुंसा चेतसि देवस्त्वं कृतः अन्तःकरणे त्वं देवो धृतः। तेन पुंसा सर्वं विचित्रं जगत् हस्ते कृतं । स पुमान् सर्वं जगत् हस्तामलकवत् जानातीति भावः । चित्तबाह्योऽपि सुखेन जीवति ।
**भावार्थ—**यह बात प्रसिद्ध है- यदि मोहन के शरीर पर पाँच हजार के आभूषण हैं तो वह मोहन, जिस कुर्सी पर बैठेगा उस कुर्सी पर भी पांच हजार के आभूषण कहलाते हैं। यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो कुर्सी पर भी कुछ नहीं कहलाता । पर यहाँ विचित्र ही बात है । आपके चित्त में कुछ भी नहीं है पर जो मनुष्य आपको अपने चित्त में विराजमान करता है उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। इस विरोध का परिहार यह है-यद्यपि आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और रागभाव न होने से आप मन में भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं अमुक मनुष्य के लिए अमुक वस्तु दूँ। फिर भी भक्त जीव अपनी शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का बन्ध कर उनके उदय - काल में सब कुछ पा लेते हैं । अथवा जो यथार्थ में आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है वह आपके समान ही निःस्पृह हो जाता है - उसकी सब इच्छाएँ शान्त हो जाती हैं। वह सोचता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिये। मैं आज आपको अपने चित्त में धारण कर सका मानों तीनों लोकों की सम्पत्तियाँ हमारे हाथ में आ गईं।
दूसरा विरोध यह है कि आप चित्त - चेतन से बाह्य होकर भी जीवित रहते हैं। अभी, जो चेतन से रहित हो जाता है वह मृत कहलाने लगता है, पर यहाँ उससे विरुद्ध बात है । विरोध का परिहार यह है - कि आप चित्तबाह्य-अर्थात् मन से चिन्तवन करने के अयोग्य होते. हुए भी अनन्त सुख से हमेशा जीवित रहते हैं - आप अजर अमर हैं। तात्पर्य यह हैं कि आपमें अनन्त सुख है तथा आप इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि भव्यजीव आपका मन से चिन्तवन भी नहीं कर पाते।
त्रिकालज्ञ
त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानियतेरमीषाम् ।
बोधाधिपत्यं प्रतिनाभविष्यत् तेऽन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्॥१६॥
अन्वयार्थ–(त्वम्) आप (त्रिकालतत्त्वम्) तीनों कालों के पदार्थों को (अवैः) जानते हैं तथा (त्रिलोकी स्वामी) तीनों लोकों के स्वामी हैं, (इति संख्या) इस प्रकार की संख्या (अमीषां नियतेः) उन पदार्थों के निश्चित संख्या वाले होने से (युज्यते) ठीक हो सकती है, परन्तु (बोधाधिपत्यं प्रति न) ज्ञान के साम्राज्य के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की संख्या ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि (इदम्) यह ज्ञान (चेत्) यदि (ते अन्ये अपि अभविष्यन्) वे तथा और भी पदार्थ होते (तर्हि) तो (अमून् अपि) उन्हें भी (व्याप्स्यत्) व्याप्त कर लेता - जान लेता ।
टीका- भो देव ! त्वं त्रिकालं तत्त्वमवैर्जानासि स्म । त्रयश्च ते कालश्च त्रिकालास्तेषां तत्त्वं। कुत इति अमीषां कालानां संख्यानियतेः कालास्रय एव सन्ति नान्ये इति संख्यानियमात् । भो देव ! त्वं त्रिलोकी स्वामी असि त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी । तस्याः स्वामी कुत इति? अमीषां लोकानां संख्यानियतेः। इतीति किं ? यतो लोकास्रय एव सन्ति नान्ये इति संख्याया निश्चयात्। तेऽन्ये इतरेपि काला लोकाश्च नाभविष्यन्। अभविष्यन् चेत् यदि ते काला लोकाश्चान्येऽभविष्यन् तर्हि अमून् कालान् लोकान् प्रत्यपीदम् बोधाधिपत्यं व्याप्त्यच्छश्वत् काला लोकाश्च अन्ये न सन्तीत्यर्थः ।
भावार्थ- हे प्रभो! आप तीन काल तथा तीन लोक की बात को जानते हैं इसलिए आपका ज्ञान भी उतना ही है ऐसा नहीं है । किन्तु आपके ज्ञान का साम्राज्य सब ओर अनन्त है । जितने पदार्थ हैं उनको तो ज्ञान जानता ही है । यदि इनके सिवाय और भी होते तो ज्ञान उन्हें भी अवश्य ही जानता।
शुभकारी सेवा
नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारि ।
तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानोरुद्बिभ्रतश्च्छत्रमिवादरेण ॥१७॥
अन्वयार्थ– (नाकस्य पत्युः) स्वर्ग के पति इन्द्र की ( रम्यम्) मनोहर (परिकर्म) सेवा (अगम्यरूपस्य ) अज्ञेयस्वरूप वाले (तव) आपका (उपकारि न) उपकार करने वाली नहीं है, किन्तु जिसका स्वरूप ज्ञात है ऐसे (भानोः) सूर्य के लिए (आदरेण) आदरपूर्वक (छत्रम् उद्विभ्रतः इव) छत्र को धारण करने वाले की तरह ( तस्य एव ) उस इन्द्र के ही (स्वसुखस्य) आत्मसुख का (हेतुः) कारण है।
टीका— भो देव! नाकस्य पत्युर्देवेन्द्रस्य रम्यं परिकर्म परिचर्यादिकं तवागम्यरूपस्योपकारी न । अगम्यमलक्ष्यं रूपं यस्य स तस्य । यदि भगवत उपकारी न तर्हि किं निष्फलं जातं । तस्यैव सेवा तत्परस्य इन्द्रस्यैव । स्वस्यात्मनः सुखस्य हेतुः कारणं । कस्येव ? भानोरिव । यथा भानोः सूर्यस्य छत्रमादरेणोद्बिभ्रत ऊर्ध्वं धरतः पुरुषस्यैवोपकारी तापहारी भवति छत्रं सूर्यस्योपकारी न भवति।
भावार्थ– जिस प्रकार कोई सूर्य के लिए छत्ता लगावे तो उससे सूर्य का कुछ भी उपकार नहीं होता क्योंकि वह सूर्य छत्ता लगाने वाले से बहुत ऊपर है परन्तु छत्ता लगाने वाले को अवश्य ही छाया का सुख होता है। उसी प्रकार इन्द्र जो आपकी सेवा करता था, उससे आपका क्या भला होता था? उल्टा शुभास्रव होने से उसी का भला होता था।
अगम्य स्वरूप
क्वोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः स चेत्किमिच्छाप्रतिकूलवादः ।
क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथातथ्यमवेविचं ते॥१८॥
अन्वयार्थ–( उपेक्षकः त्वम् क्व) रागद्वेष रहित आप कहाँ? और (सुखोपदेशः क्व) सुख का उपदेश देना कहाँ ? (चेत्) यदि (सः) वह सुख का उपदेश आप देते हैं (तर्हि) तो (इच्छाप्रतिकूलवादः क्व) इच्छा के विरुद्ध बोलना ही कहाँ है? अर्थात् आपके इच्छा नहीं है ऐसा कथन क्यों किया जाता है? (असौ क्व) इच्छा के प्रतिकूल बोलना कहाँ? (वा) और (सर्वजगत्प्रियत्वम् क्व) सब जीवों को प्रिय होना कहाँ? इस तरह जिस कारण से आपकी प्रत्येक बात में विरोध है (तत्) उस कारण से मैं (ते यथातथ्यम् नो अवेविचं) आपकी वास्तविकता - असली रूप का विवेचन नहीं कर सकता ।
टीका— भो नाथ! त्वमुपेक्षकः क्व सुखोपदेशः क्व । द्वौ क्व शब्दौ महदन्तरं सूचयतः। उपेक्षा - तृणादिकमिदं न त्याज्यं, इदं सुवर्णादिकं न ग्राह्यं इत्येवमाकारका बुद्धिर्यस्य स उपेक्षक एवंविधस्त्वं क्व ? सुखस्योपदेशः सुखोपदेशः। स क्व । चेद्यदि सुखोपदेशः, तर्हीच्छा-प्रतिकूलवादो न भवति। वा अथवाऽसावुपेक्षः क्व । सर्वजगत्प्रियत्वं क्व । यः पुमानुपेक्षकस्तस्य पुंसः सर्वं यज्जगत्तस्य प्रियत्वं न सञ्जाघटीति। त्वमुपेक्षकस्तव सर्वजगत्प्रियत्वं। तत्तस्मात् कारणात् ते तव परमेश्वरस्य यथातथ्यं अहं नावेविचं नाबूबुधम्।
भावार्थ– हे भगवन्! जब आप राग द्वेष से रहित हैं तब किसी को सुखका उपदेश कैसे देते हैं? यदि सुखका उपदेश देते हैं तो इच्छा के बिना कैसे उपदेश देते हैं? यदि इच्छा के बिना उपदेश देते हैं तो जगत् के सब जीवों को प्यारे कैसे हैं? इस तरह आपकी सब बातें परस्पर में विरुद्ध हैं । दर असल में आपकी असलियत को कोई नहीं जान सकता।
उन्नत गुण वाले
तुङ्गात्फलं यत्तदकिञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः ।
निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाद्रेर्नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः॥१९॥
अन्वयार्थ—- हे भगवन्! (तुङ्गात् अकिञ्चनात् च) उन्नत - उदार और अकिंचन-परिग्रह रहित आपसे (यत्फलं ) जो फल (प्राप्यं’ अस्ति’) प्राप्त हो सकता है (तत्) वह (समृद्धात् धनेश्वरादेः न) वह सम्पत्तिशाली धनाढ्य कुबेर आदि से प्राप्त नहीं हो सकता । ठीक ही तो है (इव) जैसे (निरम्भसः अपि उच्चतमात् अद्रेः) पानी से शून्य होने पर भी अत्यन्त ऊँचे पहाड़ से नदी निकलती है किन्तु (पयोधे: ) समुद्र से (एका अपि धुनी) एक भी नदी (न निर्याति) नहीं निकलती है ।
टीका- भो देव! अकिञ्चनाच्च तुङ्गात् उच्चैस्तरात् यत्फलं प्राप्यं लभ्यं तत्फलं समृद्धादैश्वर्यात् । धनेश्वरादेर्न प्राप्यं न लभ्यं । कस्मादिवाद्रेरिव । यथा निराम्भसोऽपि निरुदकात् उच्चतमात् अद्रेः पर्वतात् सकाशात् धुनी नदी निर्याति निर्गच्छतीत्यर्थः । साम्भसोऽपि पयोधेः समुद्रादेकापि धुनी न निर्याति। तथाऽसङ्गात् उच्चतमाद्भवतः सकाशात् यत्फलं लभ्यते तत्फलं समृद्धादप्यन्य-स्मान्नेति तात्पर्यम्।
भावार्थ- पहाड़ के पास पानी की एक बूँद भी नहीं है । परन्तु उसकी प्रकृति अत्यन्त उन्नत है इसलिए उससे कई नदियाँ निकलती हैं, परन्तु समुद्र से जो कि पानी से लवालव भरा रहता है एक भी नदी नहीं निकलती। इसका कारण है - समुद्र में ऊँचाई का अभाव। भगवन्! मैं जानता हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है। परन्तु आपका हृदय पर्वत की तरह उन्नत है-दीन नहीं है, इसलिए आपसे हमें जो चीज मिल सकती है वह अन्य धनाढ्यों से नहीं मिल सकती क्योंकि समुद्र के समान वे भी ऊँचे नहीं हैं अर्थात् कृपण हैं ।
पुण्यातिशय का प्रभाव
त्रैलोक्यसेवानियमाय दण्डं दधे यदिन्द्रो विनयेन तस्य ।
तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु॥२०॥
अन्वयार्थ– (यत्) जिस कारण से (इन्द्रः) इन्द्र ने (विनयेन) विनयपूर्वक (त्रैलोक्यसेवानियमाय ) तीन लोक के जीवों की सेवा के नियम के लिए अर्थात् मैं त्रिलोक के जीवों की सेवा करूँगा और उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाऊँगा, इस उद्देश्य से (दण्डम्) दण्ड (दध्रे) धारण किया था। (तत्) उस कारण से (प्रातिहार्यम्) प्रतीहारपना (तस्य स्यात्) उस इन्द्र के ही हो (भवतः कुतस्त्यम्) आपके कहाँ से आया? (यदि वा) अथवा (तत्कर्म-योगात्) तीर्थंकर नामकर्म का संयोग होने से या इन्द्र के उस कार्य में प्रेरक होने से (तव अस्तु) आपके भी प्रातिहार्य-प्रतिहारपना हो ।
टीका- भो देव! इन्द्रो विनयेन कृत्वा त्रैलोक्यस्य सेवा तस्या नियमो निश्चयस्तस्मै । यत् यदि चेद्दण्डं दध्रेऽदधात् तत्तर्हि तस्य इन्द्रस्य प्रातिहार्य भवतस्तव कुतस्त्यं । प्रतिहारस्य भावः प्रातिहार्यं । यदि वा युक्तोऽयमर्थः। तस्य तीर्थकृन्नाम-कर्मणो योगात् तव भगवतो अस्तु ।
भावार्थ– जब भगवान् ऋषभनाथ भोगभूमि के बाद कर्मभूमि की व्यवस्था करने के लिए तैयार हुए तब इन्द्र ने आकर भगवान् की इच्छानुसार सब व्यवस्था करने के लिए दण्ड धारण किया था। अर्थात् प्रतीहार पद स्वीकार किया था। जो किसी काम की व्यवस्था करने के लिए दण्ड धारण किया करता है उसे प्रतीहार कहते हैं । जैसे कि आजकल लाठी धारण किये हुये बालन्टियर - स्वयंसेवक । प्रतीहार के कार्य अथवा भाव को संस्कृत में प्रातिहार्य कहते हैं। हे प्रभो! जब इन्द्र ने सब व्यवस्था की थी तब सच्चा ‘प्रातिहार्य’ प्रतिहारपना इन्द्र के ही हो सकता है, आपके कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने प्रतीहारका काम थोड़े ही किया था। फिर भी यदि आपके प्रातिहार्य होता ही है ऐसा कहना है तो उपचार से कहा जा सकता है। क्योंकि आप इन्द्र के उस काम में प्रेरक थे।
अथवा श्लोक का ऐसा भी भाव हो सकता है- "तीनलोक के जीव भगवान् की सेवा करो " इस नियम को प्रचलित करने के लिए इन्द्र ने हाथ में दण्ड लिया था, इसलिए प्रातिहार्य इन्द्र के ही बन सकता है, आपके नहीं। अथवा आपके भी हो सकता है क्योंकि आपसे ही इन्द्र की उस क्रिया के कर्मकारक का सम्बन्ध होता था । यहाँ एक और भी गुप्त अर्थ है, वह इस प्रकार है-लोक में प्रातिहार्य पदका अर्थ आभूषण प्रसिद्ध है। भगवान् के भी अशोक वृक्ष आदि आठ प्रातिहार्य आभूषण होते हैं। यहाँ कवि, प्रातिहार्य पदके श्लेष से पहले यह बतलाना चाहते हैं कि संसार के अन्य देवों की तरह आपके शरीर पर प्रातिहार्य नहीं हैं । इन्द्र के प्रातिहार्य-प्रतीहारपना हो पर आपके प्रातिहार्य आभूषण कहाँ से आये? फिर उपचार पक्ष का आश्रय लेकर कहते हैं कि आपके भी प्रातिहार्य हो सकते हैं। उसका कारण है तत्कर्मयोगात् अर्थात् आभूषणों के कार्य- सौंदर्य वृद्धि के साथ सम्बन्ध होना ।
सम द्रष्टा
श्रिया परं पश्यति साधु निः स्वः श्रीमान्न कश्चित्कृपणं त्वदन्यः ।
यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस्थायीक्षतेऽसौ न तथा तमः स्थम् ॥२१॥
अन्वयार्थ– (निःस्वः) निर्धन पुरुष (श्रिया परम्) लक्ष्मी से श्रेष्ठ अर्थात् सम्पन्न मनुष्य को (साधु) अच्छी तरह - आदरभाव से (पश्यति) देखता है, किन्तु (त्वदन्यः ) आपसे भिन्न ( कश्चित्) कोई (श्रीमान्) सम्पत्तिशाली पुरुष (कृपणम्) निर्धन को (साधु न पश्यति) अच्छे भावों से नहीं देखता। ठीक है ( अन्धकारस्थायी) अन्धकार में ठहरा हुआ मनुष्य (प्रकाशस्थितम्) उजाले में ठहरे हुए पुरुष को (यथा) जिस प्रकार (ईक्षते) देख लेता है (तथा) उस प्रकार (असौ ) यह उजाले में स्थित पुरुष (तमःस्थम्) अँधेरे में स्थित पुरुष को (न ईक्षते) नहीं देख पाता।
टीका— भो देव! त्वत्तः सकाशात् अन्यः कः निस्वः दरिद्रिश्रिया लक्ष्म्या परमुत्कृष्टं साधु यथा स्यात्तथा पश्यति विलोकयति । त्वदन्यः श्रीमान् कृपणं साधु न पश्यति । यथा अन्धकारस्थायी पुमान् प्रकाशस्थितं पुरुषमीक्षते पश्यति तथाऽसौ प्रकाशस्थायी पुमान् तमस्थं पुरुषं नेक्षते नालोकयति । प्रकाशे स्थितस्तं। अन्धकारे तमसि तिष्ठतीति तम् ।
भावार्थ- हे प्रभो ! संसार के श्रीमान् निर्धन पुरुषों को बुरी निगाह से देखते हैं, पर आप श्रीमान् होते हुए भी ज्ञानादि सम्पत्ति से रहित मनुष्यों को बुरी निगाह से नहीं देखते। उन्हें भी अपनाकर हितका उपदेश दे सुखी करते हैं। इस तरह आप संसार के अन्य श्रीमानों से भिन्न ही श्रीमान् हैं। दोनों की श्री - लक्ष्मी में भेद जो ठहरा। उनके पास रुपया चांदी सोना वगैरह जड़ लक्ष्मी है पर आपके पास अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य- अनन्त चतुष्टय रूप लक्ष्मी है।
इन्द्रिय अगोचर
स्ववृद्धिनिःश्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः ।
किं चाखिलज्ञेयविवर्तिबोध स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः ॥ २२॥
अन्वयार्थ—(प्रत्यक्षं) यह प्रकट है कि [यः] जो मनुष्य (स्ववृद्धि- निःश्वास - निमेषभाजि ) अपनी वृद्धि, श्वासोच्छ्वास और आँखों की टिमकार को प्राप्त (आत्मानुभवे अपि) अपने आपके अनुभव करने में (मूढः) मूर्ख है ( स लोकः) वह मनुष्य (अखिलज्ञेयविवर्तिबोधस्वरूपं) सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला ज्ञान ही है स्वरूप जिसका ऐसे (अध्यक्ष) अध्यात्मस्वरूप आपको (किं च अवैति) कैसे जान सकता है?
टीका - लोक आत्मानुभवेऽपि निजस्वरूपानुभवेऽपि । प्रत्यक्षं साक्षात् । मूढो मूर्खो वर्तते । आत्मनोऽनुभवः आत्मानुभवस्तस्मिन्। च पुनः लोकोऽखिल-ज्ञेयविवर्त्तिबोधस्वरूपं अध्यक्षं मम प्रत्यक्षं किमवैति जानाति ? अपि तु न जानातीत्यर्थः । अखिलाश्च ते ज्ञेयाः पदार्थास्तेषां विवर्तिनः पर्यायास्तेषां बोधस्तस्य स्वरूपं तत्त्वं । कथंभूते आत्मानुभवे? स्ववृद्धि- निश्वास-निमेषभाजि। स्ववृद्धिश्च निश्वासश्च निमेषाश्च तान् भजतीति तस्मिन् ।
भावार्थ- भगवन्! जो मनुष्य अपने आपके स्थूल पदार्थों को भी जानने के लिए समर्थ नहीं है वह ज्ञानस्वरूप तथा आत्मा में विराजमान आपको कैसे जान सकता है? अर्थात् नहीं जान सकता।
स्वरूप अनभिज्ञ अज्ञानी
तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव ! त्वां येऽवगायन्ति कुलं प्रकाश्य ।
तेऽद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यं पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति ॥ २३ ॥
अन्वयार्थ - (देव!) हे नाथ! (ये) जो मनुष्य, आप (तस्य आत्मजः) उसके पुत्र हो और (तस्य पिता) उसके पिता हो (इति) इस प्रकार (कुलम् प्रकाश्य) कुल का वर्णन कर (त्वाम् अवगायन्ति) आपका अपमान करते हैं (ते) वे (अद्य अपि) अब भी (पाणौ कृतम्) हाथ में आये हुए (हेम) सुवर्ण को (आश्मनम्) पत्थर से पैदा हुआ है, (इति) इस हेतु से (पुनः) फिर (अवश्यं त्यजन्ति) अवश्य ही छोड़ देते हैं?
टीका - भो देव! ये लोकास्त्वां भगवन्तं अवगायन्ति । किं कृत्वा तस्य श्री - नाभेरात्मजः पुनस्तस्य श्रीभरतचक्रवर्तिनः पितेत्यमुना प्रकारेण कुलं प्रकाश्य प्रकटीकृत्य । ते पुरुषा अद्यापि ननु निश्चितं । पाणौ करकमले । कृतं हेम सुवर्णं अवश्यं निश्चितमाश्मनं पाषाणोद्भवं इति विलोक्य पुनस्त्यजति जहतीत्यर्थः।
भावार्थ - एक तो सुवर्ण हाथ नहीं लगता, यदि किसी तरह लग भी जावे तो उसे यह सोचकर कि इसकी उत्पत्ति पत्थरों से हुई है, फिर अलग कर देना मूर्खता है। इसी तरह आपका श्रद्धान व ज्ञान सबको नहीं होता। यदि किसी को हो भी जावे तो वह आपको मनुष्य कुल में पैदा बतलाकर फिर भी छोड़ देता है, यह सबसे बढ़कर मूर्खता है। सुवर्ण यदि शुद्ध है तो फिर वह पत्थर से तो क्या दुनियाँ के किसी हल्के से हल्के पदार्थ से उत्पन्न हुआ हो तो बाजार में उसकी कीमत पूरी ही लगेगी और मैल सहित है-अशुद्ध है तो किसी अच्छे पदार्थ से भी उत्पन्न होने पर भी उसकी पूरी कीमत नहीं लग सकती । इसी प्रकार जो आत्मा शुद्ध है, कर्ममल से रहित है, भले ही वह उस पर्याय में नीच कुल में पैदा हुआ हो, पूज्य कहलाता है और यदि वही आत्मा उच्च कुल में पैदा होकर भी अशुद्ध है-मलिन है तो उसे कोई पूछता भी नहीं है ।
मोहविजयी भगवन्
दत्तस्त्रिलोक्यां पटहोभिभूताः सुरासुरास्तस्य महान् स लाभः ।
मोहस्य मोहस्त्वयि को विरोद्धम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः ॥ २४ ॥
अन्वयार्थ- मोह के द्वारा (त्रिलोक्याम्) तीनों लोकों में (पटहः) विजय का नगाड़ा (दत्तः) दिया गया / बजाया गया उससे जो (सुरासुराः) सुर और असुर (अभिभूताः) तिरस्कृत हुए (सः) वह (तस्य) उस मोह का (महान् लाभः) बड़ा लाभ हुआ किन्तु ( त्वयि ) आपके विषय में (विरोद्धुम् ) विरोध करने के लिए (मोहस्य) मोह का (कः) कौन-सा (मोहः) भ्रम हो सकता था अर्थात् कोई नहीं, क्योंकि ( बलवद्विरोध: ) बलवान् के साथ विरोध करना (मूलस्य नाशः) मानो मूल का नाश करना है।
टीका - भो देव! मोहस्य मोहनीयकर्मणः । त्वयि विषये विरोद्धुं स्पर्धायितुं को मोहः भ्रमः । समानबलाय स्पर्धा न तु न्यूनाधिकयोः। तस्य मोहस्य स महान् लाभो यः सुरासुरा देवदानवादयोऽभिभूताः पराभूता इति त्रैलोक्ये पटहो दत्तः । कुत एवं भ्रमतः ? बलवद्भिः सह विरोधो मूलस्य नाशो भवति ।
भावार्थ– हे भगवन्! जिस मोह ने संसार के सब जीवों को अपने वश कर लिया उस मोहको भी आपने जीत लिया है अर्थात् आप मोहरहित- रागद्वेषशून्य हैं।
अभिमान रहित भगवन्
मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेः चतुर्गतीनां गहनं परेण ।
सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः ॥२५॥
अन्वयार्थ– (त्वया) आपके द्वारा (एकः) एक (विमुक्ते:) मोक्ष काही (मार्ग) मार्ग (ददृशे) देखा गया है और ( परेण ) दूसरों के द्वारा (चतुर्गतीनाम्) चारों गतियों का (गहनम् ) सघन वन (ददृशे) देखा गया है, मानो इसीलिए (त्वम्) आपने (मया सर्वं दृष्टम्) मैंने सब कुछ देखा है (इति स्मयेन) इस अभिमान से (कदाचित् ) कभी भी (भुजम्) अपनी भुजा को (मा आलुलोके) नहीं देखा था ।
टीका— भो नाथ! त्वया भगवता । एकोऽद्वितीयो विमुक्तेर्मार्गो ददृशे दर्शितः । परेण हरिहरादिदेवेन । चतुर्गतीनां नरकतिर्यग्देवमनुष्यपर्याणां । गहनं ददृशे दर्शितं । भो देव! मया सर्वं दृष्टमिति स्मयेनेत्यहंकारभरेण त्वं कदाचित् भुजं निजबाहुशिखरं मालुलोकः माद्राक्षीः । इति निन्दा-स्तुत्यलङ्कारविष्टम्भेन त्वमेव मुक्तोऽन्ये सर्वेऽपि संसारिणः इति तात्पर्यम्।
भावार्थ– घमण्डियों का स्वभाव होता है कि वे अपने को बड़ा समझकर बार-बार अपनी भुजाओं की तरफ देखते हैं, पर आपने घमण्ड से कभी अपनी भुजा की तरफ नहीं देखा । उसका कारण यह है कि आप सोचते थे कि मैंने तो सिर्फ एक मोक्ष का ही रास्ता देखा है और अन्य देवी देवता चारों गतियों के रास्तों से परिचित हैं इसलिए मैं उनके सामने अल्पज्ञ हूँ । अल्पज्ञ का बहुज्ञानियों के सामने अभिमान कैसा? श्लोक का तात्पर्य यह है कि आप अभिमान से रहित हैं और निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, परन्तु अन्य देवता अपने अपने कार्यों के अनुसार नरक आदि चारों गतियों में घूमा करते हैं ।
विरोधी रहित अविनाशी
स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः ।
संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये ॥२६॥
अन्वयार्थ– जैसे (अर्कस्य) सूर्य का ( स्वर्भानुः) राहु, (हविर्भुजः) अग्नि का (अम्भः) पानी, (अम्बुनिधेः ) समुद्र का ( कल्पान्तवातः) प्रलयकालीनवायु तथा (संसारभोगस्य) संसार के भोग का (वियोगभावः) विरहभाव, (विघातः) नाश करने वाले हैं, इस तरह ( त्वदन्ये) आपसे भिन्न सब पदार्थ (विपक्षपूर्वाभ्युदया: ‘सन्ति’) अपने विपक्ष रूप शत्रु युक्त अभ्युदय वाले हैं। अर्थात् विनाश के साथ ही उदय होते हैं।
टीका - भो देव! त्वत्तः सकाशात् अन्ये यावन्तः पदार्थाः सन्ति तावन्ते विपक्षपूर्वाभ्युदयाः सन्ति । विपक्षपूर्वः शत्रुपूर्वः अभ्युदयो भाग्यमेषां ते । अर्कस्य सूर्यस्य स्वर्भानुः राहुर्विघातोस्ति । हविर्भुजोऽग्नेरम्भस्तोयं विघातं । अम्बुनिधेः समुद्रस्य कल्पान्तवातो विघातः । संसारभोग्यस्य स्रक्चन्दन- वनितादेर्वियोगभावो विघातः । इति विपक्षपूर्वाः सर्वे। त्वमेव नेति भावः।
भावार्थ- हे प्रभो ! संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं, सिर्फ आप ही सामान्य स्वरूप की अपेक्षा नित्य हैं अर्थात् आप जन्म मरण से रहित हैं और आपकी यह विशुद्धता भी कभी नष्ट नहीं होती ।
आपको नमस्कार निष्फल नहीं
अजानतस्त्वां नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति।
हरिन्मणिं काचधिया दधानः तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः ॥ २७॥
अन्वयार्थ– (त्वाम्) आपको (अजानतः) बिना जाने ही (नमतः ) नमस्कार करने वाले पुरुष को (यत् फलम् ) जो फल होता है, (तत्) वह फल (अन्यं देवता इति जानतः) दूसरे को ‘देवता है’ इस तरह जानने वाले पुरुष को (न तु) नहीं होता। क्योंकि (हरिन्मणिम्) हरे मणि को (काचधिया) काच की बुद्धि से (दधानः) धारण करने वाला पुरुष (तं तस्य बुद्धया वहतः) हरे मणि को हरे मणि की बुद्धि से धारण करने वाले पुरुष की अपेक्षा (रिक्त: न ) दरिद्र नहीं है ।
टीका - भो नाथ! त्वामष्टविधप्रातिहार्यविभवालंकृतं त्वामजानतो नमतः पुरुषस्य यत्फलं स्यात् । तु पुनरन्यं कञ्चन देवतेति जानतो नमतः पुरुषस्य तत्फलं न स्यात् । काचधिया काचबुद्ध्या हरिन्मणि नीलरत्नं दधानः पुमांस्तस्य हरिन्मणिर्बुद्ध्या तं काच वहतः पुरुषात् सकाशात् रिक्तो न।
भावार्थ- हे भगवन्! जो आपको नमस्कार करता है पर आपके स्वरूप को नहीं जानता, उसे भी जो पुण्यबंध होता है वह किसी दूसरे को देवता मानने वाले पुरुष को नहीं होता। जिस तरह कोई अजान मनुष्य हरित मणिको पहन कर उसे काँच समझता है तो वह दूसरे की निगाह में जो मणि को मणि समझकर पहन रहा है निर्धन नहीं कहलाता। वे दोनों एक जैसी सम्पत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। श्रद्धा और विवेक के साथ प्राप्त हुआ अल्पज्ञान भी प्रशंसनीय है।
अज्ञानियों की मान्यता
प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैः दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः ।
गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् ॥२८॥
अन्वयार्थ - ( प्रशस्तवाचः ) सुन्दर वचन बोलने वाले (चतुराः) चतुर मनुष्य ( कषायैः दग्धस्य) कषायों से जले हुए पुरुष के भी (देवव्यवहारं आहुः) देव शब्द का व्यवहार करना कहते हैं । सो ठीक ही है (हि) क्योंकि ( गतस्य दीपस्य) बुझे हुए दीपक का (नन्दितत्वं) बढ़ना (च) और (कपालस्य) फूटे हुए घड़े का (मङ्गलत्वं) मंगलपन (दृष्टम्) देखा गया है।
टीका - प्रशस्ता प्रशस्या वाग् वाणी येषां ते चतुरा पुमान्सः । कषायैः क्रोधमानमायालोभादिभिः । दग्धस्य पुन्सः । देव परमेश्वरस्तस्य व्यवहार- माहुर्भणन्ति स्म । हि निश्चितं । तैः पुरुषैः। गतस्य प्रनष्टस्य दीपस्य नन्दितत्वं वर्धमानत्व दृष्टं । च पुनस्तै, कपालस्य खर्परस्य मङ्गलत्वं माङ्गल्यं दृष्टम्।
भावार्थ- हे भगवन्! लौकिक मनुष्य रागी द्वेषी जीवों के भी दे शब्द का व्यवहार करते हैं सो सिर्फ लोकव्यवहार से ही किसी बात की सत्यता नहीं होती। क्योंकि लोक में कितनी ही बातों का उल्टा व्यवहार होता है। जैसे कि जब दीपक बुझ जाता है तब लोग कहते हैं कि दीपक बढ़ गया। और जब घड़ा फूट जाता है तब लोग कहने लगते हैं कि घड़े का कल्याण हो गया ।
हितकारी निर्दोष उपदेशक
नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः ।
निर्दोषतां के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण ॥२९॥
अन्वयार्थ–(नानार्थम्) अनेक अर्थों के प्रतिपादक तथा (एकार्थम्) एक ही प्रयोजन युक्त (त्वदुक्तम्) आपके कहे हुए (अद: हितं वचः) इन हितकारी वचनों को (निशम्य) सुनकर (के) कौन मनुष्य (ते वक्तुः) आपके जैसे वक्ता की (निर्दोषताम् ) निर्दोषता को (न विभावयन्ति) नहीं अनुभव करते हैं अर्थात् सभी करते हैं। जैसे [य] जो (ज्वरेण मुक्तः ‘भवति’) ज्वर से मुक्त हो जाता है (सः) वह (स्वरेण सुगमः ‘भवति’) स्वर से सुगम हो जाता है। अर्थात् स्वर से उसकी अच्छी तरह पहचान हो जाती है।
टीका - भो देव! त्वदुक्तं त्वया प्रणीतमदः प्रसिद्धवचो । निशम्य श्रुत्वा । ते तव । वक्तुर्निर्दोषतां दोषरहितत्वं । के पुरुषा न विभावयन्ति । ज्वरेण मुक्तः पुमान् स्वरेण कृत्वा सुगमः सुखेन ज्ञेयो भवति । कीदृशं वचो ? नानाबहवोऽर्था यस्मिन् तत् । कथंभूतमेकोऽद्वितीयः पूर्वापर-विरोधरहितः अर्थो यस्मिन् तत् । पुनः हितं हितकारी । दोषन्निष्क्रान्तो निर्दोषस्तस्य भावस्ताम्।
भावार्थ- आपके वचन नानार्थ होकर भी एकार्थ हैं। यह प्रारम्भ में विरोध मालूम होता है पर अन्त में उसका इस प्रकार परिहार हो जाता है कि आपके वचन स्याद्वाद सिद्धान्त से अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने वाले हैं, फिर भी एक ही प्रयोजन को सिद्ध करते हैं अर्थात् पूर्वापर विरोध से रहित हैं । हे भगवन्! आपके हितकारी वचनों को सुनकर यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि आप निर्दोष हैं क्योंकि सदोष पुरुष वैसे वचन नहीं बोल सकता जैसे कि किसी की अच्छी आवाज सुनकर साफ मालूम जाता है कि वह ज्वर से मुक्त है क्योंकि ज्वर से पीड़ित मनुष्य का स्वर अच्छा नहीं होता।
स्वभाव से उपकारी
न क्वापि वाञ्छा ववृते च वाक्ते काले क्वचित्कोऽपि तथा नियोगः ।
न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति ॥३०॥
अन्वयार्थ - (ते) आपकी (क्वापि ) किसी भी वस्तु में (वाञ्छा न) इच्छा नहीं है (च) और (वाक् वतृते) वचन प्रवृत्त होते हैं । सचमुच में (क्वचित् काले ) किसी काल में (तथा) वैसा (कः अपि नियोगः) कोई नियोग-नियम ही होता है। (हि) क्योंकि (शीतद्युतिः) चन्द्रमा (अम्बुधिम् पूरयामि) मैं समुद्र को पूर्ण कर दूँ (इति) इसलिए ( उदंशुः न भवति ) उदित नहीं होता किन्तु (स्वयम् अभ्युदेति) स्वभाव से उदित होता है।
टीका - भो देव! तव भगवतः क्वापि कस्मिश्चिदपि वस्तुनि वाञ्छा न । च पुनः वाग्ववृते प्रवर्तिता दिव्यध्वनिः प्रवर्त्तित इति भावः । क्वचित्काले कोऽपि अनिर्वचनीयस्तथा नियोगोऽस्ति । शीतद्युतिश्चन्द्रः अम्बुधिं पूरयामीत्युदंशुर्न हि स्वयमभ्युपैति । उदेति क्वचित्काले कोऽपि यथा तस्य नियोगोऽस्ति तथैवेति भावः ।
भावार्थ- जिस प्रकार चन्द्र यह इच्छा रख कर उदित नहीं होता कि मैं समुद्र को लहरों से भर दूँ पर उसका वैसा स्वभाव ही है कि चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, इसीप्रकार आपके यह इच्छा नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ पर वैसा स्वभाव होने से आपके वचन प्रकट होने लगते हैं।
अनन्तगुणध
गुणा 'गभीरा: परमाः प्रसन्ना बहुप्रकारा बहवस्तवेति ।
दृष्टोऽयमन्तः स्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति ॥३१॥
अन्वयार्थ – (तव) आपके (गुणाः) गुण (गभीराः) गम्भीर (परमा) उत्कृष्ट (प्रसन्नाः) उज्ज्वल (बहुप्रकाराः ) अनेक प्रकार के और (बहवः) बहुत हैं (इति) इस प्रकार (अयम्) यह ( स्तवनेन ) स्तुति द्वारा ही (तेषाम् गुणानाम् ) उन गुणों का (अन्तः दृष्ट:) अन्त देखा गया है (अतः परः गुणानाम् अन्तः किम् अस्ति ) इसके सिवाय गुणों का अन्त क्या होता है? अर्थात् नहीं ।
टीका - भो नाथ! तव भगवतो गुणा गभीराः अगाधाः । परमा उत्कृष्टाः । प्रसन्ना निर्मलाः । बहुप्रकारा नानाविधाः । बहवोऽनन्ता । इति स्तवनेन कृत्वा। गुणानामयन्तः पारो दृष्टस्तेषां गुणानामन्तः परः किमस्ति ।
भावार्थ- हे भगवन्! आपके निर्मल गुण संख्या रहित और अनुपम है।
सर्वसिद्धि प्रदायी उपासना
स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि ।
स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् ॥३२॥
अन्वयार्थ - (स्तुत्या हि) स्तुति के द्वारा ही (अभिमतम् न) इच्छित वस्तु की सिद्धि नहीं होती (परम् ) किन्तु (भक्त्या स्मृत्या च प्रणत्या ) भक्ति, स्मृति और नमस्कृति से भी होती है (ततः) इसलिए मैं (नित्यम्) हमेशा (देवम् भजामि-स्मरामि -प्रणमामि ) आप देव को भजता हूँ/ भक्ति करता हूँ, स्मरण करता हूँ और प्रणाम करता हूँ (हि) क्योंकि (फलम् ) इच्छित वस्तु की प्राप्ति रूप फल को (केन अपि उपायेन) किसी भी उपाय से (साध्यम्) सिद्ध कर लेना चाहिए।
टीका - भो देव! हि निश्चितं । परं केवलं । स्तुत्या कृत्वा मनोऽभि- लषितं न। तत्तस्मात्कारणात् भक्त्या देवमहं भजामि। च पुनः। देवं नित्यं स्मरामि । च पुनः । प्रणत्या देवं नित्यं प्रणमामि । हि निश्चितं प्राणिनां नाप्युपायेन गुणानां फलं साध्यमुपार्जनीयं ।
भावार्थ- हे भगवन्! आपकी स्तुति से, भक्ति से, स्मृति - ध्यान से और प्रणति से जीवों को इच्छित फलों की प्राप्ति होती है इसलिए मैं प्रतिदिन आपकी स्तुति करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। क्योंकि मुझे जैसे बने तैसे अपना कार्य सिद्ध करना है।
पुण्य के प्रधान कारण
ततस्त्रिलोकीनगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् ।
अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् ॥३३॥
अन्वयार्थ – (ततः) इसलिए (अहम् ) मैं (त्रिलोकी नगराधिदेवम्) तीन लोक रूप नगर के अधिपति, (नित्यम्) विनाशरहित, (परम् ) श्रेष्ठ (ज्योतिः) ज्ञान - ज्योति स्वरूप (अनन्तशक्तिम्) अनन्तवीर्य / अनन्तशक्ति से सहित, (अपुण्यपापम्) स्वयं पुण्य और पाप से रहित होकर भी (परपुण्यहेतुम्) दूसरे के पुण्य के कारण तथा (वन्द्यम्) वन्दना करने के योग्य होकर भी स्वयं ( अवन्दितारम् ) किसी की भी वन्दना नहीं करने वाले [भवन्तम्] आपको ( नमामि ) मैं नमस्कार करता हूँ ।
टीका - ततस्तस्मात्कारणात् अहं त्रिलोकीनगराधिदेवं नमामि । त्रयाणां लोकानां समाहारस्रिलोकी सैव नगरं तस्याधिदेवः स्वामी तं । कीदृशं देवं? नित्यं शश्वद्भावापन्नं । पुनः कथंभूतं? परंज्योतिषा परं ज्ञाननेनानंतवीर्य यस्य सतं । पुनः कथंभूतं? न विद्येते पुण्यपापे यस्य तं । पुनः परेषां प्राणिनां पुण्ये हेतुः पुण्यकारणं तं । पुनः कथंभूतं ? वन्द्यं सुरासुरादिशतेन्द्रैस्तुत्यं । पुनः कथंभूतं? अवन्दितारं अवन्दकं । वन्दतेऽसौ वंदकः न वन्दकोऽवंदकस्तं।
भावार्थ– हे भगवन्! आप तीन लोक के स्वामी हैं, आपका भी विनाश नहीं होता, सर्वोत्कृष्ट हैं, केवल ज्ञानरूप ज्योति से प्रकाशमान हैं, आपमें अनन्त बल है, आप स्वयं पुण्य पाप से रहित हैं, पर अपने भक्तजनों के पुण्यबन्ध में निमित्त कारण हैं, आप किसी को नमस्कार नहीं करते पर सब लोग आपको नमस्कार करते हैं । आपकी इस विचित्रता से मुग्ध हो मैं भी आपके लिए नमस्कार करता हूँ ।
सदा स्मरणीय
अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् ।
सर्वस्य मातारममेयमन्यैर् जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि ॥३४॥
अन्वयार्थ - (अशब्दम्) शब्दरहित, (अस्पर्शं) स्पर्शरहित (अरूप- गन्धं) रूप और गन्धरहित तथा (नीरसं) रसरहित होकर भी (तद्विषयाव- बोधं) उनके ज्ञान से सहित, (सर्वस्य मातारं ) सबके जानने वाले होकर भी (अन्यैः) दूसरों के द्वारा (अमेयं) नहीं जानने के योग्य तथा (अस्मार्यं) जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता ऐसे (जिनेन्द्रं त्वां अनुस्मरामि ) जिनेन्द्र भगवान् आपका प्रतिक्षण मैं स्मरण करता हूँ-ध्यान करता हूँ ।
टीका - त्वां जिनेन्द्रमहमनुस्मरामि नित्यं ध्यायामि । कथंभूतं त्वां ? न विद्यते शब्दो यस्य स तं । न स्पर्शो यस्य स तं । न रूपगन्धौ यस्य स तं । रसान्निष्क्रान्तो यः स तं । पुनः त एव विषयाः स्पर्शरसगंधवर्णशब्दास्तेषां । अवबोधो ज्ञानं यस्य स तं । सर्वस्य त्रैलोक्यस्य दंडाकारेण घनाकारेण माता प्रमापकस्तं । पुनः माया ज्ञानस्य विषयो मेयः न मेयोऽमेयस्तं । कैरन्यैर्लोकैः पुनः स्मारयतीति स्मार्यः न स्मार्यः अस्मार्यस्तं । अस्मारक - मित्यर्थः ।
भावार्थ- हे भगवन्! आप रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द से रहित हैं - अमूर्तिक हैं, फिर भी उन्हें जानते हैं । आप सबको जानते हैं पर आपको कोई नहीं जान पाता । यद्यपि आपका मन से भी कोई स्मरण नहीं कर सकता तथापि मैं अपने बाल साहस से आपका क्षण-क्षण में स्मरण करता हूँ।
सत्य शरण रूप
अगाधमन्यैर्मनसाप्यलंघ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः ।
विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि ॥३५॥
अन्वयार्थ —– (अगाधं) गम्भीर (अन्यैः) दूसरों के द्वारा (मनसा अपि अलंघ्यं) मन से भी उल्लंघन करने के अयोग्य अर्थात् अचिन्त्य (निष्किञ्चनं) निर्धन होने पर भी ( अर्थवद्भिः) धनाढ्यों के द्वारा (प्रार्थितं) याचित (विश्वस्य पारं) सबके पारस्वरूप होने पर भी (अदृष्टपारं) जिनका पार / अन्त कोई नहीं देख सका है, ऐसे (तम् जिनानां पतिं) उन जिनेन्द्रदेव की मैं (शरणम् व्रजामि) शरण को प्राप्त होता हूँ ।
टीका - अहं तं जिनानां पतिं गणधरदेवानां स्वामिनं प्रति शरणं व्रजामि यामीत्यर्थः। कथम्भूतं तं? अगाधं गम्भीरमित्यर्थः । पुनः अन्यैर्लोकैः मनसाप्यलंघ्यं लङ्घितुमशक्यं । पुनः निष्किञ्चनमसंगं चतुर्विंशतिधा परिग्रहरहितत्वात् । पुनः अर्थवद्भिर्लोकैः प्रार्थितं । पदार्थवद्भिर्धनेश्वररैर्वा याचितं मनोभिलषित-दातृत्वात् ! पुनः विश्वस्य त्रैलोकस्य पारं प्राप्तं लोकप्रकाशक- ज्ञानाधिष्ठातृत्वात् । अदृष्टपारं न दृष्टः पारो यस्य स तं ।
** **हे भगवन्! आप बहुत ही गम्भीर - धैर्यवान् हैं। आपका कोई मनसे भी चिन्तन नहीं कर सकता । यद्यपि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी धनिक लोग (अथवा याचकवर्ग) आपसे याचना करते हैं, आप सबके पार को जानते हैं, पर आपके पार को कोई नहीं जान सकता और आप जगत के जीवों के पति-रक्षक हैं ऐसा सोचकर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ।
स्वाभाविक गुणों से उन्नत
त्रैलोक्यदीक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत् ।
प्राग्गण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः पश्चान्नमेरुः कुलपर्वतोऽभूत्॥३६॥
अन्वयार्थ – (त्रैलोक्यदीक्षागुरवे ते नमः ) त्रिभुवन के जीवों के दीक्षागुरुस्वरूप आपके लिए नमस्कार हो (यः) जो आप (वर्धमानः अपि) क्रम से उन्नति को प्राप्त होते हुए भी (निजोन्नतः) स्वयमेव उन्नत (अभूत्) हुए थे । (मेरुः ) मेरुपर्वत (प्राक् ) पहले (गण्डशैलः) गोल पत्थरों का ढेर, (पुनः) फिर (अद्रिकल्पः ) पहाड़ तुल्य (पश्चात् ) फिर (कुलपर्वतः) कुलाचल (न अभूत्) नहीं हुआ था किन्तु स्वभाव से ही वैसा था।
टीका- भो भगवन् ते तुभ्यं नमः । कथंभूताय ते? त्रैलोकस्याधो- मध्योर्ध्वलोकोद्भूतजनस्य दीक्षोपदेशसूत्रगुरुस्तस्मै । यस्त्वं वर्द्धमानोऽपि सन् निजोन्नतः स्वमेवोन्नतोऽभूत् । मेरुः सुदर्शनः । प्राग् पूर्व। गण्डशैलः सन् पुनरद्रिकल्पः पर्वततुल्योऽभूत। पश्चाद्वर्द्धमानोऽपि कुलपर्वतः नाभूत् न बभूव ।
भावार्थ - हे प्रभो ! आप तीन लोक के जीवों के दीक्षागुरु हैं इसलिए आपको नमस्कार हो । इस श्लोक के द्वितीय पाद में विरोधाभास अलंकार है। वह इस तरह कि आप अभी वर्धमान हैं अर्थात् क्रम से बढ़ रहे हैं फिर भी निजोन्नत-अपने आप उन्नत हुये थे। जो चीज अभी बढ़ रही है वह पहले उससे छोटी ही होती है न कि बड़ी, पर यहाँ इससे विपरीत बात है। विरोध का परिहार इस प्रकार है कि आप वर्धमान - अन्तिम तीर्थकर होकर भी स्वयमेव उन्नत थे, न कि क्रम क्रम से उन्नत हुए थे, क्योंकि मेरु पर्वत आज जितना उन्नत है उतना उन्नत हमेशा से ही था न कि क्रम-क्रम से उन्नत हुआ है। यहाँ वर्धमान पद श्लिष्ट है ।
काल विजयी
स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशा वा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् ।
न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतम्॥३७॥
अन्वयार्थ - ( स्वयं प्रकाशस्य यस्य) स्वयं प्रकाशमान रहने वाले जिसके (दिवा निशा वा) दिन और रात की तरह (न बाध्यता न बाधकत्वं) न बाध्यता है और न बाधकपना भी । इसी प्रकार जिनके (न लाघवं गौरवं ) न लाघव है न गौरव भी उन (एकरूपं) एक रूप रहने वाले और (काल - कलां अतीतं) क्षण आदि काल की पर्याय से रहित अर्थात् अन्तरहित (विभुं वन्दे ) परमेश्वर की मैं वन्दना करता हूँ।
टीका - अहं विभुं व्यापकं प्रभुं । वन्दे नमस्करोमि । कथंभूतं तं ? कालस्य कला क्षणादिसलयस्तामतीतं रहितं । यस्य स्वयंप्रकाशस्य भगवतः तव दिवा दिवसो वा अथवा रात्रिर्बाध्यता बाधको न । तयोस्तव बाधकत्वमपि न। तव भगवतो लाघवं गौरवमपि न । कीदृशमेकरूपं ? एकमद्वितीयं ज्योतिर्लक्षणं रूपं यस्य स तम् ।
भावार्थ - स्वयं प्रकाशमान पदार्थ के पास जिस प्रकार रात और दिन का व्यवहार नहीं होता: क्योंकि प्रकाश के अभाव को रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन कहते हैं। जो हमेशा प्रकाशमान रहता है उसके पास अन्धकार न होने से रात का व्यवहार नहीं होता और जब रात का व्यवहार नहीं है तब उसके अभाव में होने वाला दिन का व्यवहार भी नहीं होता, उसी प्रकार आप में भी बाध्यता और बाधक का व्यवहार नहीं है। आप किसी को बाधा नहीं पहुँचाते, इसलिए आप में बाधकत्व नहीं और कोई आपको भी बाधा नहीं पहुँचा सकता इसलिए आप बाध्य नहीं हैं। जिसमें बाय का व्यवहार नहीं उसमें बाधक का भी व्यवहार नहीं होता और जिसमें बाधक का व्यवहार नहीं उसमें बाध्य का भी व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों धर्म परस्पर में सापेक्ष हैं । उसी प्रकार आपमें न लाघव ही है और न गुरुत्व ही । दोनों सापेक्ष धर्मों से रहित हैं। आप अगुरुलघुरूप हैं । हे भगवन्! आप समय की मर्यादा से भी रहित हैं अर्थात् अनन्तकाल तक ऐसे ही रहे आवेंगे।
अयाचित फल प्रदाता
इति स्तुतिं देव! विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि ।
छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात् कश्छायया याचितयात्मलाभः॥३८॥
अन्वयार्थ - (देव) हे देव! (इति स्तुतिं विधाय ) इस प्रकार स्तुति करके मैं (दैन्यात्) दीनभाव से (वरं न याचे) वरदान नहीं माँगता, क्योंकि (त्वं उपेक्षकः असि) आप उपेक्षक - रागद्वेष रहित हो जैसे (तरुं संश्रयतः) वृक्ष का आश्रय करने वाले पुरुष को ( छाया स्वतः स्यात्) छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है । ( याचितया छायया कः आत्मलाभः) छाया की याचना से अपना क्या लाभ है?
टीका - भो देव! इत्यमुना प्रकारेण । स्तुतिं स्तवनं । विधाय दैन्यात् दीनभावात् । अहं वरं न याचे। त्वमुपेक्षकोऽसि । तरुं वृक्षं संश्रयतः पुरुषस्य । स्वतः स्वभावेन छाया स्यात् । तत्र प्रार्थना न लगति। छायया याचितया कः आत्मनः स्वस्य लाभो भवति न कोऽपीत्यर्थः ।
भावार्थ- हे भगवन्! मैं सर्प से डसे हुए मृत प्रायः लड़के को आपके सामने लाया हूँ इसलिए स्तुति कर चुकने के बाद मैं आपसे यह वरदान नहीं माँगता कि आप मेरे लड़के को स्वस्थ कर दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप रागद्वेष से रहित हैं इसलिए न किसी को कुछ देते हैं और न किसी से कुछ छीनते भी हैं । स्तुति करने वाले को तो फल की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है । जैसे- जो मनुष्य वृक्ष के नीचे पहुँचेगा उसे छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है । छाया की याचना करने से कोई लाभ नहीं होता ।
सद्बुद्धि प्रदाता श्रेष्ठ गुरु
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिम् ।
करिष्यते देव तथा कृपां मे कोवात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः ॥ ३९ ॥
अन्वयार्थ - (अथ दित्सा अस्ति) यदि आपकी कुछ देने की इच्छा है (यदि वा) अथवा वरदान माँगो ऐसा (उपरोध: ‘अस्ति’) आग्रह है तो (त्वयि एव सक्तां) आपमें ही लीन (भक्तिबुद्धिं ) भक्तिमयी बुद्धि को (दिश) देओ । मेरा विश्वास है कि (देव) हे देव ! आप (मे) मुझ पर (तथा) वैसी (कृपां करिष्यते) दया करेंगे (आत्मपोष्ये) अपने द्वारा पोषण करने के योग्य शिष्य पर (को वा सूरिः) कौन आचार्य (सुमुखो न ‘भवति’) अनुकूल नहीं होता ! अर्थात् सभी होते हैं ।
टीका - भो देव! अथानन्तरं । यदि चेत् । दित्सा दातुमिच्छास्ति । वाऽथवा । उपरोधोऽनुग्रहोऽस्ति । तर्हि त्वय्येव सक्तां भक्तिबुद्धिः दिश देहि । भक्तेर्बुद्धिस्तां । भक्तिर्विद्यते यस्याः सा तां । भो देव तथा सा भक्तिबुद्धिः मे मम कृपां करिष्यते विधास्यतीति भावः । वा अथवा । आत्मनः स्वस्य पोषकः । सूरिः पंडितः । सुमुखो न स्यात् । आत्मपोषणे सर्वोऽपि सूरिः सुमुखो भवति।
भावार्थ– हे नाथ! यदि आपकी कुछ देने की इच्छा है तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मेरी भक्ति आपमें ही रहे । मेरा विश्वास है कि आप मुझ पर उतनी कृपा अवश्य करेंगे। क्योंकि विद्वान् पुरुष अपने आश्रित रहने वाले शिष्य की इच्छाओं को पूर्ण ही करते हैं।
पुष्पिताग्रा छन्द
भक्ति का वैशिष्ट्य
वितरति विहिता यथाकथञ्चिज्जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः ।
त्वयि नुतिविषया पुनर्विशेषाद्दिशति सुखानि यशो धनं जयं च ॥४०॥
अन्वयार्थ - (जिन) हे जिनेन्द्र ! (यथाकथञ्चित् ) जिस किसी तरह (विहिता) की गई (भक्तिः) भक्ति (विनताय) नम्र मनुष्य के लिए ( मनीषितानि) इच्छित वस्तुएँ (वितरति) देती हैं (पुनः) फिर ( त्वयि ) आपके विषय में की गई (नुतिविषया) स्तुति विषयक भक्ति (विशेषात् ) विशेष रूप से (सुखानि) सुख (यश:) कीर्ति ( धनं) धन-सम्पत्ति (च) और (जयम्) जीत को (दिशति) देती है ।
टीका - भो जिन ! यथा कथञ्चित् । विहिता निर्मिता । भक्तिर्विनताय नम्रीभूताय । मनीषितानि मनोऽभिलषितानि । वितरति ददाति । पुनस्त्वयि विषये नुतिविषया स्तुतिविषयिणी भक्तिस्त्वद्गोचरीभूता या भक्तिः । विशेषात् सुखानि च पुनर्यशश्च पुनर्धनं च पुनर्जयं च दिशति ददाति ।
भावार्थ- हे भगवन्! आपकी भक्ति से सुख, यश, धन तथा विजय आदि की प्राप्ति होती है ।
. . .
Source: पंचस्तोत्र संग्रह