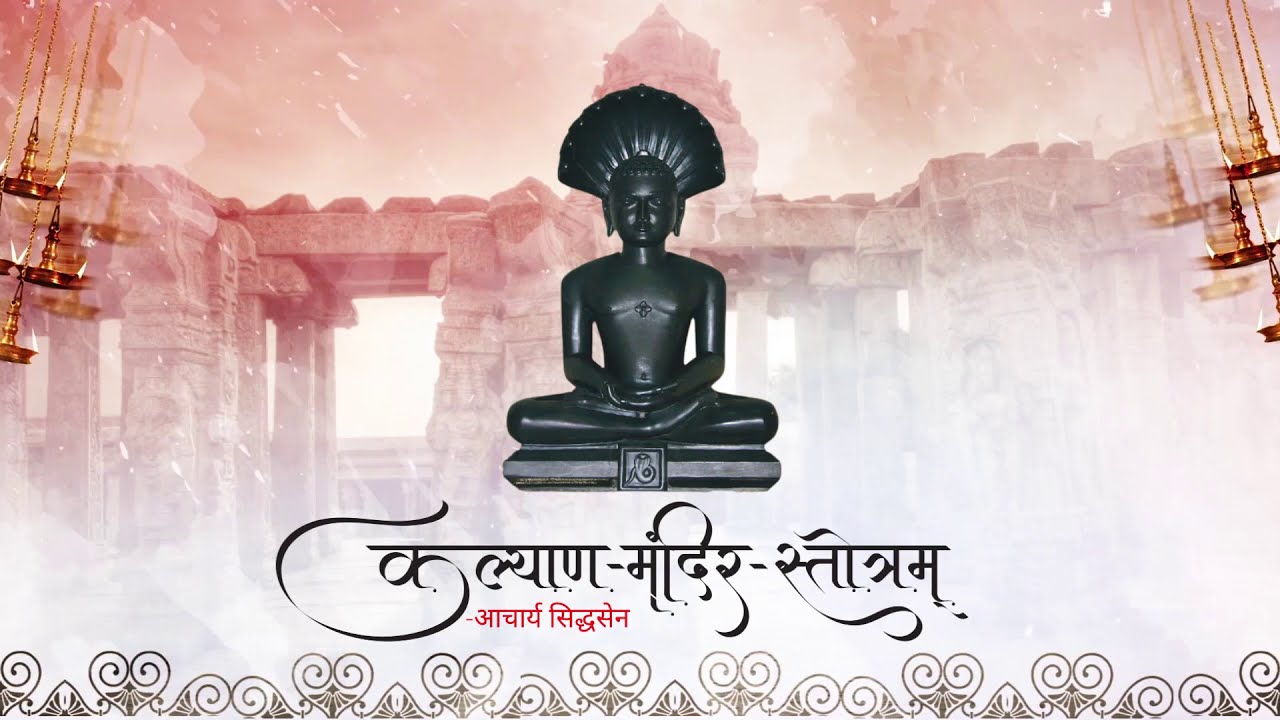तार्किकचक्रचूड़ामणि श्री कुमुदचन्द्राचार्य
अपरनाम श्री सिद्धसेनदिवाकरविरचित
कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्
(वसन्ततिलका छन्द)
(मंगलाचरण)
कल्याण- मन्दिरमुदारमवद्य-भेदि
भीताभय-प्रदमनिन्दितमङ्घ्रि- पद्मम् ।
संसार-सागर-निमज्जदशेषु-जन्तु -
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥१ ॥
यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः
स्तोत्रं सुविस्तृत-मतिर्न विभुर्विधातुम् ।
तीर्थेश्वरस्य कमठ-स्मय- धूमकेतो-
स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करष्येि ॥ २ ॥
(युग्मम्)
अन्वयार्थ – (कल्याणमंदिरम्) कल्याणों के मंदिर (उदारम्) दाता या महान् (अवद्यभेदि) पापों को नष्ट करने वाले (भीताभयप्रदम्) संसार से डरे हुए जीवों को अभयपद देने वाले (अनिन्दितं) प्रशंसनीय (संसार-सागर-निमज्ज-दशेषजन्तुपोतायमानम् ) संसाररूपी समुद्र में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए जहाज के समान (जिनेश्वरस्य) जिनेन्द्र भगवान् के (अङ्घ्रिपद्मम्) चरण-कमलों को (अभिनम्य) नमस्कार करके (गरिमाम्बुराशेः) गौरव के समुद्र- स्वरूप (यस्य) जिन पार्श्वनाथ की (स्तोत्रम् विधातुम्) स्तुति करने के लिए (स्वयं सुविस्तृतमतिः) स्वयं विशाल बुद्धि वाले (सुरगुरुः) बृहस्पति भी (विभुः) समर्थ (न ‘अस्ति’) नहीं है (कमठ - स्मयधूमकेतोः) कमठ का मान भस्म करने के लिए अग्निस्वरूप ( तस्य तीर्थेश्वरस्य) उन पार्श्वनाथ भगवान् की (किल) आश्चर्य है कि (एष: अहं) यह मैं (संस्तवनम् करिष्ये) स्तुति करूँगा।
टीका - किलेति सम्भाव्यते । एषोऽहं कविस्तस्य जगत्प्रसिद्धस्य । जिनेश्वरस्य श्रीपार्श्वनाथतीर्थङ्करपरमदेवस्य । अङ्घ्रिपद्मं चरणकमलं । अभिनम्य प्रणिपत्य। संस्तवनं सम्यक् स्तोत्रं । करिष्ये करिष्यामीत्यर्थः । कथम्भूतमङ्घ्रिपद्मं ? कल्याणानां माङ्गल्यराशीनां मन्दिरं निकेतनमित्यर्थः । अथवा पञ्चकल्याणानां स्थानमित्यर्थः । पुनः कथंभूतं ? उदारं नाना सौख्यं प्रदातृत्वात् । पुनः कथंभूतं अवद्यं पापं भेदयतीति । पुनः कथंभूतं ? भीतानां भयत्रस्तानां जन्तूनां अभयं जीवदानं प्रकर्षेण ददातीति । पुनः कथंभूतं ? अनिंदितं प्रशस्यं सर्वामरपूजितत्वात् । पुनः कथंभूतं? संसारश्चतुर्गति-लक्षणः स एव संसार - समुद्रस्तत्र निमज्जंतश्च ते अशेषजन्तवः सर्वप्राणिनश्च तेषां पोतयते तत् पोतायमानं संसारसमुद्रतारणे प्रवहण - तुल्यमित्यर्थः । तस्य कस्य? यस्य तीर्थेश्वरस्य समस्ततीर्थानां स्वामिनः। सुरगुरुर्बृहस्पतिः स्वयं स्तोत्रं विधातुं कर्तुं न विभुः न समर्थः । कथंभूतस्य यस्य गुरोर्भावः गरिमा तस्य अम्बुराशिः समुद्रस्तस्य । कथंभूतः सुरगुरुः ? सुखेन वा सुतरां विस्तृता मतिर्यस्य सः। पुनः कथंभूतस्य तस्य कमठचर - शम्बरनाम - ज्योतिष्कदेवस्य स्मयः गर्वस्तद्वृलनाय धूमकेतुर्वह्निस्तस्य ॥ युग्मं ॥
भावार्थ- जिनेन्द्र ! भगवान् के चरण कमलों को नमस्कार कर मैं उन पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति करता हूँ, जो गुरुता के समुद्र थे और कमठ का मान मर्दन करने वाले थे तथा बृहस्पति भी जिनकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हो सका था।
लघुता अभिव्यक्ति
सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप-
मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा: ।
धृष्टोऽपि कौशिक - शिशुर्यदि वा दिवान्धो,
रूपं प्ररूपयति किं किल धर्म रश्मेः ? ॥३ ॥
अन्वयार्थ - (अधीश !) हे स्वामिन्! (सामान्यतः अपि) साधारण रीति से भी (तव) आपके (स्वरूपं) स्वरूप को (वर्णयितुं ) वर्णन करने
लिए (अस्मादृशाः मुझ जैसे मनुष्य (कथम्) कैसे (अधीशा) समर्थ (भवन्ति) हो सकते हैं? अर्थात् नहीं हो सकते हैं (यदि वा) अथवा ( दिवान्धः) दिन में अन्धा रहने वाला ( कौशिकशिशुः) उल्लू का बच्चा (धृष्टः अपि 'सन् ') धीठ होता हुआ भी (किम् ) क्या (घर्मरश्मेः) सूर्य के (रूपम्) रूप की (प्ररूपयति किल) वर्णन कर सकता है? अर्थात् नहीं कर सकता।
टीका - भो अधीश ! अस्मादृशाः पुमान्सः । सामान्यतोऽपि सामान्या- कारेणाऽपि । तव भगवतः । स्वरूपं वर्णयितुं यथावदाख्यातुं । कथमधीशाः समर्था भवन्ति । विशेषतः स्वरूपं वक्तुं कुतः समर्थाः । यदि वा युक्तोऽयमर्थः । किलेति सत्यं धृष्टोऽपि कौशिकशिशुः घूकः । दिवान्धः सन्। घर्मरश्मेः सूर्यस्य स्वरूपं । किं प्ररूपयति ? अस्मादृशाः कवयस्तव निरञ्जनस्वरूपं वक्तु क्षमा न भवन्ति । क इव घूक इव । यथा घूको दिनपतेः सूर्यस्य किरणानि न प्ररूपयति । इति तात्पर्यार्थः ।
भावार्थ - हे प्रभो ! जिस तरह उल्लू का बालक सूर्य के रूप का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक सूर्य रहता है तब तक वह अन्धा रहता है, इसी तरह मैं आपके सामान्य स्वरूप का भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मिथ्याज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धा होकर आपके दर्शन से वञ्चित रहा हूँ।
अनिर्वचनीय गुणमहिमा
मोह - क्षयादनुभवन्नपि नाथ! मर्त्यो,
नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत ।
कल्पान्त-वान्त-पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्,
मीयेत के जलधेनु रत्नराशिः ॥४॥
अन्वयार्थ - ( नाथ ! ) हे नाथ! ( मर्त्यः) मनुष्य (मोहक्षयात्) मोहनीयकर्म के क्षय से (अनुभवन् अपि) अनुभव करता हुआ भी (तव) आपके (गुणान् गुणों को (गणयितुम् ) गिनने के लिए (नूनम् ) निश्चय करके ( न क्षमेत) समर्थ नहीं हो सकता ( यस्मात् ) क्योंकि ( कल्पान्त- वान्तपयसः) प्रलयकाल के समय जिसका पानी बाहर हो गया है ऐसे (जलधेः) समुद्र की (प्रकट: अपि ) प्रकट हुई भी ( रत्नराशिः) रत्नों की राशि (ननु केन मीयेत ) किसके द्वारा गिनी जा सकती है? अर्थात् किसी के द्वारा नहीं ।
टीका - भो नाथ ! भोः स्वामिन ! नूनं निश्चितं ! मर्त्यो मनुष्य मोहक्षयात् मोहनीयकर्मविनाशात्। अनुभवन्नपि जानन्नपि । तव परमेश्वरस्य गुणान् । गणयितु संख्याकर्तुं । न क्षमेत न समर्थो भवेत् । ननु युक्तोऽयमर्थो यस्मात्कारणात्केन पुन्सा । जलधेः समुद्रस्य प्रकटोऽपि रत्नराशिः । मीयते मानं कुर्वीत । कथंभूतस्य जलधेः ? कल्पान्तः प्रलयस्तेन वान्तानि बहिष्कृतानि पयान्सि जलानि यस्य स तस्य ।
भावार्थ– हे प्रभो! जिसतरह प्रलयकाल में पानी न होने से साफ साफ दिखने वाले समुद्र के रत्नों को कोई नहीं गिन पाता उसी तरह मिथ्यात्व के अभाव से साफ साफ दिखने वाले आपके गुणों को कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि वे अनन्तानन्त हैं ।
अल्पज्ञता प्रदर्शन
अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ ! जडा-शयोऽपि,
कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य ।
बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य,
विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ॥५॥
अन्वयार्थ - (नाथ) हे नाथ! (‘अहम्’ जडाशय: अपि ) मैं मूर्ख भी (लस-दसंख्यगुणाकरस्य) सुशोभित असंख्यात गुणों की खानि स्वरूप (तव) आपके (स्तवम् कर्तुम्) स्तवन करने के लिए (अभ्युद्यतः अस्मि) तैयार हुआ हूँ, क्योंकि (बाल: अपि) बालक भी (स्वधिया) अपनी बुद्धि के अनुसार (निजबाहुयुगम् ) अपने दोनों हाथों को (वितत्य) फैलाकर (किम् ) क्या (अम्बुराशेः) समुद्र के ( विस्तीर्णताम् ) विस्तार को (न कथयति) नहीं कहता ? अर्थात् कहता है ।
टीका - भो नाथ! जडाशयोऽपि अहं । तव परमेश्वरस्य । स्तवं कर्तुमभ्युद्यतोस्मि उद्यमितोऽस्मि । कथंभूतस्य तव ? लसन्तः शोभमानाः असंख्या ये गुणास्तेषामाकरस्तस्य । बालोऽपि स्वधिया बालस्वबुद्ध्या । निज बाहुयुगं वितत्य विस्तार्य । अम्बुराशेः समुद्रस्य । विस्तीर्णतां किं न कथयति न प्ररूपयति? अपि तु प्ररूपयतीति तात्पर्यार्थः ।
भावार्थ - हे नाथ! जैसे बालक शक्ति न रहते हुए भी समुद्र का विस्तार वर्णन करने के लिए तैयार रहता है वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ।
अविचारित कार्य
ये योगिनामपि न यान्ति, गुणास्तवेश!,
वक्तुं कथं भवति तेषु ममाव - काश: ? ।
यापीठ जाता तदेव-मसमीक्षित कारितेयं,
जल्पन्ति वा निज-गिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥६॥
अन्वयार्थ - ( ईश ! ) हे भगवन्! (तव) आपके (ये गुणाः) जो गुण (योगिनाम् अपि) योगियों को भी ( वक्तुम्) कहने के लिए (न यान्ति) नहीं प्राप्त होते अर्थात् जिनका कथन योगीजन भी नहीं कर सकते (तेषु) उनमें (मम) मेरा (अवकाशः) अवकाश (कथम् भवति) कैसे हो सकता है? अर्थात् मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ? (तत्) इसलिए ( एवम् इयम्) इस प्रकार मेरा यह (असमीक्षितकारिता जाता ) बिना विचारे काम करता हुआ (वा) अथवा (पक्षिणः अपि) पक्षी भी (निजगिरा ) अपनी वाणी से ( जल्पन्ति ननु) बोला करते हैं।
टीका - हे ईश ! ये तव गुणा योगिनामपि वक्तुं न यान्ति न प्राप्नुवन्ति । तेषु गुणेषु ममावकाशः मम सामर्थ्यं कथं भवति । भो देव तत्तस्मात्कारणात्। एवमियमसमीक्षितकारिता जाता। अविचारितकार्यत्वं जातं । असमीक्षितस्य अविचारितस्य कारिता असमीक्षितकारिता । वा अथवा । ननु निश्चितं । पक्षिणोऽपि निजगिरा स्वकीयवाण्या जल्पन्ति भणन्ति । तथैवाहमपीति भावः ।
भावार्थ- हे प्रभो! आपका स्तवन प्रारम्भ करने के पहले मैंने इस बात का विचार नहीं किया कि आपके जिन गुणों का वर्णन बड़े-बड़े योगी भी नहीं कर सकते हैं उनका वर्णन मैं कैसे करूँगा? इसलिए हमारी यह प्रवृत्ति बिना विचारे हुई है।
प्रभु नाम
आस्ता - मचिन्त्य - महिमा जिन !
संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति ।
तीव्रातपोपहत -पान्थजनान् निदाघे-
प्रीणातिपद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥
अन्वयार्थ - ( जिन !) हे जिनेन्द्र ! (अचिन्त्यमहिमा) अचिन्त्य है महिमा जिसकी, ऐसा (ते) आपका (संस्तवः ) स्तवन (आस्ताम् ) दूर रहे, (भवतः) आपका (नाम अपि) नाम भी ( जगन्ति ) जीवों को (भवतः ) संसार से ( पाति) बचा लेता है, क्योंकि ( निदाघे) ग्रीष्मकाल में (तीव्रातपोपहत-पान्थजनान्) तीव्र घाम से सताये हुए पथिकजनों को (पद्मसरसः) कमलों के सरोवर का ( सरसः) शीतल (अनिलः अपि) पवन भी (प्रीणाति) संतुष्ट करता है ।
टीका - भो जिन! ते तव । संस्तवः स्तवनं । आस्तां दूरे तिष्ठतु । कथंभूतः संस्तवः ? अचिन्त्यमहिमा अनिर्वचनीयमहिमा यस्य स इति अचिन्त्यमहिमा । भवतस्तव नामाऽपि अभिधानमपि। भवतः संसारात् । जगति पाति रक्षति । निदाघे ग्रीष्मे । पद्मसरसः पद्ममण्डिततडागरस्य सरसः रसेन जलच्छटाभिः सह वर्तमानः । अनिलोऽपि वायुस्तीव्रः दुस्सहः स चासावातपस्तेन उपहता उपद्रुताश्च ते पान्था जनाश्च पथिकास्तान् प्रीणाति तर्पयति ।
भावार्थ - हे देव ! आपके स्तवन की तो अचिन्त्य महिमा है ही, पर आपका नाम मात्र भी जीवों को संसार के दुःखों से बचा लेता है। जैसे ग्रीष्मऋतु में घाम से पीड़ित मनुष्यों को कमलयुक्त सरोवर तो सुख पहुँचा ही हैं, पर उन सरोवरों की शीतल हवा भी सुख पहुँचाती है।
जिन भक्ति से कर्मनाश
हृद्-वर्तिनि त्वयि विभो ! शिथिली - भवन्ति,
जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धाः |
सद्यो भुजङ्गम-मया इव मध्यभाग,
मभ्यागते वन- शिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥
अन्वयार्थ - ( विभो ! ) हे स्वामिन्! ( त्वयि ) आपके (हृद्वर्तिनि ‘सति’) हृदय में मौजूद रहते हुए (जन्तोः) जीवों के (निबिडाः कर्मबन्धाः अपि) सघन कर्मों के बन्धन भी ( क्षणेन) क्षणभर में (वनशिखण्डिनि अभ्यागते) वन मयूर के आने पर (चन्दनस्य मध्यभागम् ‘सति’) चन्दनवृक्ष के मध्यभाग में (भुजङ्गम-मयाः इव) सर्पों के बंधनरूप कुण्डलियों के समान (सद्यः) शीघ्र ही (शिथिलीभवन्ति ) ढीले पड़ जाते हैं।
टीका - हे विभो ! त्वयि भगवति द्वर्तिनि सति चित्ते वर्तयति सति । जन्तोः प्राणिनः । निबिडा अपि कर्मबन्धाः क्षणेन क्षणमात्रेण । शिथिलीभवन्ति । हृदि वर्तत इत्येवंशीलः हृद्वर्ती तस्मिन् । कर्मणां बन्धाः कर्मबन्धाः अशिथिलाः शिथिला भवन्तीति शिथिलीभवन्ति । के इव? भुजङ्गममया बन्धा इव । यथा वनशिखण्डिनि वनमयूरे । चन्दनस्य मध्य-भागमभ्यागते सति भुजङ्गममया बन्धा इव सद्यः तत्कालं शिथिलीभवन्ति । भुजङ्गमप्रकारा भुजङ्गममयाः प्रकारे मयट् ।
भावार्थ - हे भगवन् ! जिस तरह मयूर के आते ही चन्दन वृक्ष लिपटे हुए साँप ढीले पड़ जाते हैं उसी तरह जीवों के हृदय में आपके आने पर उनके कर्मबन्धन ढीले पड़ जाते हैं।
प्रभु दर्शन की महिमा
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र !
रौद्रैरुपद्रव - शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।
गो-स्वामिनि स्फुरित - तेजसि दृष्टमात्रे:,
चारै-रिवा पशवः प्रपलायमानैः॥९॥
अन्वयार्थ - ( जिनेन्द्र ! ) हे जिनेन्द्र ! ( स्फुरिततेजसि ) पराक्रमी (गोस्वामिनि दृष्टमात्रे) राजा के दिखते ही (आशु) शीघ्र ही (प्रपलाय- मानैः) भागते हुए (चौरैः) चोरों के द्वारा (पशवः इव) पशुओं की तरह (त्वयि वीक्षिते अपि) आपके दिखते ही / आपके दर्शन करते ही (मनुजाः) मनुष्य (रौद्रैः) भयङ्कर (उपद्रवशतैः) सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा (सहसा एव) शीघ्र ही (मुच्यन्ते) छोड़ दिये जाते हैं ।
टीका - भो जिनेन्द्र ! त्वयि भगवति वीक्षिते सति । रौद्रैरपि उपद्रवशतैः उपसर्गकोटिभिः। मनुजाः सहसा मुच्यन्त एव विमुक्ता एव। कैरिव? चौरेरिव । यथाः चौरैः गोस्वामिनि नृपे दृष्टमात्रे सति । आशु शीघ्रं । पशवः मुच्यते । कथंभूते गोस्वामिनि ? स्फुरितुं प्रतापाक्रान्तं तेजो यस्य स तस्मिन् । कथंभूतैश्चौरैः । प्रकर्षेण पलायमानाः प्रपलायमानास्तैः शीघ्रं नश्यद्भिः ।
भावार्थ - हे नाथ! जिस तरह तेजस्वी मालिक के दिखते ही चोर चुराई हुई गायों को छोड़कर शीघ्र ही भाग जाते हैं उसीतरह आपके दर्शन होते ही अनेक भयंकर उपद्रव मनुष्यों को छोड़कर भाग जाते हैं।
भवसिन्धु तारक जिन
त्वं तारको जिन! कथं भविनां त एव,
त्वामुद् वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः ।
यद्वा दृतिस्तरति यज्जल - मेष नून-,
मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥१०॥
अन्वयार्थ - (जिन) हे जिनेन्द्रदेव! (त्वम्) आप (भविनाम्) संसारी जीवों के (तारकः कथम्) तारने वाले कैसे हो सकते हैं? (यत्) क्योंकि ( उत्तरन्तः ) संसार - समुद्र से पार होते हुए (ते एव) वे संसारी जीव ही (हृदयेन) हृदय से (त्वाम् ) आपको (उद्वहन्ति) तिरा ले जाते हैं । (यद्वा) अथवा ठीक ही है (दृतिः) मसक (यत्) जो (जलम् तरति ) जल में तैरती है ( स एषः) वह यह ( नूनम् ) निश्चय से ( अन्तर्गतस्य) भीतर स्थित (मरुतः) हवा का (किल अनुभावः) निश्चित ही प्रभाव है।
टीका - यत् यस्मात्कारणात् । त एव प्राणिनः भवाब्धे उत्तरन्तः सन्तो हृदयेन त्वां उद्वहन्ति तारयन्ति । अहमेवं सम्भावयामि भवः संसारः विद्यते येषां ते भविनस्तेषां भविनां । यद्वा युक्तोऽयमर्थः । यत् यस्मात्कारणात् दृतिश्चर्म भस्त्रिका जलं तरति । नूनं निश्चितं । किलेति सत्ये । एष अन्तर्गतस्य मरुतः पूरितस्य वायोरनुभावः प्रभावः ।
भावार्थ - हे प्रभो ! जिस तरह भीतर भरी हुई वायु के प्रभाव से मसक पानी में तैरती है उसी तरह आपको हृदय में धारण करने वाले (मन से आपका चिन्तन करने वाले) पुरुष आपके ही प्रभाव से संसार-समुद्र से तिरते हैं।
मदन विजेता पार्श्वनाथ
यस्मिन् हर - प्रभृतयोऽपि हत - प्रभावाः,
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन ।
विध्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन, अनविद्यापीठ
पीतं न किं तदपि दुर्धर - वाडवेन ॥ ११॥
अन्वयार्थ - ( यस्मिन्) जिसके विषय में (हरप्रभृतयः अपि) विष्णु- महादेव आदि भी (हतप्रभावाः ‘जाता:’) प्रभाव रहित हो गए हैं (सः) वह (रतिपतिः अपि) कामदेव भी (त्वया) आपके द्वारा (क्षणेन) क्षणमात्र में (क्षपितः) नष्ट कर दिया गया (अथ) अथवा ठीक है कि (येन पयसा ) जिस जल के द्वारा ( हुतभुजः विध्यापिताः) अग्नि बुझायी जाती है (तत् अपि) वह जल भी (दुर्द्धरवाडवेन) प्रचण्ड बड़वानल से (किम्) क्या (न पीतम्) नहीं पिया गया? अर्थात् पिया गया।
टीका- भो पार्श्वनाथ! यस्मिन् कामे हरिप्रभृतयोऽपि ब्रह्माविष्णु- महेशादयो हतप्रभावा निरस्तशक्तयो जाताः सोऽपि रतिपतिः कामस्त्वया क्षणेन क्षणमात्रेण क्षपितो ध्वस्तः । अथ युक्तोऽयमर्थः । येन पयसा हुतभुजोऽग्नयो विध्यापिता निरस्तास्तदपि जलं दुर्द्धरवाडवेन दुःसहवाड - वाग्निना किं न पीतं ? अपि तु शोषितमित्यर्थः ।
भावार्थ- जिस काम ने हरि-हर-ब्रह्मा आदि महापुरुषों को पराजित कर दिया था उस काम को भी आपने पराजित कर दिया यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जो जल संसार की समस्त अग्नि को नष्ट करता है उस जल को भी बड़वानल नामक समुद्र की अग्नि नष्ट कर डालती है ।
महापुरुषों का अचिन्त्य प्रभाव
स्वामिन्! - ननल्प - गरिमाणमपि प्रपन्नाः,
त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः ।
जन्मोदधिं लघु तरन्त्यति - लाघवेन,
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः॥१२॥
अन्वयार्थ - ( स्वामिन्!) हे प्रभो ! (अहो ) आश्चर्य है कि (अनल्प- गरिमाणम् अपि) अधिक गौरव से युक्त भी विरोध पक्ष में- अत्यन्त वजनदार (त्वाम्) आपको (प्रपन्नाः) प्राप्त हो (हृदये दधानाः) हृदय में धारण करने वाले (जन्तवः) प्राणी (जन्मोदधिम् ) संसार - समुद्र को (अतिलाघवेन ) बहुत ही लघुता से ( कथम्) कैसे (लघु तरन्ति) शीघ्र तर जाते हैं (यदि वा) अथवा (हन्त) हर्ष है कि (महताम्) महापुरुषों का (प्रभाव:) प्रभाव (चिन्त्यः) चिन्तन के योग्य ( न भवति) नहीं होता है ।
टीका - भो स्वामिन्! अतुल्यगरिमाणमपि मानरहितगुरुत्वभारा- क्रान्तमपि । त्वां प्रपन्नाः प्राप्ता जन्तवः अहो इत्याश्चर्ये । हृदये दधानाः सन्तः । लघु यथा स्यात्तथा । जन्मोदधिं भवार्णवं । अतिलाघवेन शीघ्रेण । कथं तरन्ति ? अन्यत् गुरुत्वाक्रान्तवस्तु हृदये दधानाः सन्तः प्राणिनोऽब्धौनिमज्जन्ति । त्वां गुरुत्वाक्रान्तं हृदये दधानाः सन्तः भवार्णवे तरन्ति तन्मम मनसि महच्चित्रं । यदि वा पक्षान्तरे हन्त इत्यहो महतां महानुभावानां परमपुरुषाणां प्रभावो लोकोत्तरो महिमा न चिन्त्यः नो विचारणीय इत्यर्थः ।
भावार्थ - श्लोक में आये हुए ‘अनल्पगरिमाणम्’ पद के 'अधिक वजनदार’और ‘“ अत्यन्त गौरव से युक्त श्रेष्ठ" इस तरह दो अर्थ होते हैं । उनमें से आचार्य ने प्रथम अर्थ को लेकर उस विरोध को बतलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया है और दूसरे अर्थ को लेकर उस विरोध का परिहार किया है।
क्रोध के अभाव का प्रभाव
क्रोधस्त्वया यदि विभो ! प्रथमं निरस्तो,
ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौराः ।
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके,
नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥ १३ ॥
अन्वयार्थ - (विभो ) हे प्रभो ! (यदि) यदि (त्वया) आपके द्वारा (क्रोध) क्रोध (प्रथमम् ) पहले ही (निरस्तः) नष्ट कर दिया गया था, (तदा) तो फिर (वद) कहिए कि आपने ( कर्मचौरा:) कर्मरूपी चोर (कथम्) कैसे (ध्वस्ताः किल ) नष्ट किए? (यदि वा ) अथवा (अमुत्र लोके) इसलोक में (हिमानी) बर्फ - तुषार (शिशिरापि) ठण्डा होने पर भी (किम्) क्या (नीलद्रुमाणि) हरे-हरे हैं वृक्ष जिनमें ऐसे (विपिनानि) वनों को (न प्लोषति) नहीं जला देता है? अर्थात् जला देता है / मुरझा देता है।
टीका - भो विभो ! भो त्रिजगन्नाथ ! यदि चेत्त्वया भगवता । क्रोधः प्रथमं निरस्तो निराकृतः । तदा तर्हि । वतेति विस्मयावहम् । किलेति सत्ये । कर्मचौरा अष्टकर्मदस्यवः । कथं ध्वस्ताः निर्मूलिताः । कर्माण्येव चौराः कर्मचौराः । यदि वा युक्तोऽयमर्थः । अमुत्र लोके । शिशरापि शीतलापि । हिमानी हिमसंहतिः । नीलद्रुमाणि विपिनानि किं न प्लोषति न दहति ? अपि तु प्लोषत्येव। नीला हरितो द्रुमा वृक्षा येषु तानि । प्लुष दाहे इत्यस्य धातोः प्रयोगः ।
भावार्थ- लोक में ऐसा देखा जाता है कि क्रोधी मनुष्य ही शत्रुओं को जीतते हैं, पर भगवन् आपने क्रोध को तो नवमें गुणस्थान में ही जीत लिया था। फिर क्रोध के अभाव में चौदहवें गुणस्थान तक कर्मरूपी शत्रुओं को कैसे जीता? आचार्य ने इस लोकविरुद्ध बात पर पहले आश्चर्य प्रकट किया, पर जब बाद में उन्हें ख्याल आता है कि ठण्डा तुषार बड़े- बड़े वनों को क्षणभर में जला देता है अर्थात् क्षमा से भी शत्रु जीते जा सकते हैं, तब वे अपने आश्चर्य का स्वयं समाधान कर लेते हैं।
आत्मा की खोज
त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूप,
मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोशदेशे ॥
पूतस्य निर्मल-रुचेर्यदि वा किमन्य,
दक्षस्य सम्भव - पदं ननु कर्णिकायाः ॥१४॥
अन्वयार्थ - (जिन !) हे जिन ! (योगिनः) ध्यान करने वाले मुनीश्वर (सदा) हमेशा (परमात्मरूपम्) परमात्मास्वरूप ( त्वाम् ) आपको (हृदयाम्बुज - कोशदेशे) अपने हृदयरूप कमल के मध्यभाग में (अन्वेष- यन्ति) खोजते हैं (यदि वा) अथवा ठीक है कि ( पूतस्य निर्मलरुचेः) पवित्र और निर्मल कान्ति वाले (अक्षस्य) कमल के बीज का अथवा शुद्धात्मा का (सम्भवपदम् ) उत्पत्ति स्थान अथवा खोज करने का स्थान (कर्णिकायाः अन्यत्) कमल की कर्णिका / डण्ठल को छोड़कर अथवा हृदय - कमल की कर्णिका को छोड़कर (अन्यत् किम् ननु) दूसरा क्या हो जैन विद्यापीठ सकता है?
टीका— भो जिन! योगिनः सर्वदा सर्वकाले | हृदयाम्बुजकोशदेशे निजमनोऽम्बुजकोटरे । त्वां परमात्मरूपं चिदानन्दरूपं। अन्वेषयन्ति गवेषयन्ति । परं सर्वोत्कृष्टं मं ज्ञानं यस्य स चासावात्मा स एव रूपं स्वरूपं यस्य स तं। हृदयमेवाम्बुजं कमलं हृदयाम्बुजं तस्य कोशदेश- स्तस्मिन् । यदि वा युक्तोऽसमर्थः ननु निश्चितं कर्णिकायाः सकाशात् अन्यत् पूतस्य निर्मलस्य अक्षस्य कमलबीजस्य । यत् स्थानं किं सम्भवि सम्भवति ? अपि तु न सम्भवति । कथंभूतस्य अक्षस्य ? निर्मला रुचिर्यस्य स तस्य ।
भावार्थ- बड़े बड़े योगीश्वर ध्यान करते समय अपने हृदय कमल में आपको खोजते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जैसे कमल बीज की उत्पत्ति कमल कर्णिका में ही होती है उसी तरह शुद्धात्म स्वरूप आपका सद्भाव भी हृदय कमल की कर्णिका में ही होगा । श्लोक में आये हुए अक्ष शब्द के ‘कमलबीज कमलगटा’ और आत्मा (अक्ष्णोति -जानातीत्यक्षः = आत्मा) इस तरह दो अर्थ होते हैं ।
परमात्म ध्यान का लाभ
ध्यानाज्जिनेश! भवतो भविनः क्षणेन,
देहं विहाय परमात्म- दशां व्रजन्ति ॥
तीव्रानलादुपल - भावमपास्य लोके,
चामीकरत्वमचिरादिव धातु - भेदाः ॥१५॥
अन्वयार्थ - (जिनेश ! ) हे जिनेश ! (लोके) लोक में (इव) जैसे (तीव्रानलात्) तीव्र अग्नि के सम्बन्ध से (धातुभेदा: ) अनेक धातुएँ (उपलभावम्) पत्थररूप पूर्वपर्याय को (अपास्य) छोड़कर (अचिरात्) शीघ्र ही (चामीकरत्वम्) सुवर्ण पर्याय को (व्रजन्ति) प्राप्त होती हैं उसी तरह (भविनः) संसार के प्राणी (भवतः ) आपके (ध्यानात्) ध्यान से ( देहम् ) शरीर को (विहाय) छोड़कर (क्षणेन) क्षणभर में (परमात्म- दशाम्) परमात्मा की अवस्था को (व्रजन्ति) प्राप्त होते हैं |
टीका - भो जिनेश ! भविनः प्राणिनः । भवतो ध्यानात् । क्षणेन क्षण- जैन विद्यापीठ मात्रेण । देहं शरीरं । विहाय समुत्सृज्य । परमात्मदशां परमात्मावस्थां व्रजन्ति प्राप्नुवन्ति । परमात्मनो दशा ताम् । क इव ? धातुभेदा इव । यथा धातुभेदाः सुवर्णोपलाः लोके संसारे । तीव्रानलात् अत्यन्तदुःसहाग्नेः सकाशात्। उपलभावं उपलत्वं । अपास्य विहाय । अचिरात् अचिरकालेन । चामीकरत्वं सुवर्णभावं गच्छन्ति। तीव्रश्चासौ अनलश्च तीव्रनलस्तस्मात्। चामीकरस्य भावः चामीकरत्वम्।
भावार्थ- जो जीव आपका ध्यान करते हैं वे थोड़े ही समय में शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं ।
ध्यान से बन्धन मुक्ति
अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वम्,
भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ? ।
एतत्स्वरूपमथ मध्य-विवर्तिनो हि,
यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ १६॥
अन्वयार्थ - ( जिन !) हे जिनेन्द्र ! (भव्यैः) भव्यजीवों के द्वारा (यस्य) जिस शरीर के (अन्तः) भीतर (त्वम् ) आप (सदैव) हमेशा (विभाव्यसे) ध्याये जाते हैं (तत्) उस (शरीरम् अपि) शरीर को ही आप (कथम्) क्यों (नाशयसे) नष्ट करा देते हैं? (अथ) अथवा ( एतत् स्वरूपम्) यह स्वभाव ही है (यत्) कि (मध्यविवर्तिनः) मध्यस्थ-बीच में रहने वाले और राग-द्वेष से रहित (महानुभावा:) महापुरुष (विग्रहम्) विग्रह शरीर और द्वेष को ( प्रशमयन्ति ) शान्त करते हैं ।
टीका - हे जिन ! यस्य शरीरस्यान्तर्मध्ये । सदैव सर्वदा काले । भव्यैः प्राणिभिस्त्वं । विभाव्यसे स्मर्यसे । तदपि शरीरं कथं नाशयसे अथ पक्षे । हि युक्तोऽयमर्थः । हि यस्मात्कारणात् । मध्यविवर्तिनां प्राणिनां एतत् स्वरूपं एतत् किं? यत् मध्यविवर्तिनो महानुभावाः विग्रहं कलहं पक्षे शरीरं । प्रशमयंति उपशमयंति। मध्ये विवर्तन्त इत्येवंशीलाः मध्यविवर्तिनः। महान् अनुभावः महिमा येषां ते महानुभावाः ।
भावार्थ- लोक में रीति प्रचलित है कि जो जहाँ रहता है अथवा जहाँ जिसका ध्यान सम्मान आदि किया जाता है वह उस जगह का विनाश नहीं करता । पर भगवन्! आप भव्य जीवों के जिस शरीर में हमेशा सन्मान पूर्वक ध्याये जाते हैं आप उन्हें उसी तरह विग्रह (शरीर) को नष्ट करने का उपदेश देते हैं । आचार्य को पहले इस लोकविरुद्ध बात पर भारी आश्चर्य होता है पर जब उनकी दृष्टि विग्रह शब्द के द्वेष अर्थ पर जाती है तब उनका आश्चर्य दूर हो जाता है । श्लोक में आये हुए विग्रह शब्द के दो अर्थ हैं एक ‘शरीर’ और दूसरा ‘द्वेष’ इसी तरह ’ मध्यविवर्तिनः ’ शब्द के भी दो अर्थ हैं एक "बीच में रहने वाला” और दूसरा "रागद्वेष से रहित समताभावी ” ।
परमात्म स्वरूप का अनुभव
आत्मा मनीषिभि-रयं त्वदभेद-बुद्धया
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रभावः ।
पानीय-मप्यमृत-मित्यनुचिन्त्यमानं,
किन्नाम नो विष-विकार - मपाकरोति ॥१७॥
अन्वयार्थ - (जिनेन्द्र !) हे जिनेन्द्र ! ( मनीषिभिः) बुद्धिमानों के द्वारा (त्वदभेद-बुद्ध्या ) " आपसे अभिन्न है" ऐसी बुद्धि से (ध्यातः) ध्यान किया गया (अयम् आत्मा) यह आत्मा (भवत्प्रभावः) आप ही के समान प्रभाव वाला (भवति) हो जाता है (अमृतम् इति अनुचिन्त्यमानम्) यह अमृत है, इस तरह निरन्तर चिन्तन किया जाने वाला (पानीयम् अपि) पानी भी (किम्) क्या (विषविकारम्) विष के विकार को (नो अपाकरोति नाम) दूर नहीं करता? अर्थात् करता है ?
टीका - भो जिनेन्द्र ! मनीषिभिः पुंभिः अयं प्रमाणसिद्धः । आत्मा त्वदभेदबुद्ध्या त्वत्तः सकाशादभिन्नधिया । ध्यातः सन् इह लोके भवत्प्रभावो भवति। यादृशो भवत्प्रभावस्तादृशेन प्रभावेन युक्तो भवति । त्वत्सदृशो भवतीत्यर्थः। मनीषा बुद्धिर्विद्यते येषां ते तैः । त्वत्तः अभेदः ऐक्यं तस्य बुद्धिस्तया भवद्वत् प्रभावो यस्य सः । पानीयमपि अमृतं पीयूष इत्यनुचिन्त्यमानं स्मर्यमाणं सत् नामेति निश्चितं । विषविकारं किन्नो अपाकरोति? किं नो दूरीकरोति? अपि तु करोतीत्यर्थः । विषस्य विकारो विषविकारस्तम्। जैन विद्यापीठ
भावार्थ- जो पुरुष अपने आपको आपसे अभिन्न अनुभव करता है अर्थात् जो सोचता है कि - " भगवन् ! जैसी विशुद्ध आत्मा आपकी है निश्चय नय से हमारी आत्मा भी वैसी ही आपके समान विशुद्ध है किन्तु वर्तमान में कर्मोदय से अशुद्ध हो रही है । यदि मैं भी आपके रास्ते पर चलने का प्रयत्न करूँ तो मेरी आत्मा भी शुद्ध हो जायेगी" | ऐसा सोचकर जो शुद्ध होने का प्रयत्न करता है वह आपके ही समान शुद्ध हो जाता है । जैसे कि यह अमृत है, इस प्रकार निरन्तर चिन्तन किया गया पानी मन्त्रादि के संयोग से अमृतरूप हो जाता है और विष के विकार को दूर करने लगता है।
सर्वमान्य वीतराग जिन
त्वामेव वीत तमसं परवादिनोऽपि,
नूनं विभो ! हरिहरादिधिया प्रपन्नाः ।
किं काच- कामलिभिरीश ! सितोऽपि शङ्खो,
नो गृह्यते विविध - वर्ण - विपर्ययेण ॥ १८ ॥
अन्वयार्थ - (विभो !) हे स्वामिन्! ( परवादिनः अपि) अन्य मतावलम्बी पुरुष भी (वीततमसम्) अज्ञान अन्धकार से रहित (त्वाम् एव) आपको ही (नूनम्) निश्चय से (हरिहरादिधिया) विष्णु, महादेवादि की कल्पना से (प्रपन्नाः) प्राप्त होते हैं/ पूजते हैं (किम्) क्या (ईश!) हे विभो ! (काचकामलिभिः) जिनकी आँख पर रंगदार चश्मा है अथवा जिन्हें पीलिया रोग हो गया है, ऐसे पुरुषों के द्वारा (शङ्खः सित: अपि) शंख सफेद होने पर भी (विविधवर्ण - विपर्ययेण ) अनेक प्रकार के विपरीत वर्णों से (नो गृह्यते) ग्रहण नहीं किया जाता है? अर्थात् किया जाता है।
टीका - भो विभो ! नूनं निश्चितं । परवादिनोऽपि नैयायिकादयः । त्वामेव परमेश्वरं । हरिहरादिधिया ब्रह्माविष्णुमहेशसुगतादिबुद्धया । प्रपन्नाः प्राप्ताः। ध्यायन्तीत्यर्थः। हरिनारायणो हर ईश्वर इत्यादीनां धीस्तया । कथंभूतं त्वां ? वीतं निराकृतं तमो येन स वीततमास्तं वीततमसं । परे च ते वादिनश्च पर वादिनः । भो ईश ! एतद्युक्तं काचकामलिभिः पुंभिः । सितोऽपि उज्ज्वलो ऽपि शंखः। विविधवर्णविपर्ययेण नानाविधरक्तपीतादिवर्णभ्रान्त्या । अन्यथारूपेण किं नो गृह्यते ? अपि तु गृह्यत एव । चक्षुषो भ्रान्तिकारी काचकामलरोगो विद्यते येषां ते तैः । विविधाश्च ते वर्णाश्च विविध-वर्णास्तेषां विपर्ययस्तेन ।
भावार्थ– हे भगवन्! जिस तरह पीले चश्मावाला अथवा पीलिया रोग वाला मनुष्य सफेद शंख को पीला समझकर ग्रहण करता है उसीतरह मिथ्यात्व के उदय से अन्य मतावलम्बी पुरुष आपको विष्णु, महेश्वर आदि मानकर पूजते हैं।
अशोक प्रातिहार्य
धर्मोपदेश - समये सविधानु —भावा-,
दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः ।
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि ।
किं वा विबोध - मुपयाति न जीवलोकः ॥१९॥
अन्वयार्थ – (धर्मोपदेशसमये) धर्मोपदेश के समय (ते) आपकी (सविधानु-भावात्) समीपता के प्रभाव से (जनः आस्ताम्) मनुष्य तो दूर रहे (तरु: अपि) वृक्ष भी (अशोक) अशोक / शोक रहित (भवति) हो जाता है। (वा) अथवा ( दिनपतौ अभ्युद्गते ‘सति’) सूर्य के उदय होने पर (समहीरुहः अपि जीवलोकः ) वृक्षों सहित समस्त जीवलोक (किम्) क्या (विबोधम्) विकास / विशेष ज्ञान को (न उपयाति) नहीं प्राप्त होते अर्थात् होते हैं।
टीका - भो परमेश्वर ! धर्मोपदेशसमये धर्मदेशनाकाले । तव परमेश्वरस्य। सविधानुभावात् सामीप्यप्रभावात् । जनोः लोकः । आस्तां तिष्ठतु । तरुरपि अशोको भवति शोकरहितो भवति । तत्र लोकोऽपि भवतीति किमाश्चर्यं इति भावः। धर्मस्य उपदेशस्तस्य समयः दिव्यध्वनिकालस्तस्मिन् । सविधस्य अनुभावः महिमा तस्मात् । वा युक्तोऽयमर्थः दिनपतौ सूर्ये । अभ्युद्गते सति समन्तादुदिते सति । समहीरुहोऽपि वृक्षसहितोऽपि । जीवलोकः प्राणिवर्गः । विबोधं ज्ञानं किं न उपयाति ? ति? जाग्रदवस्थां किं न गच्छति? अपि उपयातीत्यर्थः । महीरुहैः सह वर्तमानः समहीरुहः ।
भावार्थ - इस श्लोक में अशोक शब्द के दो अर्थ हैं एक अशोक वृक्ष और दूसरा शोक रहित । इसी तरह विबोध शब्द के भी दो अर्थ हैं एक विशेष ज्ञान और दूसरा हरा भरा तथा प्रफुल्लित होना । हे भगवन् ! जब आपके पास मे रहने वाला वृक्ष भी अशोक हो जाता है तब आपके पास रहने वाला मनुष्य अशोक अर्थात् शोक रहित हो जावे इसमें क्या आश्चर्य है? यह ‘अशोक वृक्ष’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य
चित्रं विभो ! कथमवाङ्मुख - वृन्तमेव ।
विष्वक् पतत्य- विरला सुर - पुष्प - वृष्टिः ॥
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश !
गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥२०॥
अन्वयार्थ - (विभो ! ) हे स्वामिन्! (चित्रम्) आश्चर्य है कि (विष्वक्) सब ओर (अविरला) व्यवधान रहित (सुरपुष्पवृष्टिः) देवों के द्वारा की हुई पुष्पों की वर्षा (अवाङ्मुखवृन्तम् एव) नीचे डण्ठल और ऊपर को है पांखुरी जिसकी ऐसी ही (कथम्) क्यों (पतति) गिरती है? (यदि वा) अथवा ठीक ही है कि (मुनीश !) हे मुनियों के नाथ ! ( त्वद्गोचरे) आपके समीप (सुमनसाम्) पुष्पों अथवा विद्वानों के (बन्धनानि) डंठल अथवा कर्मों के बन्धन (नूनम् हि) निश्चय से ( अध: एव गच्छन्ति) नीचे को ही जाते हैं ।
टीका - हे विभो ! सुरपुष्पवृष्टि अवाङ्मुखवृन्तमेव यथा स्यात्तथा विष्वक् समन्तात् कथं पतति ? एतन्महच्चित्रं अवाङ्मुखानि अधोमुखानि वृंतानि प्रसवबन्धनानि यत्र क्रियायां तत् वृन्तं प्रसवबन्धनमित्यमरः । सुराणां देवानां पुष्पवृष्टिः। न विरला अविरला निबिडा चेत्यर्थः। यदि वा युक्तोऽयमर्थः । नूनं निश्चितं । भो मुनीश । सुमनसां प्राणिनां त्वद्गोचरे त्वत्सान्निध्ये। बन्धनानि अध एव गच्छन्ति । यथा सुमनसां पुष्पाणां अधोमुखेन वृन्तपतनं तथा बन्धनानि कर्मबन्धनान्यपि सुमनसां प्राणिनां अधो गच्छन्तीति भावः। सुष्ठु मनो येषां ते सुमनसस्तेषां । पुष्पं सुमनसं फुल्लमिति धनञ्जयः ।
भावार्थ - इस श्लोक में सुमनस् शब्द के दो अर्थ हैं - एक फूल और दूसरा विद्वान् या देव । इसी तरह बन्धन शब्द के भी दो अर्थ हैं - एक फूलों का बन्धन डंठल और दूसरा कर्मों के प्रकृति आदि चार तरह के बन्ध। हे भगवन्! जो आपके पास रहता है उसके कर्मों के बन्धन नीचे चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो आपके ऊपर जो फूलों की वर्षा होती है उनमें फूलों के बन्धन नीचे होते हैं और पांखुरी ऊपर। यह ‘पुष्पवृष्टि’ प्रातिहार्य वर्णन है।
दिव्यध्वनि प्रातिहार्य
स्थाने गभीर - हृदयोदधि - सम्भवायाः,
पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति ।
पीत्वा यतः परम - सम्मद - सङ्ग - भाजो,
भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरा-मरत्वम्॥२१॥
अन्वयार्थ – (गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः) गम्भीर हृदयरूपी समुद्र से पैदा हुई (तव) आपकी (गिरः) वाणी के (पीयूषताम् ) अमृतपने को लोग (स्थाने) ठीक ही ( समुदीरयन्ति ) प्रकट करते हैं (यतः) क्योंकि (भव्याः) भव्यजीव (ताम् पीत्वा ) उसे पीकर (परमसम्मदसङ्गभाजः 'सन्तः ') परमसुख के भागी होते हुए (तरसा अपि) बहुत ही शीघ्र ( अजरामरत्वम्) अजर - अमरपने को (व्रजन्ति) प्राप्त होते हैं।
टीका - भो प्रभो ! तव परमेश्वरस्य । गिरः दिव्यध्वनयः । पीयूषतां अमृतभावं। समुदीरयन्ति जना गिरोऽमृतमयाः कथयन्ति । पीयूषस्य भावः पीयूषता तां । एतत् स्थाने इति युक्तं । कुतः यतः कल्याणात् । भव्याः प्राणिनः । या अमृतमया गिरः पीत्वा । तरसापि वेगेन । अजरामरत्वं व्रजन्ति अजरामरस्य भावः अजरामरत्वं। कीदृशाः भव्याः ? परमः सर्वोत्कृष्टः चासौ सम्मदः आनन्दस्तत्सङ्गं संयोगं भजन्ते इत्येवंशीलाः । कथंभूता गिरः ? गम्भीरं च तत् हृदयं च तदेव उदधिः समुद्रः तस्मात्सम्भवः उत्पत्तिर्यासां ताः ।
भावार्थ- लोक में प्रचलित है कि अमृत गहरे समुद्र से निकला था और उसका पान करने से देव लोग अत्यन्त आनन्दित होते हुए अजर- बुढ़ापा रहित तथा अमर=मृत्युरहित हो गये थे । भगवन्! आपकी वाणी भी आपके गंभीर हृदयरूपी समुद्र से पैदा हुई है और उसके सेवन करने से लोक परम सुखी हो अजर-अमर हो जाते हैं- मुक्त हो जाते हैं ऐसी हालत में लोग यदि यह कहें कि आपकी वाणी अमृत है तो ठीक ही कहते हैं । यह ‘दिव्यध्वनि’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
चँवर प्रातिहार्य
स्वामिन्! सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो,
मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः ।
येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय,
ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥२२॥
अन्वयार्थ - ( स्वामिन्!) हे स्वामिन्! ( मन्ये) मैं मानता हूँ कि (सुदूरम्) नीचे को बहुत दूर तक (अवनम्य) नम्रीभूत होकर (समुत्पतन्तः) ऊपर को आते हुए (शुचयः ) पवित्र (सुरचामरौघाः) देवों के चँवर- समूह ( वदन्ति) लोगों से कह रहे हैं कि (ये) जो (अस्मै मुनिपुङ्गवाय ) इन श्रेष्ठ मुनीन्द्र को (नतिम्) नमस्कार ( विदधते) करते हैं, (ते) वे ( नूनम् ) निश्चय से (शुद्धभावाः) विशुद्ध परिणाम वाले होकर (ऊर्ध्वगतयः) ऊर्ध्वगति वाले (खलु भवन्ति) सचमुच हो जाते हैं अर्थात् स्वर्ग/मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।
टीका - भो स्वामिन्! अहं एवं मन्ये इति सम्भावयामि । इतीति किं? शुचय उज्जवलाः। सुरचामरौघा देवानां चतुःषष्टिचामरयुग्मानि । सुदूरं अतिसमीपं । यथा स्यात्तथा अवनम्य अल्पं मस्तकोपरि निपत्य । समुत्पतन्तः सन्तः। इति वदन्ति इति भणन्ति इतीति किं ? ये पुरुषा अस्मै मुनिपुंगवाय समवसरणविराजमानतीर्थङ्कर श्रीपार्श्वनाथाय । नतिं नमस्कारं । विदधते कुर्वते । ते भव्याः नूनं खलु इति सत्ये । शुद्धभावाः सन्तः ऊर्ध्वगतयो भवन्ति। यथा वयं चामरौघाः अवनम्राः सन्तः ऊर्ध्वगतयस्तथा भवन्तः अपि भवन्ति । शुद्धभावः सम्यक्त्वं येषां ते ।
**भावार्थ–**हे भगवन्! जब देवलोग आप पर चँवर ढोरते हैं तब वे चँवर पहले नीचे की ओर झुकते हैं और बाद में ऊपर को जाते हैं, सो मानों लोगों से यह कहते हैं कि भगवान् को झुककर नमस्कार करने वाले पुरुष हमारे समान ही ऊपर को जाते हैं अर्थात् स्वर्ग मोक्ष को पाते हैं । यह ‘चॅवर’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
सिंहासन प्रातिहार्य
श्यामं गभीर - गिर- मुज्ज्वल - हेमरत्न-
सिंहासनस्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् ।
आलोकयन्ति रभसेन नदन्त - मुच्चैश्-,
चामीकराद्रि-शिरसीव नवाम्बुवाहम्॥२३॥
अन्वयार्थ— (इह) इसलोक में (श्यामम्) श्याम वर्ण (गभीर- गिरम्) गम्भीर दिव्यध्वनि युक्त और (उज्ज्वलहेमरत्नसिंहासनस्थं) उज्ज्वल स्वर्ण से निर्मित रत्नों से जड़ित सिंहासन पर स्थित (त्वाम्) आपको (भव्य-शिखण्डिनः) भव्यजीवरूपी मयूर (चामीकराद्रिशिरसि) सुवर्णमय मेरुपर्वत के शिखर पर (उच्चैः नदन्तम् ) उच्च स्वर से गरजते हुए (नवाम्बुवाहम् इव) नूतन मेघ की तरह ( रभसेन) अति उत्सुकता से (आलोकयन्ति) देखते हैं।
टीका- भो विभो ! भव्यशिखण्डिनः भव्यलक्षणाः शिखण्डिनो मयूराः इह लोके त्वां । रभसेन वेगेन । आलोकयन्ति । भव्या एव शिखण्डिनः भव्यशिखण्डिनः। कीदृशं त्वां ? गभीरा तत्त्वार्थे अत्यन्तमगाधा धीर्यस्य स तं । पुनः कीदृशं त्वां ? उज्ज्वलैर्निर्मलैर्हेमरत्नैः खचिते सिंहासने तिष्ठतीति तं । पुनः कीदृशं त्वां ? चामीकराद्रिशिरसि मेरोः शृङ्गे । उच्चैर्नदन्तं नवाम्बुवाहमिव नवमेघमिवोत्प्रेक्षा । चामीकराद्रेः शिरस्तस्मिन् । नवश्चासौ अम्बुवाहश्च तम्।
भावार्थ- हे प्रभो ! जिस तरह सुवर्णमय मेरुपर्वत उमड़ते-घुमड़ते हुए गर्जना करने वाले काले मेघ को देखकर मयूरों को बहुत ही आनन्द होता है उसी तरह दिव्यध्वनि करते हुए तथा सोने के सिंहासन पर विराजमान श्यामवर्ण वाले आपके दर्शन कर भव्य जीवों को अत्यन्त आनन्द होता है । उनका मन मयूर की तरह नाचने लगता है । यह ‘सिंहासन’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
भामण्डल प्रातिहार्य
उद्गच्छता तव शिति-द्युति- मण्डलेन,
लुप्तच्छदच्छवि -रशोक -तरुर्बभूव ।
सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !,
नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ॥२४॥
अन्वयार्थ— (उद्गच्छता) स्फुरायमान (तव) आपके (शितिद्युति- मण्डलेन) श्याम प्रभामण्डल के द्वारा (अशोकतरुः) अशोकवृक्ष (लुप्तच्छदच्छविः) कान्तिहीन पत्रों वाला (बभूव) हो गया (यदि वा ) अथवा (वीतराग !) हे राग-द्वेष रहित देव ! ( तव सान्निध्यतः अपि ) आपकी समीपता मात्र से ही (क: सचेतनः अपि) कौन पुरुष सचेतन भी (नीरागताम् ) राग / ललाई से रहितपने अथवा अनुराग के अभाव को (न व्रजति) नहीं प्राप्त होता ? अर्थात् प्राप्त होता है ।
टीका - भो वीतराग! अशोकतरुः । तव भगवतः। उद्गच्छता उदीयमानेन शितिद्युतिमण्डलेन उज्ज्वलभामण्डलेन । लुप्तच्छदानां पत्राणां छविः शोभा । यस्य स एवंविधो बभूव । शिति च तद्द्युतिमण्डलं च शितिद्युतिमण्डलं तेन । यदि वा युक्तोऽयमर्थः । तव सान्निध्यतोऽपि । कः सचेतनोऽपि सुज्ञोऽपि । नीरागतां रागेच्छारहिततां न व्रजति ? अपि तु व्रजतीत्याशयः। चेतनेन सह वर्तमानः सचेतनः ।
भावार्थ- हे भगवन्! आपकी श्यामल कान्ति के संसर्ग से अशोक वृक्ष की लालिमा दब गई सो ठीक ही है, वीतराग (ललाई रहित, दूसरे पक्ष में स्नेहरहित) के सामीप्य से कौन सचेतन - प्राणी वीतराग (ललाई रहित, दूसरे पक्ष में स्नेह रहित ) नहीं हो जाता? अर्थात् सभी हो जाते हैं । इस श्लोक में रागपद दो अर्थ वाला है - अनुराग - प्रेम - स्नेह और दूसरा लालिमा- ललाई। यह ‘भामण्डल’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
दुन्दुभि प्रातिहार्य
भो भोः प्रमाद - मवधूय भजध्वमेन-,
मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् ।
एतन् निवेदयति देव! जगत्त्रयाय,
मन्ये नदन्नभिनभः सुर दुन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥
अन्वयार्थ - (देव ! ) हे देव! (मन्ये) मैं समझता हूँ कि (अभिनभः) आकाश में सब ओर (नदन्) शब्द करती हुई (ते) आपकी (सुर दुन्दुभिः) देवों के द्वारा बजाई गई दुन्दुभि (जगत्त्रयाय) तीन लोकों के जीवों को (एतत् निवेदयति) यह सूचित करती है कि (भो भोः) रे प्राणियों ! (प्रमादम् अवधूय) प्रमाद को छोड़कर (निर्वृतिपुरीम् प्रति सार्थवाहम्) मोक्षपुरी को जाने में अगुवा (एनं ) इन पार्श्वनाथ भगवान् को (आगत्य) आकर (भजध्वम्) भजो / सेवा करो ।
टीका - भो देव! अहं एवं मन्ये एवं सम्भावयामि । ते तव । सुरदुन्दुभिःदेवपटहः। अभिनभः नभः समन्तात्। नदन्। जगत्त्रयाय त्रैलोक्याय एतन्निवेदयति । सुराणां दुन्दुभिः सुरदुन्दुभिः । एतत् किं ? भो भो जनाः प्रमादं अवधूय आलस्यं परित्यज्य । आगत्य समेत्य । एवं श्रीपार्श्वनाथं । भजध्वं सेवध्वं । कथंभूतं एवं? निवृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् ।
भावार्थ–हे प्रभो! आकाश में जो देवों का नगाड़ा बज रहा है वह मानों तीन लोक के जीवों को चिल्ला-चिल्ला कर सचेत कर रहा है कि जो मोक्षनगरी की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं वे प्रमाद छोड़कर भगवान् पार्श्वनाथ की सेवा करें। यह ‘दुन्दुभि’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
छत्रत्रय प्रातिहार्य
उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ!
तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः ।
मुक्ता कलाप कलितोल्लसितातपत्र -,
व्याजात्त्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः॥२६॥
अन्वयार्थ– (नाथ!) हे नाथ! ( भवता भुवनेषु उद्योतितेषु दिन विद्यापीठ ‘सत्सु’) आपके द्वारा तीनों लोकों के प्रकाशित होने पर (विहताधिकारः) अपने अधिकार से भ्रष्ट तथा (मुक्ताकलाप - कलितोल्लसितातपत्र- व्याजात्) मोतियों के समूह से सहित अतएव शोभायमान सफेद छत्र के छल से (तारान्वितः ) ताराओं से वेष्टित (अयम् विधुः ) यह चन्द्रमा (त्रिधा धृततनुः ) तीन-तीन शरीर धारण कर (ध्रुवम् ) निश्चय से ( त्वाम् अभ्युपेतः) आपकी सेवाओं में प्राप्त हुआ है।
टीका- भो नाथ! अयं तारान्वितो नक्षत्रग्रहतारकान्वितो विधुश्चन्द्रः ध्रुवं निश्चितं । अभ्युपेतः समेतः केषु सत्सु । भवता परमेश्वरेण । भुवनेषु त्रैलोक्येषु । उद्योतितेषु सत्सु । कथंभूतोऽयं ? विहतः अधिकारो येन सः । पुनः कथंभूतोऽयं ? मुक्तानां कलापः समूहस्तेन कलितं सहितं उल्लसितं शोभायमानं च तत् आतपत्रं च तस्य व्याजं मिषं । तस्मात् त्रिधा धृततनुः शरीरं येन सः ।
भावार्थ- हे प्रभो ! जब आपने अपनी कांति वा ज्ञान से तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया तब मानों चन्द्रमा का प्रकाश करने रूप अधिकार छीन लिया गया। इसलिए वह तीन छत्र का वेष धरकर आपकी सेवा में अपना अधिकार वापस चाहने के लिए उपस्थित हुआ है। छत्रों में जो मोती लगे हुए हैं वे मानों चन्द्रमा के परिवारस्वरूप तारागण हैं। यह ‘छत्रत्रय’ प्रातिहार्य का वर्णन है ।
समवसरण में तीन प्रकोट
स्वेन प्रपूरित जगत्त्रयपिण्डितेन,
कान्ति - प्रताप - यशसामिव सञ्चयेन ।
माणिक्य हेम - रजत प्रविनिर्मितेन,
सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥२७॥
अन्वयार्थ – (भगवन्) हे भगवन्! आप (अभितः) चहुँ ओर (प्रपूरित - जगत्त्रय-पिण्डितेन) भरे हुए तीनों जगत् के पिण्ड अवस्था को प्राप्त (स्वेन कान्ति-प्रताप - यशसाम् सञ्चयेन इव) अपने कान्ति, प्रताप और यश के समूह के समान (माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन) माणिक्य, सुवर्ण और चाँदी से बने हुए (सालत्रयेण ) तीनों कोटों से (विभासि) शोभायमान होते हैं ।
टीका- भो भगवन्! शालत्रयेण प्राकारत्रयेण । त्वं अभितः समन्तात् । विभासि शोभसे । कथम्भूतेन सालत्रयेण ? माणिक्यानि च हेमानि च रजतानि च माणिक्यहेमरजतानि तैः निर्मितं तेन । केनेव कान्तिप्रतापयशसां संचयेनेव ? यथा स्वेन कान्तिप्रतापयशसां सञ्चयेन त्वं विभासि । कान्तिश्च प्रतापश्च यशश्च कान्तिप्रतापयशान्सि तेषां । कथम्भूतेन संचयेन ? प्रपूरितं च जगत्त्रयं च प्रपूरितजगत्त्रयं प्रपूरित जगत्त्रयेण पिण्डितः एकीभूतस्तेन । इति तात्पर्यार्थः ।
भावार्थ- हे भगवन्! समवसरण भूमि में जो आपके चारों ओर माणिक्य सुवर्ण और चाँदी के बने हुए तीन कोट हैं वे मानों आपकी कांति प्रताप और यश का वह समूह है जो कि तीनों जगत् में फैला हुआ है।
इन्द्रों द्वारा वन्दनीय
दिव्यस्रजो जिन! नमत्रिदशाधि पाना-
मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् ।
पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र,
त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव॥२८॥
अन्वयार्थ - (जिन!) हे जिनेन्द्र ! (दिव्यस्रजः ) दिव्य पुष्पों की मालाएँ (नमत् त्रिदशाधिपानाम् ) नमस्कार करते हुए इन्द्रों के (रत्नरचितान् अपि मौलिबन्धान्) रत्नों से बने हुए मुकुटों के बंधनों को भी (उत्सृज्य) छोड़कर (भवतः पादौ श्रयन्ति) आपके चरणों का आश्रय लेती हैं (यदि वा) अथवा ठीक है कि ( त्वत्सङ्गमे ‘सति’) आपका समागम होने पर (सुमनसः ) पुष्प मालाएँ या उत्तम हृदय वाले मनुष्य (परत्र) किसी दूसरी जगह (न एव रमन्ते) नहीं रमण करते हैं ।
टीका - भो जिन ! दिव्यस्रजः मनोज्ञपुष्पमालाः । नमत्रिदशाधिपानां प्रणमत्त्रिदशेन्द्राणां । रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् रत्नखचितान् किरीटान् । उत्सृज्य। भवतः परमेश्वरस्य । पादौ श्रयन्ति । नमन्तश्च ते त्रिदशाधिपाश्च तेषां । रत्नैः रचितास्तान् । मौलिनां बन्धाः मौलिबन्धास्तान् । यदि वा युक्तोऽयमर्थः। सुमनसः प्राणिनः । त्वत्सङ्गमे त्वत्समीपे। सति परत्र अन्यत्र। न रमन्त एव। इति स्थूलार्थः।
भावार्थ - श्लोक में आये हुए सुमनस् शब्द के दो अर्थ हैं- एक पुष्प और दूसरा विद्वान् पुरुष । हे भगवन्! नमस्कार करते समय देवों के मुकुटों में लगी हुई फूलों की मालाएँ जो आपके चरणों में गिर जाती हैं सो मानों वे पुष्पमालाएँ आपसे इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उनके पीछे देवों के रत्नों से बने हुए मुकुटों को भी छोड़ देती हैं । सुमनस=फूलों का (दूसरे पक्ष में- विद्वानों का) आप में अगाध प्रेम होना उचित ही है । श्लोक का तात्पर्य यह है कि आपके लिए बड़े इन्द्र भी नमस्कार करते हैं ।
संसार समुद्र तारक विभु
त्वं नाथ! जन्मजलधेर्विपराङ्मुखोऽपि,
यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठलग्नान्।
युक्तं हि पार्थिवनृपस्य सतस्तवैव,
चित्रं विभो ! यदसि कर्मविपाकशून्यः ॥२९॥
अन्वयार्थ – (नाथ!) हे नाथ! (त्वम्) आप (जन्म - जलधे:) संसाररूप समुद्र से (विपराङ्मुखः अपि सन्) पराङ्मुख होते हुए भी (यत्) जो (निज-पृष्ठलग्नान्) अपने पीछे लगे हुए अनुयायी (असुमतः ) जीवों को (तारयसि ) तार देते हो (‘तत्’) वह (पार्थिवनृपस्य सतः ) राजाधिराज अथवा मिट्टी के पके हुए घड़े की तरह परिणमन करने वाले (तव) आपको (युक्तम् एव) उचित ही है, परन्तु (विभो ) हे प्रभो ! (तत् चित्रम्) वह आश्चर्य की बात है (यत्) जो आप (कर्मविपाकशून्यः असि) कर्मों के उदयरूप पाक क्रिया से रहित हो ।
टीका— भो नाथ! त्वं जन्मजलधेः भवसमुद्रात् विपराङ्मुखोपि सन् निजपृष्ठलग्नान् असुमतः प्राणिनः यत्तारयसि हि निश्चितं तवैव सतो विद्यमानस्य पार्थिवनृपस्य राजाधिराजस्य त्रिजगत्स्वामिनः युक्तं । हे विभो ! यत्कर्मविपाक-शून्योऽसि तच्चित्रं । यः कोऽपि तारयति स फलं वाञ्छति तव क्वाऽपि वाञ्छा न। अथवा यः कोऽपि कार्यं किमपि करोति तस्य शुभाशुभकर्मबन्धो भवति तव सोऽपि नास्तीति चित्रं महदाश्चर्यं । पार्थिवनृपस्य घटस्य जलधेः विपराङ्-मुखतारकत्वं युक्तं तस्य घटस्य कर्मविपाकशून्यता नास्ति। स तु घटः कर्मविपाकसहितः। जन्मैव जलधिस्तस्मात् । निजपृष्ठ- लग्नांस्तान्। पार्थिवानां नृपः स्वामी तस्य । घटपक्षे पृथिव्यां अयं पार्थिवः। नॄन् मनुष्यान् । जलदानेन पातीति नृपः । पार्थिवश्चासौ नृपश्च पार्थिवनृपस्तस्य । कर्मणां बन्धः अष्टकर्मणां विपाक उदयस्तेन शून्यः । घटपक्षे कर्मवद्विपाकः पचनं तेन शून्यो न । अत्र श्लेषालङ्कारः ।
भावार्थ- जिस तरह घड़ा पानी में अधोमुख होकर अपनी पीठ पर स्थित लोगों को नदी आदि से पार कर देता है, उसी तरह आप यद्यपि राग न होने से संसार - समुद्र से पराङ्मुख रहते हैं तथापि अपने अनुयायियों को उससे पार लगा देते हैं - मोक्ष प्राप्त करा देते हैं । पर जब घड़ा अग्नि से पकाया हुआ हो तभी पानी में तैर कर दूसरों को पार करता है। कच्चा घड़ा पानी में गल कर घुल जाता है, किन्तु आप पाक रहित हो यह आश्चर्य की बात है। उसका परिहार यह है कि आप कर्मों के उदय से रहित हैं। श्लोक में आये हुए विपाक शब्द के दो अर्थ हैं- अग्नि से किसी कोमल मिट्टी की वस्तु का कठोर होना और कर्मों का उदय आना ।
विरोधाभास गुण स्तुति
विश्वेश्वरोऽपि जनपालक ! दुर्गतस्त्वम्,
किं वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश ! |
अज्ञान वत्यपि सदैव कथञ्चिदेव,
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः ॥३०॥
अन्वयार्थ - (जनपालक!) हे जीवों के रक्षक ! (त्वम्) आप (विश्वेश्वरः अपि दुर्गतः) तीन लोक के स्वामी होकर भी दरिद्र हैं, (किं वा) और (अक्षरप्रकृतिः अपि त्वम् अलिपिः) अक्षरस्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से रहित हैं (ईश!) हे स्वामिन्! (कथञ्चित्) किसी प्रकार से (अज्ञानवति अपि त्वयि ) अज्ञानवान् होने पर भी आपमें (विश्व - विकासहेतुः ज्ञानम् सदा एव स्फुरति ) सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान हमेशा स्फुरायमान रहता है ।
टीका– जनान्पालयतीति जनपालकः तस्यामन्त्रणे हे जनपालक ! त्वं विश्वेश्वरोऽपि त्रैलोक्यनाथोऽपि सन् दुर्गतः किं दरिद्रः कथमिति विरोधः शब्दतः । द्रष्टुं ज्ञातुमशक्यं गतं यस्य सः । वा अथवा भो ईश ! भो विभो ! त्वं अक्षरप्रकृतिरपि वर्णस्वरोऽपि अलिपिः कथं । अक्षरा अविनश्वरा प्रकृतिः स्वभावो यस्य सः। न विद्यते लिपिर्मोहो यस्य सः । यः अक्षरः प्रकृति क्षरतीति क्षरः न क्षरतीति अक्षरः सो लिपिर्न भवति । इति शब्दतो विरोधः नार्थतः। भो जिन ! त्वयि सदैव अज्ञानवत्यपि सति ज्ञानरहितेऽपि सति कथञ्चिदेव विश्वविकासहेतुज्ञानं स्फुरति । योऽज्ञानवांस्तस्मिन् ज्ञानं क्वेति शब्दतो विरोधः नार्थतः। अज्ञानप्राणिनोऽवतीति तस्मिन् । विश्वेषां विकाशः प्रकटीकरणं तस्य हेतुर्निदानं ।
भावार्थ - इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है । विरोधाभास अलंकार में शब्द के सुनते समय तो विरोध मालूम होता है पर अर्थ विचारने पर बाद में उसका परिहार हो जाता है । जहाँ इस अलंकार का मूल श्लेष होता है वहाँ बहुत ही अधिक चमत्कार पैदा हो जाता है। देखिये-भगवन्! आप विश्वेश्वर होकर भी दुर्गत हैं। यह पूरा विरोध है भला, जो (जगत् का ईश्वर है वह दरिद्र कैसे हो सक्ता है ? विश्वेश्वर होकर भी दुर्गत = कठिनाई से जाने जा सकते हैं। इसी तरह आप अक्षर प्रकृति- अक्षर स्वभाव वाले होकर भी अलिपि लिखे नहीं जा सकते यह विरोध है । जो क ख आदि अक्षरों जैसा है वह लिखा क्यों न जायेगा ?) परन्तु दोनों शब्दों का श्लेष विरोध को दूर कर देता है । आप अक्षर प्रकृति-अविनश्वर स्वभाववाले होकर भी अलिपि = आकार रहित हैं-निराकार हैं। इसी प्रकार अज्ञानवति अपि अज्ञान युक्त होने पर भी आपमें विश्वविकाशि ज्ञानं स्फुरति संसार के सब पदार्थों को जानने वाला ज्ञान स्फुरायमान होता है, यह विरोध है । जो अज्ञानयुक्त है उसमें पदार्थों का ज्ञान कैसा? पर इसका भी नीचे लिखे अनुसार परिहार हो जाता है - अज्ञान अवति अपि त्वयि - अज्ञानी मनुष्यों की रक्षा करने वाले आप में हमेशा केवलज्ञान जगमगाता रहता है।
उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ
प्राग्भार-सम्भृत-नभांसि रजांसि रोषा -,
दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि ।
छायापि तैस्तव न नाथ! हता हताशो,
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥
अन्वयार्थ - (नाथ) हे स्वामिन्! (शठेन कमठेन) दुष्ट कमठ के द्वारा (रोषात्) क्रोध से (प्राग्भार - सम्भृतनभांसि) सम्पूर्णरूप से आकाश को व्याप्त करने वाली (यानि) जो ( रजांसि ) धूल (उत्थापितानि) आपके ऊपर उड़ाई गई थी (तै: तु) उससे तो (तव) आपकी ( छाया अपि) छाया भी (न हता) नहीं नष्ट हुई थी (परम् ) किन्तु (अयमेव दुरात्मा) यही दुष्ट (हताश:) हताश हो ( अमीभि:) इन कर्मरूप रजों से (ग्रस्तः ) जकड़ा गया था।
टीका - भो नाथ! शठेन मूर्खेण । कमठेनेति कमठचरसंवरनाम ज्योतिष्कदेवेन । रोषात् पूर्वोपार्जितवैरात् । यानि रजांसि उत्थापितानि तैः । स्वरजोभिः तव भगवतश्च्छायापि प्रतिबिम्बमपि न हतं न स्पृष्टं । अपि तु परं केवलं अमीभिः अयमेव पापीयान् कमठ एव ग्रस्तः मलिनीकृतः । कथंभूतोऽयं? हता आशा यस्य स हताशः । प्राग्भारेण सामस्त्येन सम्भृतं व्याप्तं नभो यैस्तानि ।
भावार्थ– जब भगवान् पार्श्वनाथ तपस्या कर रहे थे तब उनके पूर्वभव के वैरी कमठ के जीव ने उन पर धूल उड़ाकर भारी उपसर्ग किया था। लोक में यह देखा जाता है कि जो सूर्य पर धूल फेंकता है उससे सूर्य की जरा भी कान्ति नष्ट नहीं होती, पर वही धूली फेंकने वाले के ऊपर गिरती है। श्लोक में आये हुए रज शब्द के दो अर्थ हैं - एक धूलि, दूसरा कर्म। कमठ के जीव ने भगवान् पर उपसर्ग कर कर्मों का बन्ध किया था इस बात को कवि ने लोक-प्रचलित उक्त उदाहरण से स्पष्ट किया है।
जलवृष्टि उपसर्ग
यद्गर्जदूर्जित— घनौघ मदभ्रभीम्,
भ्रश्यत्तडिन्मुसल- मांसल - घोरधारम् ॥
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दधे,
तेनैव तस्य जिन ! जिन! दुस्तरवारिकृत्यम् ॥३२॥
अन्वयार्थ - (अथ) और (जिन!) हे जिनेश्वर ! (दैत्येन) उस कमठ ने (गर्जदूर्जितघनौघम् ) खूब गरज रहे हैं बलिष्ठ - मेघ - समूह जिसमें (भ्रश्यत् - तडित् ) गिर रही है बिजली जिसमें और ( मुसलमांसल - घोर- धारम्) मूसल के समान बड़ी मोटी है धारा जिसमें ऐसा तथा (अदभ्रभीमम्) अत्यन्त भयंकर (यत्) जो (दुस्तर - वारि) अथाह जल (मुक्तम्) वर्षाया था, (तेन) उस जलवृष्टि से ( तस्य एव ) उस कमठ ने ही अपने लिए (दुस्तरवारिकृत्यम् दध्रे) तीक्ष्ण तलवार के कार्य को धारण किया अर्थात् उससे वह कमठ स्वयं ही घायल हो गया ।
टीका - भो जिन ! यत् दैत्येन कमठदानवेन दुस्तरवारि दुर्द्धरपानीयं मुक्त भवान् दध्रे। अथ पुनस्तस्य कमठस्य तेनैव पानीयेन दुस्तरवारिकृत्यं जातं । दुस्तरं दुस्सहं यत् दुस्तरवारि दुष्ठु यो हि तरवारिश्चञ्चत्खड्गस्- तद्वत्कृत्यं यस्य तत् एवंविधं समजनि । कथंभूतं दुस्तरवारि ? गर्जिता ऊर्जिता महत्तरा ये घना मेघास्तेषां ओघा यस्मिंस्तत् । मुसलवन्मांसलाः स्थूला घोरां भयदा धारा यस्मिंस्तत् ।
भावार्थ- हे भगवन्! आप पर मूसलधार पानी वर्षाकर कमठ के जीव ने जो उपसर्ग किया था उससे आपका क्या बिगड़ा? परंतु उसी ने अपने लिए ‘दुस्तरवारिकृत्यं’ दुष्ट तलवार का कार्य अर्थात् घाव कर लिया-ऐसे कर्मों का बन्ध किया जो तलवार के घाव के समान दुःखदायी हुए थे । श्लोक में ‘दुस्तरवारि’ शब्द दो वार आया है उनमें से पहले का अर्थ कठिनाई से तरने योग्य जल है और दूसरे का अर्थ दुष्ट तरवारि- तलवार है।
भूत पिशाचों के द्वारा उपसर्ग
ध्वस्तोर्ध्व-केश-विकृताकृति - मर्त्य-मुण्ड-
प्रालम्बभृद्भयद वक्त्र विनिर्यदग्निः ।
प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः,
सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः॥३३॥
अन्वयार्थ– (ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्ड - प्रालम्बभृद्) मुंडे हुए तथा विकृत आकृति वाले नर कपालों की माला को धारण करने वाला और (भयद-वक्त्रविनिर्यदग्निः) जिसके भयंकर मुख से अग्नि निकल रही है, ऐसा (यः) जो (प्रेतव्रजः) पिशाचों का समूह ( भवन्तम् प्रति) आपके प्रति (ईरितः ) प्रेरित किया गया था - दौड़ाया गया था (सः) वह (अस्य) उस असुर को (प्रतिभवम्) प्रत्येक भव में (भव-दुःखहेतुः) संसार के दुःखों का कारण (अभवत्) हुआ था ।
टीका- भो परमेश्वर! यः प्रेतव्रजो भूतसमूहः भवन्तं श्रीमन्त प्रत्यपि । ईरितः प्रेरितः। स प्रेतव्रजः । अस्य कमठस्य । प्रतिभवं भवं प्रति । भवस्य संसारस्य। दुःखानां हेतुः । अभूत् बभूव । प्रेतानां व्रजः प्रेतव्रजः। ध्वस्ता विस्तारिता ये ऊर्ध्वकेशास्तैर्विकृता विकारिण्य आकृतयो येषां ते ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतय एवं विधा ये मर्त्यास्तेषां मुण्डानि कपालानि तेषां प्रालम्बमालां बिभर्तीति । पुनः कथं प्रेतव्रजः ? भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः भयदायि यद्वक्त्रं तस्माद्वि-निर्यन्त निःसरन्तोऽग्नयो यस्य सः ।
भावार्थ– हे भगवन्! कमठ के जीव ने आपको तपस्या से विचलित करने के लिए जो पिशाच दौड़ाये थे उनसे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ परंतु उस पिशाच को ही भारी कर्म - बंध हुआ जिससे उसे अनेक भवों में दुःख उठाने पड़े ।
प्रभु भक्त धन्यवाद का पात्र
धन्यास्त एव भुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य-
माराधयन्ति विधिवद् विधुतान्य- कृत्याः ।
भक्त्योल्लसत्पुलक - पक्ष्मल - देह - देशा:,
पादद्वयं तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ॥३४॥
अन्वयार्थ - (भुवनाधिप ! ) हे त्रिलोकीनाथ! (ये) जो (जन्म- भाजः) प्राणी, (विधुतान्यकृत्याः) जिन्होंने अन्य काम छोड़ दिए हैं और (भक्त्या) भक्ति से (उल्लसत् - पुलक- पक्ष्मल - देहदेशाः ‘सन्तः’) प्रकट हुए रोमाञ्चों से जिनके शरीर का प्रत्येक अवयव व्याप्त है, ऐसे होते हुए (विधिवत्) विधिपूर्वक (त्रिसन्ध्यम्) तीनों कालों में (तव) आपके (पादद्वयम् आराधयन्ति) चरणयुगल की आराधना करते हैं (विभो !) हे स्वामिन्! (भुवि) संसार में (ते एव) वे ही (धन्याः) धन्य हैं ।
टीका - भो भुवनाधिप ! भो विभो ! भुवि पृथिव्यां । त एव जन्मभाजो धन्याः पुण्यवन्तः ते के? ये जन्मभाजः प्राणिनः । त्रिसन्ध्यं त्रिकालं । भक्त्या श्रद्धया । तव विभो । पादद्वयं चरणकमलं । विधिवत् विध्युक्तप्रकारेण । आराधयन्ति निषेवन्ते । कीदृशास्ते ? विधूतानि स्फेटितानि अन्यानि कृत्यानि । यैस्ते। पुनरुल्लसन्तश्च ते पुलकाश्च तैः पक्ष्मलाः कलङ्किता व्याप्ता वा देहस्य शरीरस्य प्रदेशा येषां ते ।
भावार्थ- हे भगवन्! संसार में उन्हीं का जन्म सफल है जो भक्तिपूर्वक आपके चरणों की आराधना करते हैं ।
प्रभु नाम श्रवण से विपदा मुक्ति
अस्मिन्त्रपार - भव - वारि निधौ मुनीश !,
मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि ।
आकर्णिते तु तव गोत्र - पवित्र - मन्त्रे,
किं वा विपद् - विषधरी सविधं समेति ॥ ३५ ॥
अन्वयार्थ - ( मुनीश ! ) हे मुनीन्द्र ! ( मन्ये) मैं समझता हूँ कि (अस्मिन् अपारभव- वारिनिधौ) इस अपार संसाररूप समुद्र में कभी भी आप (मे) मेरे (श्रवणगोचरतां न गतः असि) कानों की विषयता को प्राप्त नहीं हुए हो क्योंकि (तु) निश्चय से (तव गोत्रपवित्रमन्त्रे आकर्णिते ‘सति’) आपके नामरूपी पवित्र मन्त्र के सुने जाने पर ( विपद् - विषधरी) विपत्तिरूपी नागिन (किम् वा ) क्या (सविधम् ) समीप (समेति) आती है? अर्थात् नहीं ।
टीका - भो मुनीश ! अहमेवं मन्ये इति सम्भावयामि । इतीति किं ? अस्मिन् प्रत्यक्षगोचरीभूते । अपारवारिनिधौ अगाधसंसारसमुद्रे । मे मम । श्रवणगोचरतां कर्णयमलप्रत्यक्षभावं । त्वं न गतोऽसि न प्राप्तोऽसि । अपारो अगाधो यो भव एव वारिनिधिस्तस्मिन् । श्रवणयोः कर्णयोः गोचरता प्रत्यक्षभावता तां। वा अथवा । तव भगवतो गोत्रपवित्रमन्त्रे तव भगवतः पावनमन्त्रे। आकर्णितेऽपि सति । विपद्विषधरी आपदभुजङ्गी । किं सविधं समीपं । समेति आगच्छति ? अपि तु न समेतीत्यर्थः । गोत्रं नाम तल्लक्षणो यः पवित्रमन्त्रस्तस्मिन् । विपदेव विषधरी सर्पिणी विपद्विषधरी ।
भावार्थ- हे प्रभो ! जो मैं संसार में अनेक दुःख उठा रहा हूँ उससे विश्वास होता है कि मैंने कभी भी आपका पवित्र नाम नहीं सुना।
प्रभुपद पूजे बिन मिले विपद
जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव!,
मन्ये मया महितमीहित - दान दक्षम्।
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां,
जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्॥३६॥
अन्वयार्थ— (देव!) हे देव! (मन्ये) मैं मानता हूँ कि मैंने (जन्मान्तरे अपि) दूसरे जन्म में भी (ईहितदानदक्षम्) मनोवांछित फल देने में समर्थ (तव पादयुगम्) आपके चरणयुगल (न महितम्) नहीं पूजे, (तेन) उसी से (इह जन्मनि) इस भव में (मुनीश ! ) हे मुनीश ! (अहम् ) मैं (मथिताशयानाम्) हृदयभेदी - मनोरथों को नष्ट करने वाले (पराभवानाम्) तिरस्कारों का (निकेतनम् ) घर (जातः) हुआ हूँ ।
टीका – हे देव! अहमेवं मन्ये मया जन्मान्तरेऽपि एकस्मिन् जन्मन्यपि। तवार्हतं। पादयुगं चरणद्वन्द्वं । न महितं न पूजितमित्यर्थः । एकस्माज्जन्मनोऽन्यज्जन्म जन्मान्तरं तस्मिन् । कीदृशं पादयुगं ? ईहितं अभिलषितं तस्य दानं प्रदानं तत्र दक्षं । भो मुनीश ! तेन कारणेन भवच्चरणापूजनहेतुना इह जन्मनि इह भवान्तरेऽपि । अहं पराभवानां आपदां । पात्रं स्थानं । जातोस्मि अभूवं । कथंभूतानां पराभवानां? मथितः विलोडितः आशयश्चित्तं यैस्ते तेषाम् ।
भावार्थ - हे भगवन्! जो मैं तरह तरह के तिरस्कारों का पात्र हो रहा हूँ उससे स्पष्ट पता चलता है कि मैंने आपके चरणों की पूजा नहीं की। क्योंकि आपके चरणों के पुजारियों का कभी किसी जगह भी तिरस्कार नहीं होता ।
दर्शन बिन दुःख पाये
नूनं न मोह - तिमिरावृतलोचनेन,
पूर्वं विभो ! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि ।
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः,
प्रोद्यत्प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते ॥३७॥
अन्वयार्थ – (विभो ) हे स्वामिन्! ( मोहतिमिरावृतलोचनेन ) मोहरूपी अन्धकार से आच्छादित हैं नेत्र जिसके ऐसे (मया) मेरे द्वारा आप (पूर्वम्) पहले कभी (सकृद् अपि) एक बार भी (नूनम् ) निश्चय से (प्रविलोकितः न असि) अच्छी तरह अवलोकित नहीं हुए हो अर्थात् मैंने आपके दर्शन नहीं किए (अन्यथा हि) नहीं तो जो (प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः) जिनमें कर्मबन्ध की गति बढ़ रही है ऐसे (एते) ये (मर्माविध:) मर्मभेदी (अनर्थाः) अनर्थ (माम्) मुझे ( कथम्) क्यों (विधुरयन्ति) दुःखी करते ?
टीका - भो विभो । नूनं निश्चितं । मोह एव तिमिराणि अन्धकाराणि तैरावृते उज्झम्पिते छादिते लोचने यस्य स तेनैवं विधेन मया । पूर्वं प्रागेव । सकृदपि एकवारमपि । त्वं न प्रविलोकितोऽसि नयनगोचरीभावं न गतोऽसि । हि युक्तोऽयमर्थः । अन्यथा चेत् त्वं मम नयनगोचरीभावं गतश्चेत् । एते अनर्थाः जन्ममृत्युजरादयः मां कथं विधुरयन्ति पीडयन्ति ? कथम्भूता अनर्थाः ? प्रोद्यन्त्य उदीयमानाः प्रबन्धानां कर्मबन्धानां गतयो येषु ते । पुनः कथम्भूता ? मर्माविधो मर्मभेदकाः ।
भावार्थ- भगवन्! मैंने मिथ्यात्व के उदय से अन्धे होकर कभी भी आपके दर्शन नहीं किये। यदि दर्शन किये होते तो आज ये दुःख मुझे दुःखी कैसे करते? क्योंकि आपके दर्शन करने वालों को कभी कोई भी अनर्थ दुःख नहीं पहुँचा सकते ।
भाव शून्य करनी फलदायक नहीं
आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षतोऽपि,
नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जनबान्धव! दुःखपात्रं,
यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥३८॥
अन्वयार्थ - अथवा (जनबान्धव !) हे जगत् बन्धु ! (मया) मेरे द्वारा आप (आकर्णित: अपि) सुने हुए भी हैं (महित: अपि ) पूजित भी हुए हैं और (निरीक्षित: अपि) अवलोकित भी हुए हैं अर्थात् मैंने आपका नाम भी सुना है, पूजा भी की है और दर्शन भी किए हैं, फिर भी ( नूनम् ) निश्चय है कि (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (चेतसि) चित्त में (न विधृतः असि) धारण नहीं किए गए हो (तेन) उसी से मैं (दुःखपात्रम् जातः अस्मि) दुःखों का पात्र हो रहा हूँ ( यस्मात् ) क्योंकि ( भावशून्याः) भाव रहित (क्रिया:) क्रियाएँ (न प्रतिफलन्ति) सफल नहीं होतीं ।
टीका - भो विभो ! मया अज्ञानिना । त्वं आकर्णितोऽपि समवसरण- लक्ष्मीविराजमान एवं श्रुतोपि । एवंविधस्त्वं महितोऽपि पूजितोऽपि । एवंविधस्त्वं। निरीक्षितोऽपि । नूनं निश्चितं । चेतसि मनसि। भक्त्या सम्यक्त्वपूर्वकं। न विधृतोऽसि । हे जनानां बान्धव! तेनैव हेतुना अहं । दुःखानां पात्रं जातोऽस्मि सर्वदुःखस्थानं अभूवं । यस्मात्कारणद्भावशून्याः सम्यक्त्वरहिताः क्रियाः न प्रतिफलन्ति । भावेन शून्या भावशून्याः ।
भावार्थ - इससे पहले तीन श्लोकों में कहा गया था कि हे भगवन् ! मैंने “ आपका नाम नहीं सुना’ “” चरणों की पूजा नहीं की" और " दर्शन नहीं किये” इसलिए मैं दुःख उठा रहा हूँ । अब इस श्लोक में पक्षान्तर रूपसे कहते हैं कि मैंने आपका नाम भी सुना, पूजा भी की और दर्शन भी किये, फिर भी दुःख मेरा पिण्ड नहीं छोड़ते उसका कारण सिर्फ यही मालूम होता है कि मैंने भक्तिपूर्वक आपका ध्यान नहीं किया । केवल आडम्बर रूप से ही उन कामों को किया है न कि भावपूर्वक भी । यदि भाव से करता तो कभी दुःख नहीं उठाने पड़ते ।
दुःख नाशक प्रार्थना
त्वं नाथ! दुःखि-जन-वत्सल! हे शरण्य!
कारुण्य- पुण्य- वसते! वशिनां वरेण्य ! |
भक्त्या नते मयि महेश! दयां विधाय,
दुःखाङ्कुरोद्दलन-तत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥
अन्वयार्थ – (नाथ!) हे नाथ! (दुःखिजनवत्सल!) दुखियों पर प्रेम करने वाले ! ( हे शरण्य!) हे शरणागत प्रतिपालक ! (कारुण्य- पुण्यवसते!) हे दया की पवित्र भूमि ! ( वशिनाम् वरेण्य!) हे जितेन्द्रियों में श्रेष्ठ ! और (महेश) हे महेश्वर ! ( भक्त्या) भक्ति में (नते मयि ) नम्रीभूत मुझ पर (दयाम् विधाय) दया करके (दुःखाडुरोद्दलन-तत्परताम्) मेरे दुःखाङ्कुर के नाश करने में तत्परता/ तल्लीनता (विधेहि) कीजिए ।
टीका - भो शरण्य शरणाय अर्हं ! भो नाथ ! भो दुःखिजनानां वत्सल बांधव। भो कारुण्यपुण्यवसते! हे वशिनां वरेण्य ! हे यतीनां श्रेष्ठ ! हे महेश! मयि विषये। दयां कृपां । विधाय । दुःखानां अंकुरास्तेषां उद्दलनं निराकरणं तत्र तत्परस्तस्य भावस्तां विधेहि कुरु । कथंभूते मयि? भक्त्या नम्रीभूते । भो नाथ! हे पार्श्वनाथ ! हे जन बान्धव ! मम दुःखानि निवारय मोक्षं देहीति तात्पर्यार्थः ।
भावार्थ- आप शरणागत प्रतिपालक है, दयालु हैं और समर्थ भी हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे दुःखों को दूर करने के लिए तत्पर होइये ।
प्रभु चिन्तन बिन जीवन निस्सार
निः संख्य - सार - शरणं शरणं शरण्य-,
मासाद्य सादित - रिपुः प्रथिता वदानम् !
त्वत्पाद - पङ्कजमपि प्रणिधान - वन्ध्यो,
वन्ध्योऽस्मि चेद्भुवन-पावन! हा हतोऽस्मि ॥४०॥
अन्वयार्थ - (भुवनपावन!) हे संसार को पवित्र करने वाले भगवन्! (निःसंख्य-सारशरणम्) असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर की (शरणम्) रक्षा करने वाले (शरण्यम्) शरणागत प्रतिपालक और (सादितरिपु प्रथिता-वदानम्) कर्म-शत्रुओं के नाश से प्रसिद्ध है पराक्रम जिनका ऐसे (त्वत्पाद-पङ्कजम्) आपके चरणकमलों को (आसाद्य अपि ) पाकर भी (प्रणिधान - वन्ध्यः) उनके ध्यान से रहित हुआ मैं (वन्ध्यः अस्मि) अभागा-फलहीन हूँ और (तत्) उससे (हा) खेद है कि मैं (हतः अस्मि) नष्ट हुआ जा रहा हूँ अर्थात् कर्म मुझे दुःखी कर रहे हैं ।
टीका - हे भुवनपावन हे त्रैलोक्यपावन ! चेत् यदि । त्वत्पाद पंकजमपि तव चरणकमलमपि । आसाद्य प्राप्य । प्राणिधानेन वध्यः । पुनः पुनश्चिन्तन- रहितस्तर्हि बन्ध्योऽस्म्यहं अहं निष्फल एव । तव पादा एव पंकज त्वत्पादपङ्कजं । हा इति खेदे हतोऽस्मि पीडितोऽस्मि । कथम्भूतं त्वत्पादपङ्कजं ? निःसंख्याः संख्यारहिता ये साराः पदार्थास्तेषां शरणं गृहं । पुनः कथंभूतं? सादिता रिपवः कर्म वैरिणो येन तत्। पुनः कथंभूतं? प्रथितो विख्यातोऽवदानो महिमा यस्य तत् ।
भावार्थ– हे भगवन्! आपके पवित्र और दयालु चरणों को पाकर भी जो मैं उनका ध्यान नहीं कर रहा हूँ उससे मेरा जन्म निष्फल जा रहा है और मैं कर्मों के द्वारा दुःखी किया जा रहा हूँ ।
रक्षा प्रार्थना
देवेन्द्रवंद्य ! विदिताखिल वस्तुसार!
संसारतारक! विभो ! भुवनाधिनाथ ! |
त्रायस्व देव! करुणा - हृद! मां पुनीहि,
सीदन्त - मद्य भयद-व्यसनाम्बुराशेः॥४१॥
अन्वयार्थ– (देवेन्द्रवन्द्य!) हे इन्द्रों के वन्दनीय ! (विदिताखिल- वस्तुसार!) हे सब पदार्थों के रहस्य को जानने वाले (संसारतारक ! ) संसार सागर से तारने वाले ! (विभो ) हे प्रभो ! (भुवनाधिनाथ!) हे तीनों लोक के स्वामिन्! (करुणाहृद!) हे दया के सरोवर ! (देव !) देव ! (अद्य) आज (सीदन्तम्) दु:खी होते हुए (माम्) मुझको (भयद- व्यसनाम्बुराशेः ) भयंकर दुःखों के सागर से ( त्रायस्व) बचाओ और (पुनीहि) पवित्र करो।
टीका- देवेन्द्राणां वन्द्यः पूज्यस्तस्यामन्त्रणे हे देवेन्द्रवन्द्य! विदितो- ज्ञातोऽखिलवस्तूनां सर्वपदार्थानां सारस्तात्पर्यं येन स तस्यामन्त्रणे हे विदिताखिलवस्तुसार! संसारे भवाब्धौ : तारयतीति तस्यामन्त्रणे हे संसार- तारक! हे भुवनाधिनाथ! हे देव! करुणाया हृदः समुद्रः तस्यामन्त्रणे हे करुणाहृद! मां भक्तजनं । त्रायस्व पाहि ! भो देव! अद्य भयदो भयदायी यो व्यसनानां आपदां अम्बुराशिः सागरस्तस्मात् । पुनीहि पवित्रय रक्ष । कथम्भूतं मां सीदन्तं दुःखितं दुःखेन पीडितम् ।
भावार्थ - हे भगवन्! आप हरएक तरह से समर्थ हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस दुःख - समुद्र में डूबने से बचाइये और हमेशा के लिए कर्म-मैल से रहित कर दीजिये ।
भक्ति फल की याचना
यद्यस्ति नाथ! भवदङ्गि — सरोरुहाणां,
भक्तेः फलं किमपि सन्तत - सञ्चितायाः।
तन्मे त्वदेक - शरणस्य शरण्य! भूयाः,
स्वामी! त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥
अन्वयार्थ - ( नाथ !) हे नाथ! (त्वदेकशरणस्य) केवल आप ही की है शरण जिसको ऐसे (मे) मुझे ( सन्ततसञ्चितायाः ) चिरकाल से सञ्चित-एकत्रित हुई (भवद् अङ्गिसरोरुहाणाम्) आपके चरण कमलों की (भक्तेः ) भक्ति का (यदि) यदि (किमपि फलम् अस्ति ) कुछ भी फल है (तत्) तो उससे (शरण्य!) हे शरणागत प्रतिपालक ! (त्वम् एव) आप ही (अत्र भुवने) इहलोक में और ( भवान्तरे अपि) परलोक में भी ( मे स्वामी) मेरे स्वामी (भूयाः ) होवें ।
टीका - भो नाथ! भो शरण्य ! यदि चेत् भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां श्रीमच्चरण-कमलानां भक्तेः किमपि फलं अस्ति चेत् तत्तर्हि मे मम अत्र भुवने इह जन्मनि भवान्तरेऽपि वा त्वमेव स्वामी प्रभुर्भूया भवतात् । कथं भूताया भक्तेः? सन्तत्या निरन्तरेण सञ्चिता कृता तस्याः । कथंभूतस्य मे? त्वमेव एकं अद्वितीयं शरणं यस्य स तस्य ।
भावार्थ - हे भगवन् ! स्तुति कर मैं आपसे अन्य किसी फलकी चाह नहीं रखता। सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप ही मेरे हमेशा स्वामी रहें । अर्थात् जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक आप ही मेरे स्वामी रहें।‘“तुम होहु भवभव स्वामि मेरे, मैं सदा सेवक रहूँ"।
भक्ति की विधि
इत्थं समाहित – धियो विधिवज्जिनेन्द्र !
सान्द्रोल्लसत्पुलक-कञ्चुकिताङ्ग - भागाः ।
त्वद्विम्ब - निर्मल मुखाम्बुज - बद्धलक्ष्याः,
ये संस्तवं तव विभो ! रचयन्ति भव्याः ॥४३॥
अन्वयार्थ - (जिनेन्द्र !) हे जिनेन्द्र ! (ये भव्याः) जो भव्यजन (इत्थम्) इस तरह (समाहितधियः) सावधान बुद्धि से युक्त हो (त्वद् बिम्बनिर्मल-मुखाम्बुजबद्धलक्ष्याः) आपके निर्मल मुखकमल की ओर अपलक लक्ष्य करके ( सान्द्र - उल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः) सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से व्याप्त शरीर के अवयव जिनके ऐसे ( सन्तः ) होते हुए ( विधिवत् ) विधिपूर्वक (तव) आपका (संस्तवम् ) स्तवन ( रचयन्ति) रचते हैं।
टीका- भो जिनेन्द्र भो विभो ! ये भव्याः प्राणिनः शुद्धसम्यक्त्व- धारिणो जनाः । तव भगवतो । जिनस्य संस्तवनं यथार्थं स्तोत्रं । इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण । विधिवत् यथाविधि रचयन्ति । कथम्भूता भव्याः ? समाहिता सावधाना धी बुद्धिर्येषां ते । पुनः कथम्भूताः ? सान्द्रः निबिडः उल्लसन् यो हि पुलकः कण्टकस्तेन कञ्चुकिताः कवचिता अङ्गभागा शरीरप्रदेशा येषां ते । पुनः कथम्भूता? तव बिम्बं त्वद्विम्ब तस्य निर्मलं यन्मुखाम्बुजं मुखकमलं तत्र बद्धं लक्ष्यं यैस्ते ।
भक्ति का फल स्वर्ग मोक्षसंपद
जननयनकुमुदचन्द्र! प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ।
विगलित-मल- निचया अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥ ४४ ॥
टीका - जनानां भव्यानां नयनान्येव कुमुदानि कैरवाणि तत्र चन्द्रस्तस्यामंत्रणे हे जननयनकुमुदचन्द्र ! ते भव्याः ! स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा स्वर्गसाम्राज्यं परिभुज्य। अचिरात् स्वल्पकालेन। मोक्षं प्रपद्यन्ते लभंते। कीदृश्यः स्वर्गसम्पदः? प्रभास्वराः प्रकर्षेण भास्वराः दीप्यमानाः कथंभूता भव्याः? विगलितो मलनिचयो येषां ते विगलितमलनिचयाः।
अन्वयार्थ— (ते) वे (जननयनकुमुदचन्द्र !) हे प्राणियों के नेत्ररूपी कुमुदों-कमलों को विकसित करने के लिए चन्द्रमा की तरह शोभायमान देव ! (प्रभास्वराः) देदीप्यमान (स्वर्गसम्पदः) स्वर्ग की विभूतियों को (भुक्त्वा) भोगकर (विगलितमलनिचयाः 'सन्तः ') कर्मरूपी मल - समूह से रहित हो (अचिरात्) शीघ्र ही (मोक्षम् प्रपद्यन्ते) मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
भावार्थ- हे भगवन्! जो भक्ति से गद्गद चित्त हो आपकी स्तुति करते हैं वे स्वर्ग के सुख भोग बहुत जल्दी आठ कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । " स्वर्गन के सुख भोगकर, पावे मोक्ष निदान ।"